निबंध
विषय पर: "प्रजनन"
परिचय 3
1. प्रजनन के प्रकार 4
1.1 अलैंगिक प्रजनन 4
1.2 लैंगिक प्रजनन 6
2. जीवों का व्यक्तिगत विकास 10
2.1 भ्रूण विकास की अवधि 10
2.2 विकास की भ्रूणोत्तर अवधि 13
2.3 विकास के सामान्य पैटर्न. बायोजेनेटिक कानून 15
निष्कर्ष 18
सन्दर्भ 18
परिचय
पुनरुत्पादन की क्षमता, अर्थात्। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की नई पीढ़ी का उत्पादन जीवित जीवों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, आनुवंशिक सामग्री को मूल पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है, जो न केवल किसी प्रजाति की, बल्कि विशिष्ट मूल व्यक्तियों की विशेषताओं का प्रजनन सुनिश्चित करता है। किसी प्रजाति के लिए, प्रजनन का अर्थ उसके मरने वाले प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करना है, जो प्रजातियों के अस्तित्व की निरंतरता सुनिश्चित करता है; इसके अलावा, उपयुक्त परिस्थितियों में, प्रजनन से प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि संभव हो जाती है।
प्रत्येक नए व्यक्ति को, उस चरण तक पहुंचने से पहले, जिस पर वह प्रजनन करने में सक्षम है, वृद्धि और विकास के कई चरणों से गुजरना होगा। कुछ व्यक्ति शिकारियों, बीमारियों और विभिन्न यादृच्छिक घटनाओं द्वारा विनाश के परिणामस्वरूप प्रजनन चरण (या यौन परिपक्वता) तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं; इसलिए, प्रजातियां केवल इस शर्त पर जीवित रह सकती हैं कि प्रत्येक पीढ़ी प्रजनन में भाग लेने वाले मूल व्यक्तियों की तुलना में अधिक संतान पैदा करती है। व्यक्तियों के प्रजनन और विलुप्त होने के बीच संतुलन के आधार पर जनसंख्या के आकार में उतार-चढ़ाव होता है। कई अलग-अलग प्रचार रणनीतियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग फायदे और नुकसान हैं; उन सभी का वर्णन इस सार में किया जाएगा।
1. प्रजनन के प्रकार
प्रजनन के विभिन्न रूप ज्ञात हैं, लेकिन उन सभी को दो प्रकारों में जोड़ा जा सकता है: यौन और अलैंगिक।
यौन प्रजनन से तात्पर्य पीढ़ियों के परिवर्तन और गोनाडों में बनी विशेष सेक्स कोशिकाओं से जीवों के विकास से है। इस मामले में, अलग-अलग माता-पिता द्वारा गठित दो रोगाणु कोशिकाओं के संलयन के परिणामस्वरूप एक नया जीव विकसित होता है। हालाँकि, अकशेरुकी जानवरों में, शुक्राणु और अंडे अक्सर एक ही जीव के शरीर में बनते हैं। इस घटना, उभयलिंगीपन को उभयलिंगीपन कहा जाता है। फूल वाले पौधे भी उभयलिंगी होते हैं। एंजियोस्पर्म (फूल वाले) पौधों की अधिकांश प्रजातियों में, एक उभयलिंगी फूल में पुंकेसर, जो पुरुष सेक्स कोशिकाएं (शुक्राणु कोशिकाएं) बनाते हैं, और स्त्रीकेसर, जिनमें अंडे होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। लगभग एक चौथाई प्रजातियों में, नर (स्टैमिनेट) और मादा (पिस्टिलेट) फूल स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यानी। इनके फूल एकलिंगी होते हैं। इसका एक उदाहरण भांग है. कुछ पौधों (मकई, सन्टी) में नर और मादा दोनों फूल एक ही व्यक्ति पर दिखाई देते हैं।
जानवरों और पौधों की कुछ प्रजातियाँ विकसित होती हैं
अनिषेचित अंडा. इस प्रकार के प्रजनन को वर्जिन या पार्थेनोजेनेटिक कहा जाता है।
अलैंगिक प्रजनन की विशेषता यह है कि एक नया व्यक्ति गैर-यौन, दैहिक (शारीरिक) कोशिकाओं से विकसित होता है।
1.1 अलैंगिक प्रजनन
अलैंगिक प्रजनन के साथ, एक नया जीव एक कोशिका से या माँ की कई अलैंगिक (दैहिक) कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता-पिता शामिल होता है। चूँकि पुत्री जीवों को जन्म देने वाली कोशिकाएँ माइटोसिस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं, इसलिए सभी वंशज वंशानुगत विशेषताओं में मातृ व्यक्ति के समान होंगे।
चावल। 1. हरी यूग्लीना का प्रजनन
कई प्रोटोजोआ (अमीबा, हरा यूग्लीना, आदि), एककोशिकीय शैवाल (क्लैमाइडोमोनस) माइटोटिक कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं (चित्र 1)। अन्य एककोशिकीय कुछ निचले कवक, शैवाल (क्लोरेला), जानवर, उदाहरण के लिए मलेरिया मलेरिया प्लास्मोडियम का प्रेरक एजेंट, स्पोरुलेशन द्वारा विशेषता है। इस मामले में, कोशिका बड़ी संख्या में व्यक्तियों में टूट जाती है, जो उसके नाभिक के बार-बार विभाजन के परिणामस्वरूप मूल कोशिका में पहले बने नाभिकों की संख्या के बराबर होती है। बहुकोशिकीय जीव भी स्पोरुलेशन में सक्षम हैं: ये काई, उच्च कवक, बहुकोशिकीय शैवाल, टेरिडोफाइट्स और कुछ अन्य हैं।
एककोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में, मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। उदाहरण के लिए, यीस्ट कवक और कुछ सिलिअट्स (चूसने वाले सिलिअट्स) में, जब मातृ कोशिका पर नवोदित होता है, तो शुरू में एक नाभिक, एक कली युक्त एक छोटा ट्यूबरकल बनता है। यह बढ़ता है, मां के शरीर के आकार के करीब पहुंचता है और फिर अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व की ओर बढ़ता है। बहुकोशिकीय जीवों (मीठे पानी के हाइड्रा) में, गुर्दे में शरीर की दीवार की दोनों परतों की कोशिकाओं का एक समूह होता है। कली बढ़ती है, लंबी हो जाती है, और इसके अग्र सिरे पर एक मुँह खुलता है, जो जालों से घिरा होता है। मुकुलन एक छोटे हाइड्रा के निर्माण के साथ समाप्त होता है, जो फिर मातृ जीव से अलग हो जाता है।
बहुकोशिकीय जानवरों में, अलैंगिक प्रजनन उसी तरह होता है (जेलीफ़िश, एनेलिड्स, फ्लैटवर्म, इचिनोडर्म)। ऐसे प्रत्येक भाग से एक पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है।
पौधों में वानस्पतिक प्रसार व्यापक है, अर्थात्। शरीर के अंग कटिंग, टेंड्रिल, कंद। इस प्रकार, आलू तने के संशोधित भूमिगत भागों - कंदों द्वारा प्रजनन करते हैं। चमेली और विलो के अंकुर और कलम आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं। अंगूर, किशमिश और आंवले को कटिंग का उपयोग करके प्रचारित किया जाता है।
स्ट्रॉबेरी टेंड्रिल के लंबे रेंगने वाले तने कलियों का निर्माण करते हैं, जो जड़ें जमाकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। कुछ पौधे, जैसे बेगोनिया, को पत्ती की कटिंग (पत्ती ब्लेड और डंठल) द्वारा प्रचारित किया जा सकता है। पत्ती के नीचे की ओर, उन स्थानों पर जहां बड़ी नसें शाखा करती हैं, जड़ें दिखाई देती हैं, ऊपरी तरफ कलियाँ होती हैं, और फिर अंकुर होते हैं।
जड़ का उपयोग वानस्पतिक प्रसार के लिए भी किया जाता है। बागवानी में, रसभरी, चेरी, प्लम और गुलाब को पार्श्व जड़ों से कलमों का उपयोग करके प्रचारित किया जाता है। डहलिया जड़ कंदों का उपयोग करके प्रजनन करते हैं। तने के प्रकंद के भूमिगत भाग का संशोधन भी नए पौधों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए, प्रकंदों की सहायता से थीस्ल बोना प्रति 1 वर्ग मीटर मिट्टी में एक हजार से अधिक नए व्यक्ति पैदा कर सकता है।
1.2 लैंगिक प्रजनन
अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन के बहुत बड़े विकासवादी फायदे हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि संतान का जीनोटाइप माता-पिता दोनों के जीनों के संयोजन से उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप, जीवों की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता बढ़ जाती है। चूंकि प्रत्येक पीढ़ी में नए संयोजन होते हैं, इसलिए अलैंगिक प्रजनन की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति अस्तित्व की नई स्थितियों के लिए अनुकूलित हो सकते हैं। नए जीन संयोजनों का उद्भव बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों का अधिक सफल और तेजी से अनुकूलन सुनिश्चित करता है।
इस प्रकार, यौन प्रजनन का सार दो अलग-अलग स्रोतों - माता-पिता से आनुवंशिक जानकारी के वंशज की वंशानुगत सामग्री में संयोजन में निहित है।
सेक्स कोशिकाएं गोनाड में विकसित होती हैं: पुरुष शुक्राणु, महिला अंडाणु (या अंडे)। पहले मामले में, उनके विकास को शुक्राणुजनन कहा जाता है, दूसरे में - अंडजनन (लैटिन ओवो - अंडा से)।
रोगाणु कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में, कई चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है। पहला चरण प्रजनन की अवधि है, जिसमें प्राइमर्डियल रोगाणु कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि होती है।
दूसरा चरण विकास की अवधि है। अपरिपक्व नर युग्मकों में इसका उच्चारण नहीं होता है। इनका आकार थोड़ा बढ़ जाता है. इसके विपरीत, भविष्य के अंडों के अंडकोष आकार में बढ़ जाते हैं, कभी-कभी सैकड़ों, और अधिक बार हजारों और यहां तक कि लाखों बार। oocytes की वृद्धि शरीर की अन्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थों के कारण होती है। इस प्रकार, मछली, उभयचर और, काफी हद तक, सरीसृपों और पक्षियों में, अंडे का बड़ा हिस्सा जर्दी होता है। यह यकृत में संश्लेषित होता है, एक विशेष घुलनशील रूप में रक्त द्वारा अंडाशय तक पहुंचाया जाता है, बढ़ते हुए अंडाणु में प्रवेश करता है और वहां जर्दी प्लेटों के रूप में जमा हो जाता है। इसके अलावा, भविष्य की प्रजनन कोशिका में ही, कई प्रोटीन और बड़ी संख्या में विभिन्न आरएनए संश्लेषित होते हैं: परिवहन, राइबोसोमल और सूचनात्मक। जर्दी विकासशील भ्रूण को पोषण देने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों (वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आदि) का एक संग्रह है, और आरएनए विकास के प्रारंभिक चरण में प्रोटीन के संश्लेषण को सुनिश्चित करता है, जब इसकी अपनी विनाशकारी जानकारी का अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है।
अगला चरण, परिपक्वता की अवधि, या अर्धसूत्रीविभाजन, चित्र 2 में प्रस्तुत किया गया है। परिपक्वता की अवधि में प्रवेश करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक द्विगुणित सेट और पहले से ही दोगुनी मात्रा में डीएनए होता है।

चावल। 2. रोगाणु कोशिकाओं की परिपक्वता (अर्धसूत्रीविभाजन)
अर्धसूत्रीविभाजन का सार यह है कि प्रत्येक सेक्स कोशिका को गुणसूत्रों का एक एकल, अगुणित, सेट प्राप्त होता है। हालाँकि, एक ही समय में, अर्धसूत्रीविभाजन एक ऐसा चरण है जिसके दौरान विभिन्न मातृ और पितृ गुणसूत्रों के संयोजन से जीन के नए संयोजन बनते हैं; वंशानुगत झुकावों का पुनर्संयोजन भी क्रॉसिंग ओवर के परिणामस्वरूप होता है - प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच वर्गों का आदान-प्रदान अर्धसूत्रीविभाजन का.
अर्धसूत्रीविभाजन में दो क्रमिक विभाजन शामिल होते हैं। माइटोसिस की तरह, प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में चार चरण होते हैं: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़।
प्रथम (I) अर्धसूत्रीविभाजन. प्रोफ़ेज़ I की शुरुआत गुणसूत्रों के सर्पिलीकरण से होती है। जैसा कि आपको याद है, प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर पर जुड़े दो क्रोमैटिड होते हैं। फिर समजातीय गुणसूत्र एक-दूसरे के करीब आते हैं, एक गुणसूत्र के प्रत्येक क्रोमैटिड का प्रत्येक बिंदु दूसरे, समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड के संबंधित बिंदु के साथ जुड़ जाता है। अर्धसूत्रीविभाजन में समजात गुणसूत्रों को सटीक और निकट लाने की इस प्रक्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। भविष्य में, ऐसे गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर हो सकता है - समान, या समजात, यानी समान जीन वाले क्षेत्रों का आदान-प्रदान। प्रोफ़ेज़ के अंत में, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकारक बल उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले, वे सेंट्रोमियर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और फिर अन्य क्षेत्रों में।
मेटाफ़ेज़ I में, गुणसूत्र सर्पिलीकरण अधिकतम होता है। संयुग्मित गुणसूत्र भूमध्य रेखा के साथ स्थित होते हैं, समजात गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर कोशिका के विभिन्न ध्रुवों का सामना करते हैं। धुरी के धागे उनसे जुड़े होते हैं।
एनाफ़ेज़ I में, समजात गुणसूत्रों की भुजाएँ अंततः अलग हो जाती हैं, और गुणसूत्र अलग-अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप, समजातीय गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े से केवल एक ही पुत्री कोशिका में प्रवेश करता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र समूह अगुणित हो जाता है। हालाँकि, प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं, यानी, इसमें अभी भी डीएनए की दोगुनी मात्रा होती है।
टेलोफ़ेज़ I में, थोड़े समय के लिए एक परमाणु आवरण बनता है। अर्धसूत्रीविभाजन के पहले और दूसरे विभाजन के बीच अंतरावस्था के दौरान, डीएनए दोहराव नहीं होता है। परिपक्वता के पहले विभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं पैतृक और मातृ गुणसूत्रों की संरचना में और, परिणामस्वरूप, जीन के सेट में भिन्न होती हैं।
उदाहरण के लिए, प्राइमर्डियल जर्म कोशिकाओं सहित सभी मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23 पिता से और 23 माता से प्राप्त हुए। जब पहले अर्धसूत्रीविभाजन के बाद रोगाणु कोशिकाएं बनती हैं, तो शुक्राणुकोशिका और अंडाणु को भी 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। हालाँकि, एनाफ़ेज़ I में पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के विचलन की यादृच्छिकता के कारण, परिणामी कोशिकाओं को पैतृक गुणसूत्रों के संयोजन की एक विस्तृत विविधता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, उनमें से एक में 3 पैतृक और 20 मातृ गुणसूत्र हो सकते हैं, दूसरे में 10 पैतृक और 13 मातृ, तीसरे में 20 पैतृक और 3 मातृ, आदि। संभावित संयोजनों की संख्या बहुत बड़ी है। यदि हम अर्धसूत्रीविभाजन के पहले विभाजन के प्रोफ़ेज़ में गुणसूत्रों के समजात वर्गों के आदान-प्रदान को भी ध्यान में रखते हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्येक परिणामी रोगाणु कोशिका आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जीन का अपना अनूठा सेट होता है।
नतीजतन, अर्धसूत्रीविभाजन संयोजनात्मक जीनोटाइपिक परिवर्तनशीलता का आधार है।
दूसरा (II) अर्धसूत्रीविभाजन। अर्धसूत्रीविभाजन का दूसरा विभाजन आम तौर पर सामान्य माइटोटिक विभाजन की तरह ही आगे बढ़ता है, एकमात्र अंतर यह है कि विभाजित कोशिका अगुणित होती है। एनाफ़ेज़ II में, प्रत्येक गुणसूत्र में बहन क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाले सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं, और क्रोमैटिड्स, माइटोसिस की तरह, इस क्षण से स्वतंत्र गुणसूत्र बन जाते हैं। टेलोफ़ेज़ II के पूरा होने के साथ, अर्धसूत्रीविभाजन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है: मूल प्राथमिक रोगाणु कोशिका से चार अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं।
पुरुषों में, ये सभी युग्मक - शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। महिलाओं में, असमान अर्धसूत्रीविभाजन के कारण, केवल एक कोशिका ही व्यवहार्य अंडे का उत्पादन करती है। अन्य तीन संतति कोशिकाएँ बहुत छोटी होती हैं; वे तथाकथित मार्गदर्शक, या कम करने वाले शरीर में बदल जाती हैं, जो जल्द ही मर जाती हैं। जैविक दृष्टिकोण से, केवल एक अंडे का निर्माण और तीन आनुवंशिक रूप से पूर्ण मार्गदर्शक निकायों की मृत्यु एक कोशिका में सभी आरक्षित पोषक तत्वों को संरक्षित करने की आवश्यकता के कारण होती है जो भविष्य के भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होंगे।
गठन की अवधि में कोशिकाएं अपने कार्य के अनुरूप एक निश्चित आकार और आकार प्राप्त करती हैं।
परिपक्वता की प्रक्रिया के दौरान, मादा जनन कोशिकाएं झिल्लियों से ढक जाती हैं और अर्धसूत्रीविभाजन के पूरा होने के तुरंत बाद निषेचन के लिए तैयार हो जाती हैं। कई मामलों में, उदाहरण के लिए सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों में, अंडे के आसपास की कोशिकाओं की गतिविधि के कारण, इसके चारों ओर कई अतिरिक्त झिल्ली दिखाई देती हैं। उनका कार्य अंडे और विकासशील भ्रूण को बाहरी प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। शुक्राणु के विभिन्न आकार और आकार हो सकते हैं।
शुक्राणु का कार्य अंडे तक आनुवंशिक जानकारी पहुंचाना और उसके विकास को प्रोत्साहित करना है। गठित शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र होता है, जो एंजाइमों को स्रावित करता है जो निषेचन के दौरान, यानी शुक्राणु और अंडे के संलयन के दौरान अंडे की झिल्ली को भंग कर देता है। परिणामी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज कहा जाता है।
2. जीवों का व्यक्तिगत विकास
व्यक्तिगत विकास, या ओटोजेनेसिस, किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी अवधि को संदर्भित करता है, जिस क्षण से शुक्राणु अंडे के साथ विलय होता है और जीव की मृत्यु तक युग्मनज का निर्माण होता है। ओटोजेनेसिस को दो अवधियों में विभाजित किया गया है: 1) युग्मनज के निर्माण से लेकर जन्म तक या अंडे की झिल्लियों से बाहर निकलने तक भ्रूण; 2) अंडे की झिल्लियों से बाहर निकलने या जन्म से लेकर जीव की मृत्यु तक पोस्टएम्ब्रायोनिक।
वह विज्ञान जो भ्रूण अवस्था में जीवों के व्यक्तिगत विकास के पैटर्न का अध्ययन करता है, भ्रूणविज्ञान (ग्रीक भ्रूण भ्रूण से) कहलाता है।
2.1 भ्रूण विकास की अवधि
अधिकांश बहुकोशिकीय जानवरों में, उनके संगठन की जटिलता की परवाह किए बिना, भ्रूण के विकास के चरण समान होते हैं। भ्रूण काल में, तीन मुख्य चरण होते हैं: दरार, गैस्ट्रुलेशन और प्राथमिक ऑर्गोजेनेसिस।
बंटवारे अप। किसी जीव का विकास एकल कोशिका अवस्था से शुरू होता है। एक निषेचित अंडा एक कोशिका है और साथ ही अपने विकास के प्रारंभिक चरण में एक जीव है। बार-बार विभाजन के परिणामस्वरूप, एककोशिकीय जीव बहुकोशिकीय में बदल जाता है। द्विगुणित नाभिक, जो शुक्राणु और अंडे के संलयन के माध्यम से निषेचन के दौरान प्रकट होता है, कुछ ही मिनटों में विभाजित होना शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी इसके साथ विभाजित हो जाता है। प्रत्येक विभाजन के साथ परिणामी कोशिकाओं का आकार घटता जाता है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया को दरार कहा जाता है। विखंडन की अवधि के दौरान, सेलुलर सामग्री आगे के विकास के लिए जमा होती है। विखंडन एक बहुकोशिकीय भ्रूण, ब्लास्टुला के निर्माण के साथ समाप्त होता है। ब्लास्टुला में द्रव से भरी एक गुहा होती है, जिसे प्राथमिक शरीर गुहा कहा जाता है।
ऐसे मामलों में जहां अंडे के साइटोप्लाज्म में बहुत कम जर्दी होती है (जैसा कि लांसलेट में) या अपेक्षाकृत कम होती है (जैसा कि मेंढक में), विखंडन पूरा हो जाता है, यानी, अंडा पूरी तरह से विभाजित हो जाता है।
अन्यथा पक्षियों में विखंडन का काल आता है। जर्दी-मुक्त साइटोप्लाज्म मुर्गी के अंडे की कुल मात्रा का केवल 1% बनाता है; अंडे का संपूर्ण शेष साइटोप्लाज्म, और इसलिए युग्मनज, जर्दी के द्रव्यमान से भरा होता है। यदि आप मुर्गी के अंडे को करीब से देखते हैं, तो उसके एक ध्रुव पर सीधे जर्दी पर आप एक छोटा सा धब्बा देख सकते हैं - एक ब्लास्टुला, या जर्मिनल डिस्क, जो नाभिक वाले साइटोप्लाज्म के जर्दी-मुक्त खंड को कुचलने के परिणामस्वरूप बनता है। ऐसे में क्रशिंग को अधूरा कहा जाता है। अधूरा विखंडन भी कुछ मछलियों और सरीसृपों की विशेषता है।
सभी मामलों में, लैंसलेट, और उभयचर, और पक्षियों, साथ ही अन्य जानवरों दोनों में, ब्लास्टुला चरण में कोशिकाओं की कुल मात्रा युग्मनज की मात्रा से अधिक नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, युग्मनज का माइटोटिक विभाजन मां की मात्रा के परिणामस्वरूप बेटी कोशिकाओं की वृद्धि के साथ नहीं होता है, और क्रमिक विभाजनों की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उनका आकार उत्तरोत्तर कम होता जाता है। दरार के दौरान समसूत्री कोशिका विभाजन की यह विशेषता सभी जानवरों में निषेचित अंडों के विकास के दौरान देखी जाती है।
कुचलने की कुछ अन्य विशेषताएं भी विभिन्न पशु प्रजातियों की विशेषता हैं। उदाहरण के लिए, ब्लास्टुला की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का द्विगुणित समूह होता है, संरचना में समान होते हैं और मुख्य रूप से उनमें मौजूद जर्दी की मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसी कोशिकाएँ, जिनमें कुछ कार्य करने के लिए विशेषज्ञता के लक्षण नहीं होते, अविशिष्ट (या अविभाजित) कोशिकाएँ कहलाती हैं। दरार की एक अन्य विशेषता वयस्क जीव की कोशिकाओं की तुलना में ब्लास्टोमेरेस का बेहद छोटा माइटोटिक चक्र है। बहुत ही छोटे इंटरफ़ेज़ के दौरान, केवल डीएनए दोहराव होता है।
जठराग्नि. ब्लास्टुला, एक नियम के रूप में, विकास प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ब्लास्टोमेरेस (उदाहरण के लिए, 3000 कोशिकाओं से लैंसलेट में) से मिलकर एक नए चरण में गुजरता है, जिसे गैस्ट्रुला (ग्रीक गैस्टर पेट से) कहा जाता है। इस स्तर पर भ्रूण में कोशिकाओं की स्पष्ट रूप से अलग-अलग परतें होती हैं - तथाकथित रोगाणु परतें: बाहरी, या एक्टोडर्म (ग्रीक एक्टोस से - बाहर स्थित), और आंतरिक, या एंडोडर्म (ग्रीक एंटोस से - अंदर स्थित) . गैस्ट्रुला के निर्माण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के समूह को गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है।
लांसलेट में, गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला के ध्रुवों में से एक को दूसरे की ओर अंदर की ओर आक्रमण करके किया जाता है; अन्य जानवरों में, या तो ब्लास्टुला की दीवार के प्रदूषण द्वारा, या छोटी कोशिकाओं के साथ विशाल वनस्पति ध्रुव को उखाड़कर किया जाता है। पशु खंभा.
बहुकोशिकीय जंतुओं में, सहसंयोजकों को छोड़कर, गैस्ट्रुलेशन के समानांतर या, लैंसलेट की तरह, इसके बाद, तीसरी रोगाणु परत मेसोडर्म (मध्य में स्थित ग्रीक मेसोस से) प्रकट होती है, जो एक्टो- के बीच स्थित सेलुलर तत्वों का एक समूह है। और प्राथमिक शरीर गुहा ब्लास्टोसेले में एंडोडर्म। मेसोडर्म की उपस्थिति के साथ, भ्रूण तीन-परत वाला हो जाता है।
इस प्रकार, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया का सार कोशिका द्रव्यमान की गति है। भ्रूण की कोशिकाएं व्यावहारिक रूप से विभाजित होती हैं और बढ़ती नहीं हैं। हालाँकि, इस स्तर पर भ्रूण कोशिकाओं की आनुवंशिक जानकारी का उपयोग शुरू होता है, और भेदभाव के पहले लक्षण दिखाई देते हैं।
विभेदन, या विभेदीकरण, इसके घटित होने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत कोशिकाओं और भ्रूण के भागों के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतर में वृद्धि है। रूपात्मक दृष्टिकोण से, भिन्नता एक विशिष्ट संरचना की कई सौ प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में व्यक्त की जाती है जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अविशिष्ट ब्लास्टुला कोशिकाओं से, त्वचा की उपकला कोशिकाएं, आंतों की उपकला, फेफड़े, तंत्रिका और मांसपेशी कोशिकाएं आदि धीरे-धीरे उभरती हैं। जैव रासायनिक दृष्टिकोण से, कोशिका विशेषज्ञता कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता में निहित है जो केवल किसी दिए गए कोशिका प्रकार की विशेषता हैं। लिम्फोसाइट्स सुरक्षात्मक प्रोटीन एंटीबॉडी, मांसपेशियों की कोशिकाओं सिकुड़ा प्रोटीन मायोसिन को संश्लेषित करते हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका अपने स्वयं के प्रोटीन का उत्पादन करती है, जो उसके लिए अद्वितीय है। कोशिकाओं की जैव रासायनिक विशेषज्ञता जीन की चयनात्मक, विभेदक गतिविधि द्वारा सुनिश्चित की जाती है, यानी, विभिन्न रोगाणु परतों की कोशिकाओं में, कुछ अंगों और प्रणालियों की शुरुआत, जीन के विभिन्न समूह कार्य करना शुरू करते हैं।
विभिन्न पशु प्रजातियों में, समान रोगाणु परतें समान अंगों और ऊतकों को जन्म देती हैं। इसका मतलब यह है कि वे समजातीय हैं। इस प्रकार, बाहरी रोगाणु परत की कोशिकाओं से - एक्टोडर्म - आर्थ्रोपोड्स में, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित कॉर्डेट्स, त्वचा और उनके डेरिवेटिव, साथ ही तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग बनते हैं। अधिकांश जानवरों की रोगाणु परतों की समरूपता पशु जगत की एकता के प्रमाणों में से एक है।
ऑर्गोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन के पूरा होने के बाद, भ्रूण अक्षीय अंगों का एक परिसर बनाता है: तंत्रिका ट्यूब, नॉटोकॉर्ड और आंत्र ट्यूब। लैंसलेट में, अक्षीय अंग निम्नानुसार बनते हैं: भ्रूण के पृष्ठीय पक्ष पर एक्टोडर्म मध्य रेखा के साथ झुकता है, एक खांचे में बदल जाता है, और इसके दाएं और बाएं स्थित एक्टोडर्म इसके किनारों पर बढ़ने लगता है। नाली, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत, एक्टोडर्म के नीचे डूब जाती है, और इसके किनारे बंद हो जाते हैं। एक न्यूरल ट्यूब बनती है। एक्टोडर्म का शेष भाग त्वचा उपकला का प्रारंभिक हिस्सा है।
एंडोडर्म का पृष्ठीय भाग, जो सीधे तंत्रिका मूल के नीचे स्थित होता है, एंडोडर्म के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है और एक घने रज्जु में बदल जाता है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। एंडोडर्म के शेष भाग से, मेसोडर्म और आंतों के उपकला का विकास होता है। भ्रूण कोशिकाओं के और अधिक विभेदन से रोगाणु परतों - अंगों और ऊतकों के कई व्युत्पन्नों का उद्भव होता है। रोगाणु परतों को बनाने वाली कोशिकाओं के विशेषज्ञता की प्रक्रिया में, एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग, त्वचा उपकला और दाँत तामचीनी का निर्माण होता है; एंडोडर्म आंतों के उपकला से, पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय, गलफड़ों और फेफड़ों के उपकला से; मेसोडर्म मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक से, जिसमें ढीले संयोजी ऊतक, उपास्थि और हड्डी के ऊतक, रक्त और लसीका, साथ ही संचार प्रणाली, गुर्दे, गोनाड शामिल हैं।
2.2 विकास की भ्रूणोत्तर अवधि
जन्म के समय या अंडे के छिलके से जीव की रिहाई के समय, भ्रूण की अवधि समाप्त हो जाती है और विकास की पोस्ट-भ्रूण अवधि शुरू हो जाती है। भ्रूण के बाद का विकास प्रत्यक्ष या परिवर्तन (कायापलट) के साथ हो सकता है।
प्रत्यक्ष विकास (सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों में) के दौरान, छोटे आकार का एक जीव अंडे के छिलके से या माँ के शरीर से निकलता है, लेकिन एक वयस्क जानवर की विशेषता वाले सभी मुख्य अंग पहले ही बन चुके होते हैं। इस मामले में भ्रूण के बाद का विकास मुख्य रूप से वृद्धि और यौवन तक कम हो जाता है।
कायापलट के साथ विकास के दौरान, अंडे से एक लार्वा निकलता है, जो आमतौर पर एक वयस्क जानवर की तुलना में संरचना में सरल होता है, जिसमें विशेष लार्वा अंग होते हैं जो वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होते हैं। लार्वा खाता है, बढ़ता है, और समय के साथ लार्वा अंगों को वयस्क व्यक्तियों की विशेषता वाले अंगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नतीजतन, कायापलट के दौरान, लार्वा अंग नष्ट हो जाते हैं और वयस्क जानवरों की विशेषता वाले अंग प्रकट होते हैं।
आइए हम अप्रत्यक्ष प्रसवोत्तर विकास के कई उदाहरण देखें। एस्किडियन लार्वा (फ़ाइलम कॉर्डेटा, सबफ़ाइलम लार्वा-कॉर्डेटा) में कॉर्डेट्स की सभी मुख्य विशेषताएं हैं: एक नोटोकॉर्ड, एक तंत्रिका ट्यूब, और ग्रसनी में गिल स्लिट। यह स्वतंत्र रूप से तैरता है, फिर समुद्र के तल पर कुछ ठोस सतह से जुड़ जाता है, जहां कायापलट होता है: इसकी पूंछ, नॉटोकॉर्ड और मांसपेशियां गायब हो जाती हैं, और तंत्रिका ट्यूब अलग-अलग कोशिकाओं में टूट जाती है, जिनमें से अधिकांश फागोसाइटोज्ड होती हैं। लार्वा तंत्रिका तंत्र के सभी अवशेष कोशिकाओं का एक समूह है जो तंत्रिका नाड़ीग्रन्थि को जन्म देते हैं। एक संलग्न जीवन शैली का नेतृत्व करने वाले एक वयस्क जलोदर की शारीरिक संरचना कॉर्डेट्स के संगठन की सामान्य विशेषताओं से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। ओण्टोजेनेसिस की विशेषताओं का केवल ज्ञान ही जलोदर की व्यवस्थित स्थिति को निर्धारित करना संभव बनाता है: लार्वा की संरचना कॉर्डेट्स से उनकी उत्पत्ति का संकेत देती है जो एक मुक्त जीवन शैली का नेतृत्व करते थे। कायापलट की प्रक्रिया के दौरान, एस्किडियन एक गतिहीन जीवन शैली में बदल जाते हैं, और इसलिए उनका संगठन सरल हो जाता है।
उभयचरों का लार्वा रूप एक टैडपोल है, जिसकी विशेषता गिल स्लिट, एक पार्श्व रेखा, दो-कक्षीय हृदय और रक्त परिसंचरण का एक चक्र है। कायापलट की प्रक्रिया के दौरान, जो थायराइड हार्मोन के प्रभाव में होता है, पूंछ सुलझ जाती है, अंग दिखाई देते हैं, पार्श्व रेखा गायब हो जाती है, फेफड़े और रक्त परिसंचरण का दूसरा चक्र विकसित होता है। टैडपोल और मछली (पार्श्व रेखा, हृदय और संचार प्रणाली की संरचना, गिल स्लिट) की कई संरचनात्मक विशेषताओं की समानता उल्लेखनीय है।
कीड़ों का विकास भी कायापलट के उदाहरण के रूप में काम कर सकता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर या ड्रैगनफ्लाई लार्वा वयस्क जानवरों से संरचना, जीवनशैली और निवास स्थान में काफी भिन्न होते हैं और अपने पूर्वजों, एनेलिड्स से मिलते जुलते हैं।
भ्रूण के बाद के विकास की अवधि अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, प्रजाति के आधार पर, मेफ़्लाइज़ लार्वा अवस्था में 2-3 साल तक जीवित रहती हैं, और परिपक्व अवस्था में 2-3 घंटे से लेकर 2-3 दिन तक जीवित रहती हैं। ज्यादातर मामलों में, भ्रूण के बाद की अवधि लंबी होती है। मनुष्यों में, इसमें यौवन चरण, परिपक्वता चरण और वृद्धावस्था चरण शामिल हैं।
स्तनधारियों और मनुष्यों में, यौवन और गर्भावस्था की अवधि पर जीवन प्रत्याशा की निर्भरता ज्ञात है। जीवन प्रत्याशा आमतौर पर अधिक होती है
ओटोजेनेसिस की पूर्व-प्रजनन अवधि 5-8 गुना।
भ्रूण के बाद का विकास वृद्धि के साथ होता है। अनिश्चित विकास, जो जीवन भर जारी रहता है, और निश्चित विकास, जो एक निश्चित अवधि तक सीमित होता है, के बीच अंतर किया जाता है। लकड़ी के पौधों, कुछ मोलस्क, कशेरुक, मछली और चूहों में अनिश्चित वृद्धि देखी जाती है।
कई जानवरों में, यौन परिपक्वता तक पहुंचने के तुरंत बाद विकास रुक जाता है। मनुष्यों में विकास 20-25 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है।
2.3 विकास के सामान्य पैटर्न. बायोजेनेटिक कानून
सभी बहुकोशिकीय जीव एक निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। एक ही प्रकार के जानवरों में भ्रूण का विकास काफी हद तक समान होता है। सभी कॉर्डेट्स में, भ्रूण काल में, अक्षीय कंकाल नॉटोकॉर्ड का निर्माण होता है, तंत्रिका ट्यूब दिखाई देती है, और ग्रसनी के पूर्वकाल भाग में गिल स्लिट बनते हैं। कॉर्डेट्स की संरचनात्मक योजना भी समान होती है। विकास के प्रारंभिक चरण में, कशेरुकी भ्रूण बहुत समान होते हैं (चित्र 3)। ये तथ्य के. बेयर द्वारा तैयार किए गए भ्रूण समानता के कानून की वैधता की पुष्टि करते हैं: "भ्रूण प्रारंभिक चरण से ही, प्रकार के भीतर एक निश्चित सामान्य समानता प्रदर्शित करता है।" विभिन्न व्यवस्थित समूहों के भ्रूणों की समानता उनकी सामान्य उत्पत्ति को इंगित करती है। इसके बाद, भ्रूण की संरचना से वर्ग, जीनस, प्रजाति की विशेषताओं और अंत में, किसी दिए गए व्यक्ति की विशेषताओं का पता चलता है। विकास के दौरान भ्रूण की विशेषताओं के विचलन को भ्रूणीय विचलन कहा जाता है और यह जानवरों के एक विशेष व्यवस्थित समूह के विकास, किसी प्रजाति के विकास के इतिहास को दर्शाता है।

चावल। 3. कशेरुकियों में रोगाणु समानता: 1 मोनोट्रेम (एकिडना), 2 मार्सुपियल्स (कंगारू), 3 आर्टियोडैक्टिल (हिरण), 4 मांसाहारी (बिल्ली), 5 प्राइमेट (बंदर), 6 - मनुष्य
विकास के प्रारंभिक चरण में भ्रूणों के बीच बड़ी समानता
बाद के चरणों में मतभेद की घटना की अपनी व्याख्या है।
विकास के दौरान शरीर परिवर्तनशीलता के अधीन है।
उत्परिवर्तन प्रक्रिया उन जीनों को प्रभावित करती है जो सबसे कम उम्र के भ्रूणों की संरचनात्मक और चयापचय विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। लेकिन उनमें जो संरचनाएं उत्पन्न होती हैं (दूर के पूर्वजों की प्राचीन विशेषताएं) आगे के विकास की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि संकेत दिया गया है, नॉटोकॉर्ड प्रिमोर्डियम तंत्रिका ट्यूब के निर्माण को प्रेरित करता है, और इसके नुकसान से विकास रुक जाता है। इसलिए, प्रारंभिक चरणों में परिवर्तन आमतौर पर व्यक्ति के अविकसितता और मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, बाद के चरणों में परिवर्तन, कम महत्वपूर्ण लक्षणों को प्रभावित करते हुए, जीव के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और ऐसे मामलों में प्राकृतिक चयन द्वारा उठाए जाते हैं।
आधुनिक जानवरों के विकास के भ्रूण काल में उनके दूर के पूर्वजों की विशेषताओं की उपस्थिति अंगों की संरचना में विकासवादी परिवर्तनों को दर्शाती है।
अपने विकास में जीव एककोशिकीय अवस्था (जाइगोट अवस्था) से गुजरता है, जिसे आदिम अमीबा की फाइलोजेनेटिक अवस्था की पुनरावृत्ति माना जा सकता है। सभी कशेरुकियों में, उनके उच्चतम प्रतिनिधियों सहित, एक नॉटोकॉर्ड बनता है, जिसे बाद में रीढ़ द्वारा बदल दिया जाता है, और उनके पूर्वजों में, लांसलेट द्वारा देखते हुए, नॉटोकॉर्ड जीवन भर बना रहता है। मनुष्यों सहित पक्षियों और स्तनधारियों के भ्रूण विकास के दौरान, ग्रसनी में गिल स्लिट और संबंधित सेप्टा दिखाई देते हैं। स्थलीय कशेरुकियों के भ्रूण में गिल तंत्र के कुछ हिस्सों के गठन के तथ्य को मछली जैसे पूर्वजों से उनकी उत्पत्ति से समझाया गया है जो गलफड़ों से सांस लेते थे। गठन की प्रारंभिक अवधि में मानव भ्रूण के हृदय की संरचना मछली के इस अंग की संरचना से मिलती जुलती है: इसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। बिना दांत वाली व्हेल के दांत भ्रूण काल के दौरान विकसित होते हैं। ये दाँत फूटते नहीं, नष्ट होकर घुल जाते हैं।
यहां दिए गए उदाहरण और कई अन्य उदाहरण जीवों के व्यक्तिगत विकास और उनके ऐतिहासिक विकास के बीच गहरे संबंध की ओर इशारा करते हैं। यह संबंध 19वीं सदी में एफ. मुलर और ई. हेकेल द्वारा तैयार किए गए बायोजेनेटिक कानून में व्यक्त किया गया है: प्रत्येक व्यक्ति का ओटोजेनेसिस (व्यक्तिगत विकास) उस प्रजाति के फाइलोजेनी (ऐतिहासिक विकास) की एक छोटी और तीव्र पुनरावृत्ति है जिससे यह व्यक्ति जुड़ा है। संबंधित है.
निष्कर्ष
सार पर काम पूरा करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि पुनरुत्पादन, या स्व-प्रजनन की क्षमता, जैविक प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रजनन बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों तक, बिना किसी अपवाद के सभी जीवित जीवों में निहित एक गुण है।
जानवरों और पौधों, बैक्टीरिया और कवक की किसी भी प्रजाति का अस्तित्व, मूल व्यक्तियों और उनकी संतानों के बीच निरंतरता प्रजनन के माध्यम से ही बनी रहती है। स्व-प्रजनन से निकटता से संबंधित जीवित चीजों की एक और संपत्ति है।जीवों का विकास. यहयह पृथ्वी पर सभी जीवन में भी अंतर्निहित है: सबसे छोटे एककोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय पौधे और जानवर।
ग्रन्थसूची
बोगेन जी. आधुनिक जीव विज्ञान। - एम.: मीर, 1970।
ग्रीन एन., स्टाउट डब्ल्यू., टेलर डी. बायोलॉजी: 3 खंडों में। टी. 3: ट्रांस। अंग्रेजी/एड से. आर. सोपर. - एम.: मीर, 1990।
ममोनतोव एस.जी. जीवविज्ञान। सामान्य पैटर्न. एम.: बस्टर्ड, 2002.
जानवरों से इंसानों तक. एम.: नौका, 1971.
स्ल्युसारेव ए.ए. सामान्य आनुवंशिकी के साथ जीव विज्ञान। - एम.: मेडिसिन, 1978।
व्याख्यान संख्या 3 ओटोजेनेसिस
1. युग्मकजनन
2. भ्रूण काल
3. भ्रूणोत्तर काल
ओटोजेनेसिस- युग्मनज से जैविक मृत्यु तक किसी जीव का व्यक्तिगत विकास। progenesis- ओटोजेनेसिस से पहले की अवधि में गैमेटोजेनेसिस और निषेचन शामिल है। मनुष्य का बढ़ाव-प्रजातियों का विकासवादी विकास।
मनुष्य की विशेषता यौन प्रजनन है; इसकी विशेषता है: गोनाड, युग्मक की उपस्थिति, निषेचन की प्रक्रिया, और यौन द्विरूपता।
युग्मकजनन -जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया ओवोजेनेसिस -अंडाणु परिपक्वता, शुक्राणुजनन– शुक्राणु. युग्मकजनन शरीर के जननग्रंथियों में होता है। युग्मक भ्रूण उपकला कोशिकाओं से बनते हैं, जो जीव के विकास की भ्रूण अवधि के दौरान बनते हैं।
निर्माण की प्रक्रिया में, रोगाणु कोशिकाएं तीन चरणों से गुजरती हैं:
1. प्रजनन अवधि (भ्रूण उपकला की कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं);
2. विकास काल;
3. परिपक्वता की अवधि में, कोशिकाएं अर्धसूत्रीविभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है (चित्र 5)।
चावल। 5. जनन कोशिकाओं का विभाजन
शुक्राणु वृषण की वीर्य नलिकाओं में परिपक्व होते हैं। वीर्य नलिकाओं के बीच स्थित है अंतरालीय ऊतक, पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन - टेस्टोस्टेरोन. पुरुष सेक्स हार्मोन - एण्ड्रोजन, प्रजनन कार्य, युग्मकजनन और माध्यमिक यौन विशेषताओं के गठन को विनियमित करें। शुक्राणु 70 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। वीर्य नलिकाओं में परिपक्वता के विभिन्न चरणों में युग्मक होते हैं। 5 मिली में. मानव वीर्य द्रव में 12 मिलियन शुक्राणु होते हैं। वे नकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं, चार्ज उन्हें एक साथ चिपकने से रोकता है। नर युग्मकों की बड़ी संख्या जैविक रूप से समीचीन है; उनकी संख्या में 40% की कमी से निषेचन की प्रक्रिया असंभव हो जाती है। शुक्राणु छोटी, गतिशील कोशिकाएं होती हैं जिनमें सिर, गर्दन और पूंछ होती है। सिर पर है एक्रोसोम,एक संशोधित लाइसोसोम, इसमें एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान अंडे की झिल्ली को भंग कर देते हैं। जीवन प्रत्याशा 6 से 72 घंटे तक है।
ओोजेनेसिस महिला शरीर के विकास के भ्रूण काल में शुरू होता है। अर्धसूत्रीविभाजन के पहले विभाजन के प्रोफ़ेज़ चरण में, जब संयुग्मन और क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक अस्थायी विराम होता है। लड़की के यौवन के दौरान अंडे का आगे का विकास फिर से शुरू होता है। महिला सेक्स हार्मोन के प्रभाव में - एस्ट्रोजेन, एक कूप, एक सेलुलर पुटिका जो कोशिका की रक्षा और पोषण करती है, पहले क्रम के अंडाणु के चारों ओर बनती है।
जैसे ही कूप परिपक्व होता है, यह अंडाशय के किनारे तक चला जाता है और फिर फट जाता है; अंडे के विकास के इस चरण को डिम्बग्रंथि या कूपिक कहा जाता है; यह 12 दिनों तक रहता है। कूप के टूटने और अंडाशय से पेट की गुहा में अंडे के निकलने को ओव्यूलेशन कहा जाता है।
ओव्यूलेशन के बाद निषेचन संभव है। मादा युग्मक को फैलोपियन ट्यूब के फ़िम्ब्रिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। सिलिअटेड एपिथेलियम की मदद से, यह गर्भाशय में चला जाता है, गर्भाशय चरण 12-14 दिनों तक रहता है। इस समय तक, महिला सेक्स हार्मोन के प्रभाव में, गर्भाशय उपकला ढीली हो जाती है। यदि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की दीवारों की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन के परिणामस्वरूप उपकला और अंडे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को मेन्सिस कहा जाता है और यह 3-4 दिनों तक चलती है। इस प्रकार, कूप निर्माण की शुरुआत से मासिक धर्म की शुरुआत तक का समय 20-30 दिन है और इसे डिम्बग्रंथि-मासिक चक्र कहा जाता है। (चित्र 6)।

चावल। 6. ओव्यूलेशन और अंडे का गर्भाशय में प्रत्यारोपण
इसमें शामिल है डिम्बग्रंथि चरण, गर्भाशय और मासिक धर्म।डिम्बग्रंथि-मासिक धर्म चक्र के दौरान, एक महिला की संपूर्ण प्रजनन प्रणाली का पुनर्निर्माण होता है, हार्मोन की गुणात्मक और मात्रात्मक संरचना बदल जाती है, प्रदर्शन, शक्ति, लचीलापन और सहनशक्ति बदल जाती है। प्रशिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करते समय महिला शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।
निषेचन- यह एक अंडे और एक शुक्राणु का संलयन है। निषेचन के तीन चरण हैं:
1) एक्रोसोमल प्रतिक्रिया (20 सेकंड) - एक्रोसोम एंजाइम द्वारा अंडे के खोल का विघटन और अंडे में शुक्राणु का प्रवेश। ऐसा माना जाता है कि जो शुक्राणु अंडे की झिल्ली पर सबसे बड़ी प्रवेश क्षमता (उत्तेजना) पैदा करता है वह अंडे में प्रवेश करता है;
2) अस्थायी विराम - अंडे में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं होता है, चयापचय बढ़ जाता है;
3) अंडे और शुक्राणु के नाभिक का संलयन, गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की बहाली।
निषेचन फैलोपियन ट्यूब के ऊपरी तीसरे भाग में होता है। निषेचित अंडा कहा जाता है युग्मनज. युग्मनज के निर्माण के साथ, मानव ओण्टोजेनेसिस शुरू होता है।
2. ओटोजेनेसिसमानव में दो चरण शामिल हैं: भ्रूणीय और पश्च-भ्रूणिक।
विकास की भ्रूणीय अवस्थायुग्मनज से जन्म तक जारी रहता है। चरण शामिल हैं: जाइगोट, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, हिस्टोजेनेसिस, ऑर्गोजेनेसिस।
युग्मनज- माइटोसिस द्वारा बार-बार विभाजित होता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुकोशिकीय एकल-परत भ्रूण का निर्माण होता है - ब्लासटुला. ब्लास्टुला आकार में नहीं बढ़ता है, क्योंकि इस समय यह फैलोपियन ट्यूब में होता है और इसे गर्भाशय में स्वतंत्र रूप से जाना चाहिए। छठे दिन, यह गर्भाशय में प्रवेश करता है और इसकी दीवार से जुड़ जाता है, ढीले उपकला में डूब जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दाखिल करना. भ्रूण का विकास जारी रहता है और वह पहले दो, फिर तीन परतों वाला हो जाता है। विकास के इस चरण में इसे कहा जाता है गेसट्रुला. परिणामस्वरूप, तीन रोगाणु परतें बनती हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। भ्रूणीय प्रणालियों से ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है।
इस प्रकार: ब्लासटुला– एकल-परत भ्रूण, गेसट्रुला- दो और तीन परत वाला भ्रूण। ऊतकजनन- रोगाणु परतों से ऊतकों का बिछाना। जीवोत्पत्ति- अंग बिछाने. 8 सप्ताह की आयु में मानव भ्रूण का द्रव्यमान 4 ग्राम, आकार 5 मिमी होता है। इस समय तक, वह रचनात्मक प्रक्रियाओं से गुजर चुके थे और मानव शरीर की रूपरेखा प्राप्त कर चुके थे। गर्भावस्था के आठ सप्ताह के बाद मानव भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है।
मानव भ्रूण के विकास के दौरान, अनंतिम प्राधिकारी,जो जन्म के बाद अपना कार्य खो देते हैं। अनंतिम अधिकारियों में शामिल हैं: जीवाणु-संबंधीसीपियाँ, कोरियोन, एमनियन और प्लेसेंटा, गर्भनाल. नालबच्चे और माँ की केशिकाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क सुनिश्चित करता है। विकासशील जीव प्लेसेंटा के माध्यम से पोषक तत्व, ऑक्सीजन, एंटीबॉडी प्राप्त करता है और चयापचय उत्पादों को हटा देता है। प्लेसेंटा एक अवरोधक कार्य करता है, भ्रूण को सूक्ष्मजीवों, कुछ दवाओं और विषाक्त पदार्थों से बचाता है (चित्र 7)।

चावल। 7. नाल
1 - गर्भाशय; 2 - एमनियन; 3 - भ्रूण; 4 - एमनियोटिक द्रव; 5 - प्लेसेंटा; 6 - नाल की केशिकाएं; 7 - नसें; 8 - धमनियाँ
माँ के रक्त में मौजूद विषाक्त, मादक पदार्थों, शराब, निकोटीन के संपर्क में आने पर बच्चे के अंगों और ऊतकों के निर्माण की सूक्ष्म प्रक्रियाएँ बाधित हो सकती हैं। मानव भ्रूण के विकास के विकारों को जन्मजात विकृति और विकृतियाँ कहा जाता है। इनमें शामिल हैं: "फांक तालु" (ऊपरी तालु की अनुपस्थिति), "फांक होंठ" (मैक्सिलरी हड्डियों का गैर-संलयन), पॉलीडेक्टली (अतिरिक्त उंगलियां), सिंडैक्टली (जुड़ी हुई उंगलियां)। जन्मजात विकृतियों का कारण बनने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों को कहा जाता है टेराटोजेनिक(विकृति उत्पन्न करना) (चित्र 8)।

चावल। 8. मानव शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक
मानव विकास की भ्रूण अवधि 36 सप्ताह तक रहती है।
3. जन्म के बाद और जैविक मृत्यु से पहले की अवधि को कहा जाता है प्रसवोत्तर.इसमें शामिल है किशोर, यौवनविकास और उम्र बढ़ने की अवधि.
किशोर - अवधियौवन से पहले. तरुणाई– यौवन की अवधि.
खेल अभ्यास, शरीर विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान में निम्नलिखित आयु अवधिकरण का उपयोग किया जाता है मनुष्यों का भ्रूणोत्तर ओटोजेनेसिस।
1 से 10 दिन की अवधि में बच्चे को बुलाया जाता है नवजात;
10 दिन से 1 वर्ष तक - छाती;
1 वर्ष से तीन वर्ष तक - अवधि बचपन;
4 से 7 वर्ष तक – पहला बचपन;
लड़कियों के लिए 8 साल से 12 साल तक और लड़कों के लिए 13 साल तक दूसरा बचपन;
लड़कियों के लिए 12 वर्ष से 15 वर्ष तक और लड़कों के लिए 13 से 16 वर्ष तक - किशोरों;
17-21 (लड़के), 16-20 वर्ष (लड़कियां) - किशोरावस्था;
महिलाओं के लिए 20-55 और पुरुषों के लिए 21-60 की अवधि तरुणाई(तरुणाई);
55 और 60 से 70 तक - वृद्ध लोग;
70 से 90 तक बुजुर्ग आदमी;
90 से अधिक शतायु.
मानव ओण्टोजेनेसिस में हैं संवेदनशील और आलोचनात्मकअवधि.
महत्वपूर्ण अवधिव्यक्तिगत जीन और उनके परिसरों की बढ़ी हुई गतिविधि की विशेषता है जो शरीर के किसी भी लक्षण के विकास को नियंत्रित करते हैं। इन अवधियों के दौरान, नियामक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन होता है, व्यक्तिगत अंगों और कार्यात्मक प्रणालियों के विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक छलांग होती है। इन अवधियों के दौरान, शरीर पर्यावरणीय कारकों के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ओटोजेनेसिस की महत्वपूर्ण अवधियों को आरोपण, प्लेसेंटेशन, अक्षीय अंगों का निर्माण, तंत्रिका और आंतों की नलियाँ, नॉटोकॉर्ड, हृदय निर्माण और अन्य माना जाता है।
यदि कोई महिला गर्भावस्था के तीसरे और नौवें सप्ताह के बीच रूबेला से संक्रमित हो जाती है, तो भ्रूण में हृदय रोग, मोतियाबिंद और बहरापन जैसे दोष विकसित होने का जोखिम होता है। अन्य समय में, रूबेला भ्रूण संबंधी विकृतियों का कारण नहीं बनता है।
संवेदनशील अवधि- ये आनुवंशिक नियंत्रण में कमी और शैक्षणिक और कोचिंग सहित पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति शरीर की व्यक्तिगत विशेषताओं की बढ़ती संवेदनशीलता की अवधि हैं। इस प्रकार, गति की गुणवत्ता के विभिन्न संकेतकों के प्रकट होने की संवेदनशील अवधि 11-14 वर्ष की आयु में होती है और 15 वर्ष की आयु तक इसका अधिकतम स्तर पहुँच जाता है, जब उच्च खेल उपलब्धियाँ संभव होती हैं। चपलता और लचीलेपन के गुणों की अभिव्यक्ति के लिए ओटोजेनेसिस में एक समान तस्वीर देखी जाती है।
शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षकों और शिक्षकों के लिए, संवेदनशील अवधियों का ज्ञान बहुत व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि संवेदनशील अवधियों के दौरान सबसे बड़ा प्रशिक्षण प्रभाव.
उन्हें इस आधार पर विभाजित किया जा सकता है कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कितनी कोशिकाएँ शामिल हैं: अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक कोशिका से एक बेटी की पीढ़ी उत्पन्न होती है: कोशिका विभाजन एकाधिक कोशिका विभाजन स्किज़ोगोनी स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन एककोशिकीय खमीर में नवोदित...
अपना काम सोशल नेटवर्क पर साझा करें
यदि यह कार्य आपको पसंद नहीं आता है, तो पृष्ठ के नीचे समान कार्यों की एक सूची है। आप खोज बटन का भी उपयोग कर सकते हैं
जीवों का प्रजनन एवं विकास
योजना
- प्रजनन की अवधारणा और अर्थ.
- प्रजनन के रूप और प्रकार।
- कोशिका चक्र। माइटोसिस। अर्धसूत्रीविभाजन.
- युग्मकों की संरचना. युग्मकजनन।
1. पुनरुत्पादन की अवधारणा एवं अर्थ
जीवित चीजों के गुणों में से एक हैविसंगति, वे। संगठन के किसी भी स्तर पर, जीवित पदार्थ का प्रतिनिधित्व प्राथमिक संरचनात्मक इकाइयों द्वारा किया जाता है। किसी प्रजाति का प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, और प्रजाति का अस्तित्व बना रहता हैप्रजनन जीव. इस प्रकार, जीवन की विसंगति उसके पुनरुत्पादन को मानती है, अर्थात्। प्रजनन प्रक्रिया.
प्रजनन यह जीवित प्राणियों की अपनी तरह का प्रजनन करने की क्षमता है। इससे जीवन की निरंतरता एवं निरन्तरता सुनिश्चित होती है। निरंतरता इस तथ्य से निर्धारित होती है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, आनुवंशिक सामग्री को माता-पिता से संतानों में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेटी जीवों में माता-पिता की विशेषताएं एक डिग्री या किसी अन्य तक प्रकट होती हैं।
प्रजनन मूल्य:
- किसी प्रजाति की संख्या बढ़ाना या बनाए रखना। प्रजनन के कारण न केवल प्रजनन (अर्थात अपनी ही तरह का प्रजनन) होता है, बल्कि जीवित जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
- जीवन की निरंतरता. प्रजनन के लिए धन्यवाद, व्यक्तियों के कम या ज्यादा बड़े समूह (उदाहरण के लिए, आबादी और प्रजातियां) काफी लंबे समय तक मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु के कारण उनकी संख्या में कमी की भरपाई जीवों के निरंतर प्रजनन से होती है और मृत बच्चों के स्थान पर नवजात शिशुओं को जन्म देना।
- पीढ़ियों के बीच निरंतरता. प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान, पैतृक पीढ़ी के व्यक्तियों से आनुवंशिक जानकारी प्रसारित होती है, जिससे विशिष्ट माता-पिता और संपूर्ण प्रजाति की विशेषताओं का पुनरुत्पादन सुनिश्चित होता है, जिससे जीव संबंधित है।
- जीवित चीजों के आनुवंशिकता और परिवर्तनशीलता जैसे गुणों का एहसास होता है।
2. प्रजनन के रूप और प्रकार
प्रजनन के दो मुख्य रूप हैं: लैंगिक और अलैंगिक।
असाहवासिक प्रजनन
अलैंगिक प्रजनन के दौरान, शरीर की विशिष्ट गैर-प्रजनन दैहिक कोशिकाओं से एक नया व्यक्ति प्रकट होता है। इसलिए, अलैंगिक प्रजनन में एक व्यक्ति शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन बड़ी संख्या में समान व्यक्तियों के प्रजनन को सुनिश्चित करता है, जो निरंतर परिस्थितियों में रहने वाली प्रजातियों के लिए फायदेमंद है। माँ के समान संतानों का तेजी से और असंख्य प्रजनन अलैंगिक प्रजनन का जैविक अर्थ है।
प्रकृति में, अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न विकल्प हैं:विभाजन, स्पोरुलेशन, विखंडन, नवोदित, वानस्पतिक प्रसार, क्लोनिंग।
अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में कितनी कोशिकाएँ शामिल हैं, इसके आधार पर उन्हें विभाजित किया जा सकता है:
- अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक कोशिका से पुत्री पीढ़ी उत्पन्न होती है:
- कोशिका विभाजन
- एकाधिक कोशिका विभाजन (स्किज़ोगोनी)
- स्पोरुलेशन (स्पोरुलेशन)
- एककोशिकीय जीवों में नवोदित होना (खमीर)
2) अलैंगिक प्रजनन, जो कोशिकाओं के समूह के विभाजन पर आधारित है:
- वनस्पतिक
- विखंडन
- बहुकोशिकीय जीवों में नवोदित (हाइड्रा)
एक और वर्गीकरण है, जिसके अनुसार अलैंगिक प्रजनन के विकल्प हैं:
- वानस्पतिक प्रसार (अर्थात् माँ के शरीर के अंगों द्वारा विभाजन):
विभाजन
एकाधिक विखंडन (स्किज़ोगोनी)
नवोदित
विखंडन
कलमों, बल्बों, पत्तियों, प्रकंदों द्वारा पौधे का प्रसार
- बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, अर्थात्। sporulation
आइए अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों को अधिक विस्तार से देखें।
विभाजन। अलैंगिक प्रजनन का सबसे सरल रूप. विभिन्न विभाजन विकल्प हैं:
- एक मूल जीव से दो पुत्री जीवों के निर्माण के साथ साधारण संकुचन द्वारा विभाजन। बैक्टीरिया और सायनोबैक्टीरिया की विशेषता.
- केन्द्रक के समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन जिसके बाद कोशिका द्रव्य का पृथक्करण होता है। एककोशिकीय जीवों की विशेषता (कई प्रोटोजोआ - अमीबा, हरा यूग्लीना, आदि; एककोशिकीय शैवाल - क्लैमाइडोमोनस, आदि)।
दोनों ही स्थितियों में ऐसा होता हैद्विआधारी विभाजन, यानी दो कोशिकाओं में. हालाँकि, एक अन्य विकल्प भी संभव है:
- एकाधिक विखंडन (स्किज़ोगोनी)। सबसे पहले, केन्द्रक बार-बार विभाजित होता है और फिर साइटोप्लाज्म भागों में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए, मानव एरिथ्रोसाइट्स में प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (मलेरिया का प्रेरक एजेंट) का प्रजनन। इस मामले में, प्लास्मोडिया कई बार नाभिक के बार-बार विभाजन से गुजरता है, जिसके बाद साइटोप्लाज्म विभाजित होता है। परिणामस्वरूप, 1 प्लाज़मोडियम 12-24 पुत्री जीवों को जन्म देता है।
बीजाणु निर्माण (स्पोरुलेशन). जीवित जीवों के बीच अलैंगिक प्रजनन की एक बहुत व्यापक विधि और लगभग सभी पौधों, कवक और कुछ प्रोटोजोआ (उदाहरण के लिए, स्पोरोज़ोअन प्रकार), साथ ही प्रोकैरियोटिक जीवों (कई बैक्टीरिया, नीले-हरे शैवाल) में पाई जाती है।
बीजाणु यह एक कोशिका है जो एक विकसित सुरक्षात्मक आवरण से ढकी होती है - एक बीजाणु झिल्ली, जो इसे विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का सामना करने की अनुमति देती है।अपने छोटे आकार के कारण, बीजाणु में आमतौर पर केवल न्यूनतम पोषक भंडार होते हैं. कई जीवों में, यह फैलाव की मुख्य इकाई है, क्योंकि बड़ी मात्रा में बनने वाले प्रकाश बीजाणु वायु द्रव्यमान और जल प्रवाह की गति से महत्वपूर्ण दूरी पर स्वतंत्र रूप से ले जाए जाते हैं।अक्सर, बीजाणु बड़ी मात्रा में बनते हैं और उनका वजन नगण्य होता है, जिससे उन्हें हवा के साथ-साथ जानवरों, मुख्य रूप से कीड़ों द्वारा फैलना आसान हो जाता है।
इसके अलावा, कुछ रूपों (प्रोटोजोआ, कवक) में, बीजाणु जीवन चक्र के एक विशेष चरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से "जीवित" रहने की अनुमति मिलती है।वास्तव में, जीवाणु बीजाणु प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए काम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवाणु केवल एक बीजाणु पैदा करता है। जीवाणु बीजाणु सबसे अधिक प्रतिरोधी होते हैं: उदाहरण के लिए, वे अक्सर मजबूत कीटाणुनाशक और पानी में उबालने से उपचार का सामना कर सकते हैं।
कई पौधों में बीजाणु बनने की प्रक्रिया(बीजाणुजनन) स्पोरैंगिया नामक विशेष थैली जैसी संरचनाओं में किया जाता है। फ्लैगेलर उपकरण की उपस्थिति के कारण बीजाणु या तो गतिशील हो सकते हैं (इस मामले में उन्हें कहा जाता है)।ज़ोस्पोरेस), और गतिहीन, सक्रिय रूप से चलने की क्षमता से वंचित।
कुछ हरे शैवालों में ज़ोस्पोर्स देखे जाते हैं। जानवरों में, मलेरिया प्लास्मोडियम और स्पोरोज़ोअन (एककोशिकीय जीव) के एक पूरे समूह में स्पोरुलेशन देखा जाता है।
नवोदित. यह एककोशिकीय जीवों में पाया जाता है, उदाहरण के लिए, यीस्ट और कुछ प्रकार के सिलिअट्स में, और बहुकोशिकीय जीवों में, उदाहरण के लिए, कोइलेंटरेट प्रकार (हाइड्रा) के प्रतिनिधियों में, साथ ही ट्यूनिकेट्स (क्लास एस्किडियन) में भी।
एककोशिकीय जीवों के लिए, इस विधि में मातृ कोशिका पर एक केंद्रक के साथ एक ट्यूबरकल (बहिर्वाह) का निर्माण होता है, जो फिर अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है।
बहुकोशिकीय जीवों के लिए, इस विधि में यह तथ्य शामिल है कि पहले मातृ जीव के शरीर पर एक छोटा सा ट्यूबरकल दिखाई देता है, जो आकार में बढ़ता है, फिर मातृ जीव की सभी संरचनाओं और अंगों की शुरुआत दिखाई देती है। तब पुत्री व्यक्ति का वियोग (नवोदित) होता है। इसके बाद, युवा, नया अलग हुआ जीव बढ़ता है और मूल नमूने के आकार तक पहुंच जाता है।
चावल। सहसंयोजक (हाइड्रा) में मुकुलन, 1 वयस्क जीव, 2 पुत्री नवोदित जीव।
एक रसीले पौधे में नवोदित होने का एक असामान्य रूप वर्णित हैब्रायोफिलम - जेरोफाइट, अक्सर एक सजावटी हाउसप्लांट के रूप में उगाया जाता है: छोटी जड़ों से सुसज्जित लघु पौधे इसकी पत्तियों के किनारों पर विकसित होते हैं; ये "कलियाँ" अंततः गिर जाती हैं और स्वतंत्र पौधों के रूप में अस्तित्व में आने लगती हैं।
विखंडन किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन, जिनमें से प्रत्येक एक नए जीव में विकसित होता है। उदाहरण के लिए, स्पाइरोगाइरा जैसे फिलामेंटस शैवाल में विखंडन होता है। स्पाइरोगाइरा फिलामेंट किसी भी स्थान पर दो भागों में टूट सकता है, जिससे बाद में दो जीवों का निर्माण होता है।
विखंडन कुछ निचले जानवरों में भी देखा जाता है, जो अधिक उच्च संगठित रूपों के विपरीत, अपेक्षाकृत खराब विभेदित कोशिकाओं से पुनर्जीवित होने की महत्वपूर्ण क्षमता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, नेमर्टियंस (आदिम कीड़ों का एक समूह, मुख्य रूप से समुद्री) का शरीर विशेष रूप से आसानी से कई हिस्सों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक पुनर्जनन के परिणामस्वरूप एक नए व्यक्ति को जन्म दे सकता है। इस मामले में, पुनर्जनन एक सामान्य और विनियमित प्रक्रिया है; हालाँकि, कुछ जानवरों (उदाहरण के लिए, स्टारफ़िश) में, अलग-अलग हिस्सों की बहाली आकस्मिक विखंडन के बाद ही होती है। विखंडन स्पंज, कोइलेंटरेट्स (हाइड्रा), जेलिफ़िश, इचिनोडर्म, एनेलिड्स और फ्लैटवर्म में देखा जाता है। कभी-कभी यह क्षमता इतनी अच्छी तरह से विकसित होती है कि एक पूरे व्यक्ति को एक अलग टुकड़े से बहाल किया जाता है।
चावल। . एक किरण से तारामछली का पुनर्जनन। ए, बी, सी पुनर्जनन के क्रमिक चरण
वनस्पति प्रचारयह प्रजनन है, जिसमें मातृ जीव से अलग हुए एक भाग से एक नया पुत्री जीव विकसित होता है। इस मामले में, एक काफी अच्छी तरह से विभेदित हिस्सा मातृ नमूने से अलग हो जाता है, जो आगे चलकर एक स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होता है। या पौधा विशेष रूप से वानस्पतिक प्रसार के लिए डिज़ाइन की गई विशेष संरचनाएँ बनाता है। उदाहरण के लिए, बल्ब, कंद, कॉर्म, प्रकंद, टेंड्रिल, कलियाँ। इनमें से कुछ संरचनाएँ पोषक तत्वों को संग्रहीत करने का काम भी करती हैं, जिससे पौधे को ठंड या सूखे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अनुमति मिलती है। वानस्पतिक प्रसार पौधों के कई समूहों की विशेषता है, शैवाल से लेकर फूल वाले पौधों तक।
सिद्धांत रूप में, वानस्पतिक प्रसार व्यावहारिक रूप से विखंडन या नवोदित से अलग नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से यह शब्द पौधों के जीवों और केवल कभी-कभी जानवरों पर लागू होता है, विखंडन और नवोदित के विपरीत।
क्लोनिंग. यह प्रजनन की एक कृत्रिम विधि है जो प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। यह पिछले 30-40 वर्षों में ही व्यापक हो गया है और इसका उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए तेजी से किया जा रहा है। ऐसी कई विशेष तकनीकें हैं जो आपको कुछ पौधों और जानवरों का क्लोन बनाने की अनुमति देती हैं।क्लोन अलैंगिक प्रजनन की एक या किसी अन्य विधि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति से प्राप्त आनुवंशिक रूप से समान संतानों को संदर्भित करता है। यहीं से इस विधि का नाम आता है।
क्लोनिंग प्रयोग विशेष रूप से पौधों पर व्यापक रूप से किए जाते हैं, जो उनकी पुनर्जीवित करने की उच्च क्षमता के कारण होता है। व्यक्तिगत कोशिकाओं को पोषक मीडिया पर रखा जाता है जहां वे विभाजित होते हैं और, विशेष तकनीकों का उपयोग करके, कोशिकाओं का एक अव्यवस्थित द्रव्यमान प्राप्त होता है, याघट्टा. फिर वे प्राथमिक सजातीय कैली के विभेदन और विभिन्न ऊतकों और अंगों के निर्माण का कारण बनते हैं और अंततः, एक संपूर्ण पौधे जीव में मूल के समान सभी गुण होते हैं, जहां से कोशिकाएं ली गई थीं।
क्लोनिंग विधि का उपयोग करके विभिन्न संकर रूप प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार, एंजाइमों या अल्ट्रासाउंड की मदद से, पौधों की कोशिकाओं की कोशिका दीवारों को हटा दिया जाता है, जिसके बाद परिणामी "नग्न" प्रोटोप्लास्ट विलय हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संकर कोशिकाएं (उदाहरण के लिए, टमाटर-आलू या तंबाकू-पेटुनिया संकर) बन सकती हैं। इसके बाद, कोशिका की दीवारें बहाल हो जाती हैं, कैलस बनता है, और फिर एक संपूर्ण संकर पौधा बनता है।
जानवरों के मामले में, निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है: अंडे के केंद्रक को हटा दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, और दैहिक कोशिका (उदाहरण के लिए, एक उपकला कोशिका) के केंद्रक को उसके स्थान पर रख दिया जाता है। भविष्य में, ऐसे अंडे से एक जीव प्राप्त किया जा सकता है जो पशु नाभिक दाता की विशेषताओं के समान है। इस तरह, आप कुछ जानवरों के पंजे वाले मेंढकों के क्लोन प्राप्त कर सकते हैं(ज़ेनोपस), न्यूट्स (ट्रिटुरस)। वर्तमान में, स्तनधारियों के क्लोन भी प्राप्त किए गए हैं, जैसे कि प्रसिद्ध भेड़ डॉली। क्लोनिंग तकनीकों का विकास जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा - जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है, जिसके कार्य यहीं तक सीमित नहीं हैं।
यौन प्रजनन
यौन प्रजननविशिष्ट जनन कोशिकाओं के संलयन के आधार पर पीढ़ियों के परिवर्तन और जीवों के विकास को कहा जाता है (युग्मक ) और युग्मनज का निर्माण। युग्मक (महिला और पुरुष, अंडाणु और शुक्राणु) का निर्माण गोनाड में होता है।
लैंगिक प्रजनन अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए विशिष्ट है, अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक प्रगतिशील है और इसमें भारी आनुवंशिक लाभ हैं। यौन प्रजनन संतानों की आनुवंशिक विविधता को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करता है, क्योंकि ऐसे जीनों का एक संयोजन है जो पहले माता-पिता दोनों के थे। प्रजातियों को बनाने वाले व्यक्तियों के जीनोटाइप की विविधता बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजातियों के अधिक सफल और तेजी से अनुकूलन की संभावना प्रदान करती है।
निषेचन के दौरान, युग्मक विलीन होकर द्विगुणित बनाते हैंयुग्मनज जिससे विकास की प्रक्रिया में एक परिपक्व जीव प्राप्त होता है। युग्मक अगुणित होते हैं - उनमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है, जिसमें गुणसूत्रों का दोहरा सेट होता है। यह भविष्य के जीव की पहली कोशिका है।
युग्मक आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं - नर और मादा। यदि प्रजाति है तो इनका उत्पादन नर और मादा माता-पिता द्वारा किया जाता हैद्विअर्थी; ( ऐसे कुछ फूल वाले पौधे, अधिकांश जानवर और मनुष्य) या एक ही व्यक्ति (हर्माफ्रोडाइटिज़्म) द्वारा होते हैं।
नर और मादा पशुओं के लिए विशेषतायौन द्विरूपता- अर्थात। संरचना, रूप (आकार, रंग और अन्य गुण), साथ ही व्यवहार में लैंगिक अंतर। जानवरों में, यह पहले से ही विकासवादी विकास के निचले चरणों में होता है, उदाहरण के लिए, गोल हेल्मिन्थ और आर्थ्रोपोड में, और कशेरुक में इसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तक पहुंचता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच बाहरी अंतर बहुत अभिव्यंजक होते हैं। उन प्रजातियों के पौधों में जिनमें नर और मादा व्यक्तियों की उपस्थिति की विशेषता होती है, यौन द्विरूपता भी होती है, लेकिन यह बहुत कम व्यक्त होती है।
यौन और अलैंगिक प्रजनन की तुलना तालिका में दी गई है। 5
मेज़ 5
अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन की तुलना
|
असाहवासिक प्रजनन |
यौन प्रजनन (बैक्टीरिया को छोड़कर) |
|
|
एक माता - पिता |
आमतौर पर दो माता-पिता |
|
|
युग्मक नहीं बनते |
अगुणित युग्मक बनते हैं, जिनके नाभिक संलयन (निषेचन) से एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं |
|
|
कोई अर्धसूत्रीविभाजन नहीं |
जीवन चक्र के कुछ चरण में, अर्धसूत्रीविभाजन होता है, जो प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों को दोगुना होने से रोकता है। |
|
|
संतानें अपने माता-पिता के समान होती हैं. आनुवंशिक भिन्नता का एकमात्र स्रोत यादृच्छिक उत्परिवर्तन है |
वंशज एक जैसे नहीं हैं अभिभावक व्यक्ति. वे आनुवंशिक पुनर्संयोजन के परिणामस्वरूप आनुवंशिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं. यह सबसे मजबूत और योग्यतम व्यक्तियों के प्राकृतिक चयन को बढ़ावा देता है, और, परिणामस्वरूप, विकास को। |
|
|
पौधों, कुछ निचले जानवरों और सूक्ष्मजीवों की विशेषताएँ। ऊंचे जानवरों में नहीं पाया जाता |
अधिकांश पौधों और जानवरों की विशेषता |
|
|
अक्सर बड़ी संख्या में वंशजों का तेजी से निर्माण होता है |
संख्या में कम तेजी से वृद्धि |
यौन प्रजनन, आकार और कार्य में रोगाणु कोशिकाओं के अनुपात के आधार पर, तीन विकल्पों में हो सकता है:
आइसोगैमी (शैवाल, प्रोटोजोआ)। नर और मादा प्रजनन कोशिकाएं आकार, संरचना और गतिशीलता में समान होती हैं।
विषमलैंगिकता। कोशिकाएँ आकार और संरचना में भिन्न होती हैं।
ऊगामी। यह विषमलैंगिकता के प्रकारों में से एक है, जब अंडाणु बड़ा और गतिहीन होता है, और शुक्राणु आकार में छोटा होता है, उसमें गति का एक अंग होता है और उसमें गतिशीलता होती है।
लैंगिक प्रजनन के विशेष रूप हैं, जैसे उभयलिंगीपन और अनिषेकजनन।
उभयलिंगीपन। शब्द "हेर्मैप्रोडिटिज़्म" ग्रीक नामों हर्मीस (पुरुष सौंदर्य का देवता) और एफ़्रोडाइट (महिला सौंदर्य की देवी) का संयोजन है।
हालाँकि, अधिकांश उभयलिंगी प्रजातियों में, निषेचन में विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त युग्मक शामिल होते हैं, और उनमें कई आनुवंशिक, रूपात्मक और शारीरिक अनुकूलन होते हैं जो स्व-निषेचन को रोकते हैं और क्रॉस-निषेचन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, कई प्रोटोजोआ में स्व-निषेचन को आनुवंशिक असंगति के कारण रोका जाता है, कई फूल वाले पौधों में एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम की संरचना के कारण, और कई जानवरों में इस तथ्य के कारण कि अंडे और शुक्राणु एक ही व्यक्ति में अलग-अलग समय पर बनते हैं।
सच्चे उभयलिंगीपन की घटना अधिक संगठित प्राणियों में भी पाई जाती है। विशेषकर यह स्तनधारियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, सूअरों में, कभी-कभी शरीर के एक तरफ अंडाशय का विकास देखा जाता है, और दूसरी तरफ वृषण (वृषण) का विकास, या संयुक्त संरचनाओं (ओवोटेस्टिस) का विकास होता है, और दोनों ही मामलों में कार्यात्मक रूप से संश्लेषण होता है। अंडे और शुक्राणु सक्रिय होते हैं। ऐसे जानवरों को "मध्यवर्ती" लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मध्यवर्ती यौन प्रकार के अधिकांश व्यक्ति दो XX गुणसूत्र वाली मादाएं हैं। इसी तरह की घटना बकरियों में भी देखी गई है।
सच्चा उभयलिंगीपन मनुष्यों में भी होता है, जो विकास संबंधी विकारों के परिणामस्वरूप होता है। उभयलिंगी जीवों के जीनोटाइप 46XX या 46 हैं XY , अधिकांश मामलों का जिक्र करते हुए XX (लगभग 60%). गलत उभयलिंगीपन को भी जाना जाता है, जब व्यक्तियों में बाहरी जननांग और दोनों लिंगों की माध्यमिक यौन विशेषताएं होती हैं, लेकिन केवल एक ही प्रकार की रोगाणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं - पुरुष या महिला।
अधिकांश फूल वाले पौधों में उभयलिंगी फूल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक फूल में एक स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। इसी कारण सभी फूलों से फल विकसित होते हैं। गेहूँ, चेरी, सेब और कई अन्य पौधों की प्रजातियाँ उभयलिंगी हैं। उभयलिंगी के अलावा, विकास के दौरान, एक ही प्रजाति के भीतर लिंगों को अलग करने वाले पौधों का विकास हुआ, यानी, पौधों के एकलिंगी और द्विअर्थी पौधों का उदय हुआ। जिन पौधों में पिस्टिलेट (मादा) और स्टैमिनेट (नर) दोनों प्रकार के फूल होते हैं, उन्हें एकलिंगी कहा जाता है। एकलिंगी पौधों में फल केवल स्त्रीकेसर के फूलों से विकसित होते हैं। मक्का एकलिंगी हैककड़ी, कद्दू और अन्य। इसके विपरीत, डायोसियस पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पिस्टिलेट या स्टैमिनेट फूल (एक ही प्रजाति के भीतर) होते हैं। द्विअंगी पौधों में, केवल वे जिनमें स्त्रीकेसरीय फूल (मादा) होते हैं, फल लगते हैं। चिनार, स्ट्रॉबेरी और अन्य प्रकार के वुडी और शाकाहारी पौधे द्विअर्थी होते हैं।
पार्थेनोजेनेसिस (ग्रीक से।पार्थेनोस कुंवारी औरउत्पत्ति जन्म) यौन प्रजनन के संशोधनों में से एक है जिसमें मादा युग्मक नर युग्मक द्वारा निषेचन के बिना एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। पार्थेनोजेनेसिस का लाभ यह है कि कुछ मामलों में यह प्रजनन की दर को बढ़ाता है, और सामाजिक कीड़ों में यह आपको प्रत्येक प्रकार के वंशजों की संख्या को विनियमित करने की अनुमति देता है। पार्थेनोजेनेसिस बाध्यकारी (अनिवार्य) और ऐच्छिक (वैकल्पिक) हो सकता है।
उदाहरण के लिए, शहद की मक्खी में(एपिस मेलिफ़ेरा) रानी निषेचित अंडे देती है(2पी = 32), जो विकसित होने पर मादाओं (रानियों या श्रमिकों) और अनिषेचित अंडों को जन्म देती हैं(पी = 16), जो नर (ड्रोन) उत्पन्न करते हैं जो अर्धसूत्रीविभाजन के बजाय समसूत्रण द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं।
चावल। अनिषेकजनन के प्रकारों की योजना।
- कोशिका चक्र। माइटोसिस। अर्धसूत्रीविभाजन
कोशिका विभाजन जीवों के प्रजनन और व्यक्तिगत विकास का आधार है।
सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। शरीर की विशिष्ट संरचना का विकास, वृद्धि और गठन एक या मूल कोशिकाओं के समूह के प्रजनन के माध्यम से किया जाता है। जीवन की प्रक्रिया में, शरीर की कुछ कोशिकाएँ घिस जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और मर जाती हैं। संरचना और सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए, शरीर को पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का उत्पादन करना चाहिए। कोशिकाओं को बनाने का एकमात्र तरीका पिछली कोशिकाओं को विभाजित करना है।
कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। मानव शरीर में, लगभग 10 से मिलकर 13 कोशिकाएँ, उनमें से कई मिलियन को हर सेकंड विभाजित होना पड़ता है।
यूकेरियोटिक कोशिकाओं के विभाजन की तीन विधियों का वर्णन किया गया है:अमिटोसिस (प्रत्यक्ष विभाजन),पिंजरे का बँटवारा (अप्रत्यक्ष विभाजन) औरअर्धसूत्रीविभाजन (कमी प्रभाग).
अमितोसिस कोशिका विभाजन की एक अपेक्षाकृत दुर्लभ और कम अध्ययन की गई विधि। इसका वर्णन उम्र बढ़ने और रोगात्मक रूप से परिवर्तित कोशिकाओं के लिए किया जाता है। अमिटोसिस में, इंटरफ़ेज़ नाभिक को संकुचन द्वारा विभाजित किया जाता है, और वंशानुगत सामग्री का समान वितरण सुनिश्चित नहीं किया जाता है। अक्सर केन्द्रक कोशिकाद्रव्य के पृथक्करण के बिना ही विभाजित हो जाता है और द्विकेंद्रीय कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका जो अमिटोसिस से गुजर चुकी है वह बाद में सामान्य माइटोटिक चक्र में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाती है। इसलिए, अमिटोसिस, एक नियम के रूप में, मृत्यु के लिए अभिशप्त कोशिकाओं और ऊतकों में होता है, उदाहरण के लिए, स्तनधारियों के भ्रूण झिल्ली की कोशिकाओं में और ट्यूमर कोशिकाओं में।
पिंजरे का बँटवारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं को विभाजित करने की एक सार्वभौमिक विधि। पशु कोशिकाओं में इसकी अवधि लगभग 1 घंटा है। माइटोसिस एक सतत प्रक्रिया है, जिसे पारंपरिक रूप से चार चरणों में विभाजित किया गया है: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़।
किसी कोशिका के निर्माण और उसके संतति कोशिकाओं में विभाजन के बीच होने वाली घटनाओं के क्रम को कहा जाता हैकोशिका चक्र. इस चक्र में तीन मुख्य चरण होते हैं:
1. इंटरफ़ेज़। गहन संश्लेषण की अवधि औरविकास। कोशिका अपनी वृद्धि और अपने सभी अंतर्निहित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कई पदार्थों का संश्लेषण करती है। इंटरफ़ेज़ के दौरान, डीएनए प्रतिकृति होती है।
2. मिटोसिस। यह परमाणु विभाजन (कार्योकिनेसिस) की प्रक्रिया है, जिसमें क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बेटी कोशिकाओं के बीच गुणसूत्रों के रूप में पुनर्वितरित होते हैं।
3. साइटोकाइनेसिस दो संतति कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्म (साइटोकाइनेसिस) के विभाजन की प्रक्रिया है।
कोशिका चक्र की अवधि कोशिका के प्रकार और बाहरी कारकों जैसे तापमान, पोषक तत्व और ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। जीवाणु कोशिकाएं हर 20 मिनट में विभाजित हो सकती हैं, आंतों की उपकला कोशिकाएं - हर 8-10 में, प्याज की जड़ की नोक में कोशिकाएं - हर 20 घंटे में, और तंत्रिका तंत्र की कई कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती हैं।
समय के साथ प्रक्रियाओं के बीच संबंध दिखाया गया हैचावल।

चावल । कोशिका चक्र चरण
interphase कई अवधियों से मिलकर बनता है:जी 1, एस, जी 2.
अवधि जी 1 प्रीसिंथेटिक कहा जाता है. अवधि में सर्वाधिक परिवर्तनशील. इस समय, कोशिका में जैविक संश्लेषण प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, मुख्य रूप से संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रोटीन। कोशिका बढ़ती है और अगली अवधि के लिए तैयार होती है। इस अवधि के दौरान, गहन जैवसंश्लेषण प्रक्रियाएँ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट (पौधों में), एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी तंत्र, रिक्तिकाएं और पुटिकाओं का निर्माण। न्यूक्लियोलस आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का उत्पादन करता है; राइबोसोम बनते हैं; कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तीव्र सेलुलर चयापचय एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होता है। कोशिका विकास। ऐसे पदार्थों का निर्माण जो अगले चरण की शुरुआत को दबाते या उत्तेजित करते हैं।
अवधि एस सिंथेटिक कहा जाता है. यह माइटोटिक चक्र की मुख्य अवधि है। स्तनधारी कोशिकाओं को विभाजित करने में, यह लगभग 6 x 10 घंटे तक चलता है। यहां डीएनए प्रतिकृति होती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण, जो डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड से बंधता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड में बदल जाता है।
G2 अवधि कहलाती है पोस्टसिंथेटिकयह अपेक्षाकृत छोटा होता है, स्तनधारी कोशिकाओं में यह लगभग 2 x 5 घंटे का होता है। इस समय, सेंट्रीओल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की संख्या दोगुनी हो जाती है, सक्रिय चयापचय प्रक्रियाएं होती हैं, आगामी विभाजन के लिए प्रोटीन और ऊर्जा जमा होती है। कोशिका विभाजित होने लगती है। गहन जैवसंश्लेषण प्रक्रियाएँ होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का विभाजन। ऊर्जा भंडार में वृद्धि. सेंट्रीओल्स की प्रतिकृति (उन कोशिकाओं में जहां वे मौजूद हैं) और स्पिंडल गठन की शुरुआत
पिंजरे का बँटवारा सशर्त रूप से चार चरणों में विभाजित: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़
प्रोफेज़ . डीएनए सर्पिलीकरण शुरू होता है और नाभिक में धीरे-धीरे बढ़ता है। क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, दृश्यमान हो जाते हैं और एक विशिष्ट बाइक्रोमैटिड संरचना प्राप्त कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस धीरे-धीरे गायब हो जाता है। साइटोप्लाज्म में, सूक्ष्मनलिकाएं सेंट्रीओल्स के प्रत्येक जोड़े के चारों ओर उन्मुख होती हैं, जिससे स्पिंडल केंद्र बनते हैं। सेंट्रीओल्स अलग-अलग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूक्ष्मनलिकाएं कोशिका अक्ष के साथ विस्तारित होती हैं, और एक्रोमैटिन स्पिंडल का निर्माण शुरू होता है। परमाणु आवरण अलग-अलग छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ते हैं
मेटाफ़ेज़ . क्रोमोसोम अधिकतम सर्पिलीकृत होते हैं और इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके सेंट्रोमियर एक ही विमान में स्थित होते हैं - कोशिका भूमध्य रेखा का विमान। एक मेटाफ़ेज़ प्लेट बनती है। माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण पूरा हो जाता है। सेंट्रीओल्स विपरीत ध्रुवों पर जोड़े में स्थित होते हैं, और विभिन्न ध्रुवों से स्पिंडल धागे प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं।
एनाफ़ेज़ . यह माइटोसिस का सबसे छोटा चरण है। यहां, प्रत्येक गुणसूत्र का अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, धागों की कमी होती हैकोशिका के ध्रुवों की ओर क्रोमैटिड्स (बेटी क्रोमोसोम) का स्पिंडल और विचलन।
टीलोफ़ेज़ . पुत्री गुणसूत्र, एक क्रोमैटिड से मिलकर, कोशिका के ध्रुवों तक पहुँचते हैं। डीएनए जो उन्हें बनाता है वह विलुप्त होने लगता है, एक न्यूक्लियोलस प्रकट होता है, बेटी गुणसूत्रों के प्रत्येक समूह के चारों ओर एक परमाणु झिल्ली बनती है, और एक्रोमैटिन स्पिंडल के धागे धीरे-धीरे विघटित हो जाते हैं। परमाणु विखंडन पूरा हो गया है.
साइटोप्लाज्मिक विभाजन शुरू होता है(साइटोटॉमी) और पुत्री कोशिकाओं के बीच एक पट का निर्माण। पशु कोशिकाएँ साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को संकुचित करके साइटोटॉमी करती हैं। पौधों में कोशिका भूमध्य रेखा के तल में एक झिल्लीदार पट बनता है, जो पार्श्व में बढ़ता हुआ कोशिका भित्ति तक पहुँचता है। परिणामस्वरूप, दो पूर्णतः पृथक संतति कोशिकाएँ बनती हैं।
चलिए फॉलो करते हैं वंशानुगत सामग्री में परिवर्तनमाइटोटिक चक्र के दौरान. माइटोटिक चक्र की मुख्य घटनाएँ हैंडी एन ए की नकल इंटरफ़ेज़ में घटित होता है और वंशानुगत जानकारी की मात्रा दोगुनी हो जाती है, औरक्रोमैटिड पृथक्करण,माइटोसिस के एनाफ़ेज़ में होने वाली और बेटी कोशिकाओं के बीच वंशानुगत जानकारी का समान वितरण सुनिश्चित करना। वंशानुगत सामग्री विभिन्न संरचनात्मक रूपों में रहते हुए इन प्रक्रियाओं को अंजाम देती है। प्रतिकृति संश्लेषण होता हैइंटरफ़ेज़ क्रोमैटिन, इनजिसमें डीएनए अणु अपेक्षाकृत सर्पिलीकृत अवस्था में होता है। आनुवंशिक जानकारी का वितरण किया जाता हैसमसूत्री गुणसूत्र,जिसमें डीएनए अधिकतम सर्पिलीकृत होता है।
समसूत्री चक्र में वंशानुगत सामग्री की मात्रा भी बदलती रहती है। यदि किसी अगुणित समुच्चय में गुणसूत्रों की संख्या को अक्षर p से निरूपित किया जाता है (द्विगुणित समुच्चय में क्रमशः 2n), और DNA अणुओं की संख्या को अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता हैसाथ, तब माइटोटिक चक्र के विभिन्न चरणों में दैहिक कोशिका के केंद्रक के सूत्र में परिवर्तन का पता लगाना संभव है। पहलेएस -वह अवधि जब प्रत्येक गुणसूत्र में एक डीएनए अणु होता है, नाभिक में डीएनए की कुल मात्रा उसमें गुणसूत्रों की संख्या से मेल खाती है, और एक द्विगुणित कोशिका के सूत्र का रूप होता है 2पी2एस. प्रतिकृति के बाद, जब प्रत्येक गुणसूत्र का डीएनए दोगुना हो जाता है, तो नाभिक में डीएनए की कुल मात्रा दोगुनी हो जाती है और कोशिका सूत्र 2n4c का रूप ले लेता है। माइटोसिस के एनाफ़ेज़ में क्रोमैटिड पृथक्करण के परिणामस्वरूप, बेटी नाभिक को एकल-क्रोमैटिड गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट प्राप्त होता है। पुत्री कोशिकाओं का सूत्र पुनः बन जाता है 2पी2एस.
माइटोसिस का जैविक महत्वयह है कि विभाजन की इस पद्धति के परिणामस्वरूप, वंशानुगत जानकारी वाली कोशिकाएं बनती हैं जो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मातृ कोशिका की जानकारी के समान होती हैं। वंशानुगत सामग्री का समान वितरण माइटोटिक चक्र के इंटरफेज़ में डीएनए प्रतिकृति और गुणसूत्र दोहरीकरण की प्रक्रियाओं के साथ-साथ माइटोसिस के दौरान बेटी कोशिकाओं के बीच क्रोमैटिड के सर्पिलीकरण और समान वितरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। माइटोसिस कई कोशिका पीढ़ियों में कैरियोटाइप की स्थिरता के रखरखाव को सुनिश्चित करता है और शरीर की वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के साथ-साथ पुनर्जनन और अलैंगिक प्रजनन के लिए एक सेलुलर तंत्र के रूप में कार्य करता है।
कई पर्यावरणीय कारकों की कार्रवाई माइटोसिस के सामान्य पाठ्यक्रम को बाधित कर सकती है और गुणसूत्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, साथ ही शरीर की दैहिक कोशिकाओं में व्यक्तिगत गुणसूत्रों या संपूर्ण गुणसूत्र सेटों की संख्या में परिवर्तन भी कर सकती है। पैथोलॉजिकल मिटोज़ कई क्रोमोसोमल रोगों का कारण बन सकते हैं। पैथोलॉजिकल मिटोज़ विशेष रूप से अक्सर ट्यूमर कोशिकाओं में देखे जाते हैं।
मिटोसिस आरेख:
पिंजरे का बँटवारा
|
1. इंटरफ़ेज़ इसे अक्सर ग़लती से विश्राम अवस्था कहा जाता है। इंटरफ़ेज़ की अवधि भिन्न होती है और किसी दिए गए सेल के कार्य पर निर्भर करती है। यह वह अवधि है जिसके दौरान कोशिका सामान्यतः अंगकों का संश्लेषण करती है और आकार में बढ़ जाती है। न्यूक्लियोली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सक्रिय रूप से राइबोसोमल सामग्री को संश्लेषित करते हैं। कोशिका विभाजन से ठीक पहले, प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए और हिस्टोन की प्रतिकृति बनाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र को अब एक सेंट्रोमियर द्वारा एक दूसरे से जुड़े क्रोमैटिड्स की एक जोड़ी द्वारा दर्शाया जाता है। गुणसूत्रों का पदार्थ दागदार होता है और इसे क्रोमैटिन कहा जाता है, लेकिन इन संरचनाओं को स्वयं देखना मुश्किल होता है। |
|
|
2. प्रोफ़ेज़ आमतौर पर कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण। उनके सर्पिलीकरण और संघनन के परिणामस्वरूप क्रोमैटिड छोटे हो जाते हैं (उनकी मूल लंबाई का 4% तक) और मोटे हो जाते हैं। जब दाग लगाया जाता है, तो क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर दिखाई नहीं देते हैं। क्रोमैटिड के विभिन्न युग्मों में, सेंट्रोमियर अलग-अलग तरीके से स्थित होता है। पशु कोशिकाओं और निचले पौधों में, सेंट्रीओल्स कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर विचरण करते हैं। प्रत्येक सेंट्रीओल से, छोटी सूक्ष्मनलिकाएं किरणों के रूप में निकलती हैं, जो सामूहिक रूप से एक तारा बनाती हैं। न्यूक्लियोली छोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लिक एसिड आंशिक रूप से क्रोमैटिड के कुछ जोड़े में स्थानांतरित हो जाता है। प्रोफ़ेज़ के अंत में, परमाणु झिल्ली विघटित हो जाती है और एक विखंडन स्पिंडल बनता है। |
|
|
3. मेटाफ़ेज़ क्रोमैटिड के जोड़े अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल फिलामेंट्स (माइक्रोट्यूब्यूल्स) से जुड़े होते हैं और स्पिंडल के ऊपर और नीचे तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनके सेंट्रोमियर स्पिंडल के भूमध्य रेखा के साथ अपनी धुरी पर लंबवत नहीं हो जाते। |
|
|
4. एनाफ़ेज़ यह बहुत छोटी अवस्था है. प्रत्येक सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और स्पिंडल फिलामेंट्स बेटी सेंट्रोमियर को विपरीत ध्रुवों तक खींचते हैं। सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग हो चुके क्रोमैटिड्स को अपने पीछे खींचते हैं, जिन्हें अब क्रोमोसोम कहा जाता है। |
|
|
5. टेलोफ़ेज़ गुणसूत्र कोशिका ध्रुवों तक पहुँचते हैं, सर्पिल होते हैं, लम्बे होते हैं, और उन्हें अब स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। स्पिंडल तंतु नष्ट हो जाते हैं और सेंट्रीओल्स दोहराए जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों के चारों ओर एक केन्द्रक झिल्ली बनी होती है। न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट होता है। टेलोफ़ेज़ के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस (संपूर्ण कोशिका का दो भागों में विभाजन) हो सकता है। |
|
अर्धसूत्रीविभाजन (ग्रीक अर्धसूत्रीविभाजन से कमी) कोशिका विभाजन का एक अनोखा तरीका है, जिससे उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीविभाजन केंद्रीय कड़ी हैजानवरों में युग्मकजनन और बीजाणुजनन पौधों में. अर्धसूत्रीविभाजन में एकल डीएनए दोहराव से पहले दो क्रमिक विभाजन होते हैं। दोनों प्रभागों के लिए आवश्यक सभी पदार्थ और ऊर्जा अर्धसूत्रीविभाजन से पहले के इंटरफ़ेज़ के दौरान संग्रहीत होते हैंमैं। इंटरफेज़ II व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित, और विभाजन तेजी से एक के बाद एक आते जाते हैं। प्रत्येक अर्धसूत्रीविभाजन में, समान चार चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है: प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़, जो माइटोसिस की विशेषता हैं, लेकिन कई विशेषताओं में भिन्न हैं।
प्रथम अर्धसूत्रीविभाजन (अर्धसूत्रीविभाजन)।मैं ) गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और इसे कमी कहा जाता है। परिणामस्वरूप, एक द्विगुणित कोशिका से(2पी 4c) दो अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं(पी 2सी) कोशिकाएं।
प्रोफ़ेज़ I अर्धसूत्रीविभाजन सबसे लंबा और सबसे जटिल है। माइटोसिस के प्रोफ़ेज़ की विशिष्ट डीएनए हेलिक्सेशन और स्पिंडल गठन की प्रक्रियाओं के अलावा,मैं दो अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटनाएँ घटित होती हैं:संयुग्मन या सिनैप्सिस सजातीय गुणसूत्र औरबदलते हुए।
संयुग्मन समजातीय गुणसूत्रों की निकटता की प्रक्रिया है। ये युग्मित गुणसूत्र बनते हैंबीवालेन्त और विशेष प्रोटीन की सहायता से इसकी संरचना में बनाए रखा जाता है। चूँकि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं, एक द्विसंयोजक में चार क्रोमैटिड शामिल होते हैं और इसे द्विसंयोजक भी कहा जाता हैस्मरण पुस्तक। एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता हैपी द्विसंयोजक। संयुग्मन के बाद कोशिका सूत्र का रूप ले लेता हैउत्तीर्ण।
द्विसंयोजक के कुछ स्थानों में, संयुग्मित गुणसूत्रों के क्रोमैटिड संबंधित वर्गों को काटते, तोड़ते और आदान-प्रदान करते हैं। समजातीय गुणसूत्रों के टुकड़ों के आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह भविष्य के युग्मकों के गुणसूत्रों में पैतृक और मातृ जीन के नए संयोजनों के गठन को सुनिश्चित करता है। क्रॉसिंग ओवर कई क्षेत्रों (मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर) में हो सकता है, जिससे युग्मकों में वंशानुगत जानकारी का उच्च स्तर का पुनर्संयोजन होता है। प्रोफ़ेज़ के अंत तकमैं गुणसूत्र सर्पिलीकरण की डिग्री बढ़ जाती है, क्रोमैटिड स्पष्ट रूप से अलग-अलग हो जाते हैं, प्रत्येक ध्रुव से स्पिंडल धागे द्विसंयोजक गुणसूत्रों में से एक के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। परमाणु आवरण नष्ट हो जाता है, और द्विसंयोजक कोशिका के भूमध्यरेखीय तल की ओर निर्देशित हो जाते हैं।
मेटाफ़ेज़ I में अर्धसूत्रीविभाजन धुरी का निर्माण पूरा करता है, कोशिका के भूमध्यरेखीय तल में द्विसंयोजक स्थापित होते हैं। एक ध्रुव से स्पिंडल स्ट्रैंड प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं।
पश्च चरण I में अर्धसूत्रीविभाजन में, धुरी धागों की क्रिया के तहत, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। परिणामस्वरूप, कोशिका के प्रत्येक ध्रुव पर aअगुणित सेटगुणसूत्र, जिसमें समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े से एक बाइक्रोमैटिड गुणसूत्र होता है। पश्चावस्था मेंमैं विभिन्न युग्मों के गुणसूत्र, अर्थात्। गैर-समरूप गुणसूत्र एक-दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के गठन को सुनिश्चित किया जाता हैयुग्म भविष्य के युग्मकों के अगुणित सेट में पैतृक और मातृ गुणसूत्र। ऐसे संयोजनों की संख्या सूत्र 2 से मेल खाती हैपी, जहां पी समजातीय गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या. मनुष्यों में, यह मान 2 के बराबर है, अर्थात। 8.4 मानव युग्मकों में पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के संयोजन के 10 प्रकार संभव हैं।
तो, पश्चावस्था में समजात गुणसूत्रों का विचलनमैं अर्धसूत्रीविभाजन न केवल भविष्य की रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी सुनिश्चित करता है, बल्कि विभिन्न जोड़े के पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के यादृच्छिक संयोजन के कारण उत्तरार्द्ध की एक विशाल विविधता भी सुनिश्चित करता है।
टेलोफ़ेज़ I में अर्धसूत्रीविभाजन उन कोशिकाओं के निर्माण में होता है जिनके नाभिक में गुणसूत्रों का अगुणित समूह होता है और डीएनए की मात्रा दोगुनी होती है, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं। प्रथम अर्धसूत्रीविभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं का सूत्र होता हैपी2एस और एक छोटे अंतराल के बाद वे अगला विभाजन शुरू करते हैं।
दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन (अर्धसूत्रीविभाजन)।द्वितीय ) एक विशिष्ट माइटोसिस (चित्र 5.3) के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें भिन्नता है कि इसमें प्रवेश करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट होता है। इस विभाजन के परिणामस्वरूपपी बाइक्रोमैटिड क्रोमोसोम (आर2सी), विभाजन, रूपपी एकल क्रोमैटिड गुणसूत्र(पीएस). इस विभाजन को कहा जाता हैसंतुलन संबंधी (या बराबर करना)।
इस प्रकार, दो क्रमिक अर्धसूत्रीविभाजन के बाद, दो-क्रोमैटिड गुणसूत्रों (2x4c) के द्विगुणित सेट वाली एक कोशिका से, एकल-क्रोमैटिड गुणसूत्रों के अगुणित सेट वाली चार कोशिकाएं बनती हैं।(पीएस).
अर्धसूत्रीविभाजन का जैविक महत्वइसमें गुणसूत्रों के कम सेट के साथ कोशिकाओं का निर्माण और प्रजनन करने वाले जीवों की कई पीढ़ियों में कैरियोटाइप की स्थिरता बनाए रखना शामिल है। यौन संचारित। अर्धसूत्रीविभाजन संयोजनात्मक परिवर्तनशीलता के आधार के रूप में कार्य करता है, जो पैतृक और मातृ गुणसूत्रों के क्रॉसिंग ओवर, विचलन और संयोजन की प्रक्रियाओं के माध्यम से युग्मकों की आनुवंशिक विविधता प्रदान करता है। असमान क्रॉसिंग ओवर के कारण गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन, एनाफ़ेज़ में सभी या व्यक्तिगत गुणसूत्रों के विचलन में व्यवधानमैं और द्वितीय अर्धसूत्रीविभाजन से असामान्य युग्मकों का निर्माण होता है और यह जीव की मृत्यु या वंशजों में कई गुणसूत्र सिंड्रोम के विकास के आधार के रूप में काम कर सकता है।
पशु कोशिका में अर्धसूत्रीविभाजन के क्रमिक चरणों का आरेख और संक्षिप्त विवरण।
|
1. इंटरफ़ेज़ विभिन्न प्रजातियों में अवधि भिन्न-भिन्न होती है। ऑर्गेनेल प्रतिकृति होती है और कोशिका का आकार बढ़ जाता है। डीएनए और हिस्टोन की प्रतिकृति मुख्य रूप से प्रीमियोटिक इंटरफ़ेज़ में समाप्त होती है, लेकिन आंशिक रूप से प्रोफ़ेज़ की शुरुआत तक भी विस्तारित होती है। प्रत्येक गुणसूत्र को अब एक सेंट्रोमियर से जुड़े क्रोमैटिड्स की एक जोड़ी द्वारा दर्शाया जाता है। गुणसूत्र सामग्री दागदार है, लेकिन सभी संरचनाओं में से केवल न्यूक्लियोली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। |
ए. प्रारंभिक भविष्यवाणीमैं |
|
2. प्रोफ़ेज़ सबसे लंबा चरण. इसे अक्सर पांच चरणों (लेप्टोटिमा, जाइगोनेमा, पचाइनीमा, डिप्लोनेमा और डायाकाइनेसिस) में विभाजित किया जाता है, लेकिन यहां इसे गुणसूत्र परिवर्तनों का एक सतत क्रम माना जाएगा। ए . गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और अलग-अलग संरचनाओं के रूप में दिखाई देने लगते हैं। कुछ जीवों में, वे मोतियों की माला की तरह दिखते हैं: अत्यधिक दागदार सामग्री के क्षेत्र - क्रोमोमेरेस - गैर-दाग वाले क्षेत्रों के साथ वैकल्पिक होते हैं। क्रोमोमेरेस वे स्थान हैं जहां क्रोमोसोमल सामग्री अत्यधिक कुंडलित होती है। |
|
|
बी। मातृ और पितृ युग्मक के नाभिक से उत्पन्न होने वाले समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और संयुग्मित होते हैं। इन गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है, उनके सेंट्रोमियर एक ही स्थान पर होते हैं, और उनमें आमतौर पर समान रैखिक अनुक्रम में व्यवस्थित जीनों की समान संख्या होती है। समजातीय गुणसूत्रों के क्रोमोमेरेस एक दूसरे के बगल में स्थित होते हैं। संयुग्मन की प्रक्रिया गुणसूत्रों पर कई बिंदुओं पर शुरू हो सकती है, जो फिर पूरी लंबाई के साथ जुड़े होते हैं (जैसे कि एक साथ ज़िप किए गए हों)। संयुग्मित समजात गुणसूत्रों के जोड़े को अक्सर द्विसंयोजक कहा जाता है। द्विसंयोजक छोटे और मोटे हो जाते हैं। इस मामले में, आणविक स्तर पर सघन पैकिंग और बाहरी रूप से ध्यान देने योग्य घुमाव (सर्पिलीकरण) दोनों होते हैं। अब प्रत्येक गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। |
बी. प्रोफ़ेज़ I |
|
में। द्विसंयोजक बनाने वाले समजात गुणसूत्र आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, मानो एक दूसरे से दूर जा रहे हों। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं। गुणसूत्र अभी भी कई बिंदुओं पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को चियास्माटा (ग्रीक से) कहा जाता है। chiasma - पार करना)। प्रत्येक चियास्म में, क्रोमैटिड्स के वर्गों का आदान-प्रदान टूटने और पुनर्मिलन के परिणामस्वरूप होता है, जिसमें प्रत्येक चियास्म में मौजूद चार में से दो धागे शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप, एक गुणसूत्र (उदाहरण के लिए, पैतृक - ए, बी, सी) के जीन दूसरे गुणसूत्र (मातृ ए,बी , सी), जो परिणामी क्रोमैटिड में नए जीन संयोजन की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग के बाद समजात गुणसूत्र अलग नहीं होते हैं, क्योंकि बहन क्रोमैटिड (दोनों गुणसूत्रों के) एनाफेज तक मजबूती से जुड़े रहते हैं। |
बी. प्रोफ़ेज़ के दौरान पार करनामैं |
|
जी . समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, और द्विसंयोजक चियास्माटा की संख्या के आधार पर एक निश्चित विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। एक चियास्माटा वाले द्विसंयोजकों में एक क्रूसिफ़ॉर्म आकार होता है, दो चियास्माटा के साथ वे अंगूठी के आकार के होते हैं, और तीन या अधिक के साथ वे एक दूसरे के लंबवत स्थित लूप बनाते हैं। प्रोफ़ेज़ के अंत तक, सभी गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित और तीव्रता से रंजित हो जाते हैं। कोशिका में अन्य परिवर्तन होते हैं: सेंट्रीओल्स (यदि कोई हो) का ध्रुवों की ओर पलायन, न्यूक्लियोली और परमाणु झिल्ली का विनाश, और फिर स्पिंडल फिलामेंट्स का निर्माण। |
|
|
2. मेटाफ़ेज़ द्विसंयोजक भूमध्यरेखीय तल में पंक्तिबद्ध होकर एक मेटाफ़ेज़ प्लेट बनाते हैं। उनके सेंट्रोमियर एकल संरचनाओं के रूप में व्यवहार करते हैं (हालांकि वे अक्सर दोहरे दिखाई देते हैं) और उनसे जुड़े धुरी तंतुओं को व्यवस्थित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ध्रुवों में से केवल एक की ओर निर्देशित होता है। इन धागों के कमजोर खींचने वाले बल के परिणामस्वरूप, प्रत्येक द्विसंयोजक भूमध्य रेखा क्षेत्र में स्थित है, और इसके दोनों सेंट्रोमियर इससे समान दूरी पर हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर। |
डी. देर से मेटाफ़ेज़मैं |
|
3. एनाफ़ेज़ प्रत्येक द्विसंयोजक में मौजूद दो सेंट्रोमियर अभी तक विभाजित नहीं हुए हैं, लेकिन बहन क्रोमैटिड अब एक दूसरे से सटे नहीं हैं। स्पिंडल फिलामेंट्स सेंट्रोमर्स को खींचते हैं, जिनमें से प्रत्येक दो क्रोमैटिड्स से जुड़ा होता है, स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों की ओर। परिणामस्वरूप, गुणसूत्र दो अगुणित सेटों में विभाजित हो जाते हैं जो बेटी कोशिकाओं में समाप्त होते हैं। |
इ। एनाफ़ेज़ I |
|
4. टेलोफ़ेज़ विपरीत ध्रुवों पर समजात सेंट्रोमीटर और संबंधित क्रोमैटिड के विचलन का अर्थ है पहले अर्धसूत्रीविभाजन का पूरा होना। एक सेट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, लेकिन प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र दो क्रोमैटिड से बने होते हैं। चियास्माटा के निर्माण के दौरान क्रॉसिंग ओवर के कारण, ये क्रोमैटिड आनुवंशिक रूप से गैर-समान होते हैं, और दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान वे अलग हो जाएंगे। धुरी और उनके धागे आमतौर पर गायब हो जाते हैं। जानवरों और कुछ पौधों में, क्रोमैटिड्स स्पाइरल होते हैं, प्रत्येक ध्रुव पर उनके चारों ओर एक परमाणु झिल्ली बनती है, और परिणामस्वरूप नाभिक इंटरफेज़ में प्रवेश करता है। फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन (जानवरों में) या एक विभाजित कोशिका दीवार का निर्माण (पौधों में) शुरू होता है, जैसे माइटोसिस में। कई पौधों में, न तो टेलोफ़ेज़, न ही कोशिका भित्ति का निर्माण, न ही इंटरफ़ेज़ देखा जाता है, और कोशिका सीधे एनाफ़ेज़ से संक्रमण करती हैमैं भविष्यवाणी करने के लिए द्वितीय. |
जी. टेलोफ़ेज़ I एक पशु कोशिका में |
|
इंटरफेज़ II यह अवस्था आमतौर पर केवल पशु कोशिकाओं में ही देखी जाती है: इसकी अवधि अलग-अलग होती है।चरण एस अनुपस्थित है, और आगे कोई डीएनए प्रतिकृति नहीं होती है। अर्धसूत्रीविभाजन के दूसरे विभाजन में शामिल प्रक्रियाएं माइटोसिस में होने वाली प्रक्रियाओं के समान होती हैं। इनमें पहले अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप दोनों बेटी कोशिकाओं में क्रोमैटिड का पृथक्करण शामिल है। अर्धसूत्रीविभाजन का दूसरा विभाजन माइटोसिस से मुख्य रूप से दो तरीकों से भिन्न होता है: 1) मेटाफ़ेज़ मेंद्वितीय अर्धसूत्रीविभाजन, बहन क्रोमैटिड अक्सर एक दूसरे से दृढ़ता से अलग होते हैं; 2) गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। |
|
|
प्रोफ़ेज़ II उन कोशिकाओं में जो इंटरफ़ेज़ खो देती हैंद्वितीय , यह चरण भी गायब है। प्रोफ़ेज़ की अवधिद्वितीय टेलोफ़ेज़ की अवधि के व्युत्क्रमानुपातीमैं . न्यूक्लियोली और परमाणु झिल्ली नष्ट हो जाते हैं, और क्रोमैटिड छोटे और मोटे हो जाते हैं। सेंट्रीओल्स, यदि मौजूद हैं, तो कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं; धुरी तंतु दिखाई देते हैं। क्रोमैटिड्स को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उनकी लंबी कुल्हाड़ियाँ पहले अर्धसूत्रीविभाजन के स्पिंडल अक्ष के लंबवत होती हैं। |
जेड. प्रोफ़ेज़ पी |
|
मेटाफ़ेज़ II दूसरे विभाजन के दौरान, सेंट्रोमियर दोहरी संरचनाओं की तरह व्यवहार करते हैं। वे दोनों ध्रुवों की ओर निर्देशित स्पिंडल धागों को व्यवस्थित करते हैं, और इस प्रकार स्पिंडल को भूमध्य रेखा पर संरेखित करते हैं। |
मेटाफ़ेज़ II |
|
एनाफ़ेज़ II केंद्र ओमर विभाजित होता है, और स्पिंडल धागे उन्हें विपरीत ध्रुवों तक खींचते हैं। सेंट्रोमियर अलग-अलग क्रोमैटिड्स को अपने साथ खींचते हैं, जिन्हें अब क्रोमोसोम कहा जाता है। टेलोफ़ेज़ II यह चरण माइटोसिस के टेलोफ़ेज़ के समान है। गुणसूत्र विकृत हो जाते हैं, खिंच जाते हैं और फिर उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। स्पिंडल तंतु गायब हो जाते हैं और सेंट्रीओल्स दोहराने लगते हैं। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर, जिसमें अब मूल मूल कोशिका के गुणसूत्रों की आधी (अगुणित) संख्या होती है, एक परमाणु झिल्ली फिर से बनती है। साइटोप्लाज्म के बाद के विभाजन (जानवरों में) या कोशिका भित्ति (पौधों में) के परिणामस्वरूप, एक मूल मूल कोशिका से चार बेटी कोशिकाएँ प्राप्त होती हैं। |
|
माइटोसिस और अर्धसूत्रीविभाजन के चरणों के बीच अंतर
|
अवस्था |
पिंजरे का बँटवारा |
अर्धसूत्रीविभाजन |
|
प्रोफेज़ |
क्रोमोमेरेस दिखाई नहीं देते समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं चियास्माटा का निर्माण नहीं होता है क्रॉसिंग नहीं होती |
क्रोमोमेरेस दिखाई दे रहे हैं समजातीय गुणसूत्र संयुग्मित होते हैं। चियास्माटा का निर्माण होता है। पारगमन हो सकता है |
|
मेटाफ़ेज़ |
क्रोमैटिड जोड़े स्पिंडल भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं स्पिंडल भूमध्य रेखा पर सेंट्रोमियर एक ही तल में पंक्तिबद्ध होते हैं |
क्रोमैटिड्स के जोड़े केवल अर्धसूत्रीविभाजन के दूसरे भाग में स्पिंडल भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं अर्धसूत्रीविभाजन के प्रथम प्रभाग में सेंट्रोमियर भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे उससे समान दूरी पर स्थित होते हैं |
|
एनाफ़ेज़ |
सेंट्रोमियर विभाजित होते हैं। क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। अपसारी क्रोमैटिड समान होते हैं |
सेंट्रोमियर केवल अर्धसूत्रीविभाजन के दूसरे चरण में विभाजित होते हैं। अर्धसूत्रीविभाजन के दूसरे विभाजन के दौरान क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। प्रथम विभाजन में संपूर्ण गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के परिणामस्वरूप अपसारी गुणसूत्र समान नहीं हो सकते हैं |
|
टेलोलोफ़ेज़ |
पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिकाओं के समान ही होती है पुत्री कोशिकाओं में दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं (द्विगुणित में) |
पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है पुत्री कोशिकाओं में समजात गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही होता है |
|
इस प्रकार का विभाजन कहाँ होता है? |
अगुणित, द्विगुणित और बहुगुणित कोशिकाओं में संभव दैहिक कोशिकाओं और कुछ बीजाणुओं के निर्माण के दौरान, साथ ही पौधों में युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है जिसमें पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन होता है |
केवल द्विगुणित और बहुगुणित कोशिकाओं में गैमेटो- या स्पोरोजेनेसिस के दौरान |
- युग्मकों की संरचना. युग्मकजनन
यौन प्रजनन विशेष रोगाणु कोशिकाओं का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक कहलाते हैंअंडे, नर शुक्राणु.युग्मक मुख्य रूप से गुणसूत्रों की आधी संख्या के साथ-साथ चयापचय प्रक्रियाओं के निम्न स्तर के कारण दैहिक कोशिकाओं से भिन्न होते हैं।
बीजाणु अपेक्षाकृत बड़ी गैर-गतिशील कोशिकाएँ, आमतौर पर आकार में गोल; विशिष्ट अंगकों के अलावा, साइटोप्लाज्म में जर्दी के रूप में आरक्षित पोषक तत्वों का समावेश होता है (चावल .). अंडों के नाभिक में, राइबोसोमल जीन और एमआरएनए की कई प्रतियां बनती हैं, जो भविष्य के भ्रूण के महत्वपूर्ण प्रोटीन के संश्लेषण को सुनिश्चित करती हैं। विभिन्न जीवों के अंडों में जर्दी की मात्रा और वितरण की प्रकृति अलग-अलग होती है। अंडे कई प्रकार के होते हैं.

आइसोलेसीथलसमान रूप से वितरित जर्दी की थोड़ी मात्रा वाले अपेक्षाकृत छोटे अंडे कहलाते हैं। उनमें कोर केंद्र के करीब स्थित है। ऐसे अंडे कीड़े, बाइवाल्व और गैस्ट्रोपॉड, इचिनोडर्म और लांसलेट्स में पाए जाते हैं।मध्यम टेलोलेसीथलस्टर्जन और उभयचरों के अंडों का व्यास लगभग 1.5 × 2 मिमी होता है और इनमें औसत मात्रा में जर्दी होती है, जिसका बड़ा हिस्सा ध्रुवों (वानस्पतिक) में से एक पर केंद्रित होता है। विपरीत ध्रुव (जानवर) पर, जहां थोड़ी जर्दी होती है, वहां अंडे का केंद्रक होता है।
जोरदार टेलोलेसीथलकुछ मछलियों, सरीसृपों, पक्षियों और अंडे देने वाले स्तनधारियों के अंडों में बहुत अधिक मात्रा में जर्दी होती है, जो अंडे के साइटोप्लाज्म की लगभग पूरी मात्रा पर कब्जा कर लेती है। जंतु ध्रुव पर जर्दी रहित सक्रिय साइटोप्लाज्म वाली जर्मिनल डिस्क होती है। इन अंडों का आकार बड़ा, 10 15 मिमी या उससे अधिक होता है।
एलेसीटल अंडे व्यावहारिक रूप से जर्दी से रहित होते हैं, सूक्ष्म रूप से छोटे आकार (0.1 × 0.3 मिमी) होते हैं और मनुष्यों सहित अपरा स्तनधारियों की विशेषता होते हैं।
शुक्राणु या शुक्राणु बहुत छोटे मोबाइल नर युग्मक होते हैं (उदाहरण के लिए, मानव शुक्राणु 50 × 70 µm लंबे होते हैं, और मगरमच्छ 20 µm) जो नर गोनाड - वृषण द्वारा निर्मित होते हैं; इनकी संख्या लाखों में है. अलग-अलग जानवरों में शुक्राणु का आकार अलग-अलग होता है, लेकिन उनकी संरचना एक जैसी होती है, उनमें से अधिकांश का सिर और गर्दन होती है। शुक्राणु के सिर में एक केन्द्रक होता है जिसमें गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है और ढका होता हैएक्रोसोम एक्रोसोम एक विशेष संरचना है, एक संशोधित गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसमें निषेचन के दौरान अंडे की झिल्ली को भंग करने के लिए एंजाइम होते हैं, जो एक झिल्ली से घिरा होता है। गर्दन में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया और दो सेंट्रीओल्स होते हैं। सूक्ष्मनलिकाएं द्वारा गठित एक पूंछ गर्दन से बढ़ती है और शुक्राणु की गतिशीलता सुनिश्चित करती है। मध्य भाग का विस्तार इसमें मौजूद असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है, जो फ्लैगेलम के चारों ओर एक सर्पिल में इकट्ठे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया संकुचन तंत्र के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं जो फ्लैगेलम की गति प्रदान करते हैं। शुक्राणु के मुख्य और पूंछ भाग में फ्लैगेल्ला की संरचना होती है।

यदि आप ऊपर से मानव शुक्राणु के सिर को देखते हैं, तो यह गोल दिखाई देता है, और जब बगल से देखा जाता है, तो यह चपटा दिखाई देता है। अकेले फ्लैगेलर मूवमेंट शुक्राणु के लिए योनि से उस स्थान तक दूरी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है जहां निषेचन होता है। शुक्राणु का मुख्य लोकोमोटर कार्य अंडाणु के चारों ओर झुंड बनाना और अंडाणु की झिल्लियों में प्रवेश करने से पहले खुद को एक विशिष्ट तरीके से उन्मुख करना है।
युग्मकों का निर्माण (युग्मकजनन)।पुरुषों में जनन उपकला की कोशिकाएंऔर मादा गोनाड अनुक्रमिक माइटोटिक और अर्धसूत्रीविभाजन की एक श्रृंखला से गुजरती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से युग्मकजनन कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिपक्व नर युग्मक (शुक्राणुजनन) और मादा युग्मक (ओजेनेसिस) का निर्माण होता है। दोनों मामलों में, प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया गया है - प्रजनन चरण, विकास चरण और परिपक्वता चरण। प्रजनन चरण में बार-बार माइटोटिक विभाजन शामिल होता है जिससे कई शुक्राणुजन या ओगोनिया का निर्माण होता है। उनमें से प्रत्येक पहले अर्धसूत्रीविभाजन और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की तैयारी में वृद्धि की अवधि से गुजरता है। फिर परिपक्वता चरण शुरू होता है, जिसके दौरान पहला और दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन होता हैसाथ अगुणित कोशिकाओं का बाद में विभेदनऔर परिपक्व युग्मकों का निर्माण.
शुक्राणु विकास (शुक्राणुजनन)।शुक्राणु (शुक्राणु) क्रमिक कोशिका विभाजनों की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप बनते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता हैशुक्राणुजनन,इसके बाद एक जटिल विभेदीकरण प्रक्रिया कहा जाता हैशुक्राणुजनन (चित्र 20.31) ). शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 70 दिन लगते हैं; प्रति 1 ग्राम अंडकोष भार में 10 बनते हैं 7 प्रति दिन शुक्राणु. वीर्य नलिका के उपकला में कोशिकाओं की एक बाहरी परत होती हैरोगाणु उपकलाऔर इस परत के बार-बार कोशिका विभाजन के परिणामस्वरूप कोशिकाओं की लगभग छह परतें बनीं (चित्र 20.32 और 20.33); ये परतें शुक्राणु विकास के क्रमिक चरणों से मेल खाती हैं। सबसे पहले, जनन उपकला कोशिकाओं का विभाजन असंख्य को जन्म देता हैशुक्राणुजन जो आकार में बढ़ते-बढ़ते हो जाते हैंप्रथम क्रम के शुक्राणुकोशिकाएँ।पहले अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप, ये शुक्राणुनाशक अगुणित बनते हैंदूसरे क्रम के शुक्राणुनाशक,जिसके बाद वे दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन से गुजरते हैं और शुक्राणु में बदल जाते हैं। विकासशील कोशिकाओं के "स्ट्रैंड्स" के बीच बड़े होते हैंसर्टोली कोशिकाएँ, या पोषी कोशिकाएं,नलिका की बाहरी परत से लेकर उसके लुमेन तक संपूर्ण स्थान में स्थित है।

स्पर्मेटोसाइट्स सर्टोली कोशिकाओं की पार्श्व सतहों पर असंख्य आक्रमणों में स्थित होते हैं; यहां वे शुक्राणु में बदल जाते हैं, और फिर सर्टोली कोशिका के उस किनारे पर चले जाते हैं, जो वीर्य नलिका के लुमेन का सामना करता है, जहां वे परिपक्व होते हैं, बनाते हैंशुक्राणु (चित्र 20.33) ). जाहिरा तौर पर, सर्टोली कोशिकाएं परिपक्व शुक्राणु को यांत्रिक सहायता, सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हैं। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के आसपास की रक्त वाहिकाओं के माध्यम से विकासशील युग्मकों तक पहुंचाए गए सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन, और रक्त में छोड़ा गया चयापचय अपशिष्ट, सर्टोली कोशिकाओं से होकर गुजरता है। ये कोशिकाएं तरल पदार्थ भी स्रावित करती हैं जिसके साथ शुक्राणु नलिकाओं से होकर गुजरते हैं।
मनुष्यों में अंडे का विकास (ओजेनेसिस)।शुक्राणु के निर्माण के विपरीत, जो पुरुषों में केवल युवावस्था में ही शुरू होता है, महिलाओं में अंडों का निर्माण उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और प्रत्येक अंडे का निर्माण उसके निषेचन के बाद ही पूरा होता है। अंडजनन के चरणों को चित्र में दिखाया गया है। 20.36. भ्रूण के विकास के दौरान, प्राइमर्डियल जर्म कोशिकाएं माइटोसिस के माध्यम से बार-बार विभाजित होती हैं, जिससे कई बड़ी कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें कहा जाता हैओगोनिया. ओगोनिया फिर से माइटोसिस और फॉर्म से गुजरता हैपहला ऑर्डर oocygs,जो लगभग ओव्यूलेशन तक प्रोफ़ेज़ चरण में रहते हैं। प्रथम क्रम के oocytes कोशिकाओं की एक परत से घिरे होते हैं-ग्रैनुलोसा झिल्ली-और तथाकथित रूपमौलिक रोम.जन्म से ठीक पहले एक कन्या भ्रूण में लगभग 2 10 होते हैं 6 ये रोम, लेकिन उनमें से केवल लगभग 450 ही दूसरे क्रम के oocytes के चरण तक पहुंचते हैं और अंडाशय (ओव्यूलेशन) छोड़ देते हैं। ओव्यूलेशन से पहले, पहले क्रम का अंडाणु पहले अर्धसूत्रीविभाजन से गुजरता है, जिससे एक अगुणित बनता हैदूसरे क्रम का oocyteऔर पहला ध्रुवीय पिंड.दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन मेटाफ़ेज़ चरण तक पहुंचता है, लेकिन तब तक जारी नहीं रहता जब तक कि अंडाणु शुक्राणु के साथ विलीन न हो जाए। निषेचन के दौरान, दूसरे क्रम का अंडाणु दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन से गुजरता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनती है -अंडा और भी दूसरा ध्रुवीय पिंड.सभी ध्रुवीय पिंड छोटी कोशिकाएँ हैं; वे अंडजनन में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं।

अछूती वंशवृद्धि
लाचार
वैकल्पिक
अनिषेचित अंडे से ही जीवों का विकास होता है।
केवल मादाएं ही बनती हैं।
उदाहरण के लिए, कोकेशियान रॉक छिपकली
लेटलेट्स निषेचन के बिना और निषेचन के साथ दोनों विकसित हो सकते हैं
स्त्री प्रकार
नर का विकास अनिषेचित अंडों से होता है
पुरुष प्रकार
कुछ समविवाही शैवालों में
इसी तरह के अन्य कार्य जिनमें आपकी रुचि हो सकती है.vshm> |
|||
| 6644. | जीवों का व्यक्तिगत विकास (ओंटोजेनेसिस) | 78.69 केबी | |
| ऐसा माना जाता है कि केवल एक शुक्राणु की परमाणु सामग्री जानवरों के अंडे में प्रवेश करती है। मनुष्यों और कभी-कभी उच्चतर जानवरों के मामले में, जन्म से पहले के विकास की अवधि को अक्सर जन्म के बाद का जन्मपूर्व और प्रसवोत्तर कहा जाता है। अधिकांश बहुकोशिकीय जानवरों में, उनके संगठन की जटिलता की परवाह किए बिना, भ्रूण के विकास के चरण समान होते हैं। विभिन्न कशेरुकियों में कुचलने की प्रकृति और ब्लास्टुला के प्रकार... | |||
| 13714. | जीवों का व्यक्तिगत विकास और उनका व्यवहार। ओटोजेनेसिस। पौधों और जानवरों में जीवन चक्र | 9.96 केबी | |
| ओटोजेनेसिस व्यक्तित्व उत्पत्ति युग्मनज के गठन के क्षण से लेकर उसकी मृत्यु तक किसी जीव का व्यक्तिगत विकास है। युग्मक यौन कोशिकाएं हैं जो वंशानुगत जानकारी रखती हैं और उनमें अगुणित सेट होता है। निषेचन पौधों या जानवरों की नर और मादा प्रजनन कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया है और यह यौन प्रक्रिया का आधार है। भ्रूणीय रोगाणु काल युग्मनज के निर्माण से लेकर जन्म या अंडे की झिल्लियों से निकलने या अंकुरण तक ओटोजेनेसिस की अवधि है। | |||
| 10427. | प्रजनन | 6.75 केबी | |
| जीवों के प्रजनन के विभिन्न रूपों के साथ, उन सभी को दो मुख्य प्रकारों में घटाया जा सकता है: अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में, संतानों का प्रजनन एक माता-पिता से बीजाणुओं के निर्माण के माध्यम से या वानस्पतिक रूप से होता है। वानस्पतिक प्रसार के दौरान, संतान माँ से अलग हुए शरीर के अंगों से उत्पन्न होती है। वानस्पतिक प्रसार के दौरान, पौधे कई पीढ़ियों तक विषमयुग्मजीता बनाए रखते हैं। | |||
| 21332. | सीमित करने वाले कारक। कारकों के प्रति जीवों का अनुकूलन | 303.8 केबी | |
| कुछ जानवरों को तीव्र गर्मी पसंद होती है, अन्य मध्यम पर्यावरणीय तापमान को बेहतर ढंग से सहन करते हैं, आदि। इसके अलावा, जीवित जीवों को उन लोगों में विभाजित किया जाता है जो किसी भी पर्यावरणीय कारक में व्यापक या संकीर्ण सीमा में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। यदि पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव चरम मूल्यों तक नहीं पहुंचता है, तो जीवित जीव कुछ क्रियाओं या अपनी स्थिति में परिवर्तन के साथ इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, जो अंततः प्रजातियों के अस्तित्व की ओर ले जाता है। इस कार्य में अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरणीय कारक हैं; विषय सीमित कारक और जीवों का अनुकूलन है... | |||
| 8875. | जीवों और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत के सामान्य पैटर्न | 193.58 केबी | |
| मिट्टी के स्थलीय और जलीय पर्यावरण के जैविक कारक जीवित जीवों के जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ मानवजनित कारक जीवों और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत के सामान्य पैटर्न एक सीमित कारक की अवधारणा। लिबिग का न्यूनतम नियम शेल्फ़र्ड का नियम किसी जीव पर मानवजनित कारकों के प्रभाव की विशिष्टताएँ पर्यावरणीय कारकों के संबंध में जीवों का वर्गीकरण 1. फेदर ग्रास स्टेप्स की स्थितियाँ अजैविक कारकों के पूरी तरह से अलग शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। | |||
| 12700. | कीटों की जैविक विशेषताएँ एवं उनसे निपटने के उपाय | 62.79 केबी | |
| विशेष रूप से महत्वपूर्ण फसल हानि खरपतवारों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप होती है जो मिट्टी से पोषक तत्व और नमी को हटा देते हैं, खेती वाले पौधों को छाया देते हैं, और कई मामलों में विषाक्त पदार्थों और बीजों के साथ उत्पादों को दूषित करते हैं जो मनुष्यों और जानवरों के जहर का कारण बनते हैं। कृषि के रसायनीकरण की मुख्य दिशाएँ: उर्वरकों, रसायनों का उपयोग, कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से पौधों की सुरक्षा, पशुधन में रासायनिक उत्पादों का उपयोग, कृषि उत्पादों को डिब्बाबंद करना और... | |||
| 13403. | गैर-सेलुलर जीवन रूपों के रूप में वायरस। विभिन्न जीवों की कोशिकाओं के साथ वायरस की संरचना, वर्गीकरण, अंतःक्रिया | 12.75 केबी | |
| ये जैविक वस्तुएं हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए से बने जीनोम, जो जीवित कोशिकाओं में उनके जैवसंश्लेषक उपकरण का उपयोग करके उत्पादित होते हैं। वायरस और जीवन के अन्य रूपों के बीच अंतर: उनके पास एक सेलुलर संरचना नहीं है; 1 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड; केवल डीएनए या आरएनए; उनके पास अपना स्वयं का चयापचय नहीं है। वायरस की उत्पत्ति की परिकल्पना: वायरस एक सामान्य कोशिका के घटकों से उत्पन्न हुए जो नियामक तंत्र के नियंत्रण से बच गए और एक स्वतंत्र इकाई में बदल गए; संभवतः, डीएनए के एक खंड पर आनुवंशिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला हुई... | |||
| 18798. | पॉज़िम नदी घाटी के जंगल और खुले बायोटोप में मिट्टी के मेसोफ़ौना जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक संकेतक | 61.54 केबी | |
| हालाँकि, आज इस क्षेत्र का विकास कई पर्यावरणीय समस्याओं का परिणाम है। विशेष रूप से, घाटी में बाढ़ के मैदानों को खाली करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जो सीधे प्राकृतिक बायोटोप को प्रभावित करता है। | |||
| 19386. | सीआईएस में उदारवाद का विकास | 35.55 केबी | |
| विदेशी आर्थिक संबंधों के विकास की प्रक्रियाओं में विचाराधीन परिवर्तनों की जटिल प्रणाली प्रकृति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पहचान, सीमाओं और संप्रभुता के बारे में पारंपरिक विचारों के संपूर्ण सिद्धांतों के संशोधन और परिवर्तन को निर्धारित करती है... | |||
| 8867. | शिक्षा एवं विकास | 162.32 केबी | |
| प्रशिक्षण और विकास के बीच संबंध की समस्या का सार। प्रशिक्षण और विकास के बीच संबंधों की समस्या को हल करने के लिए बुनियादी दृष्टिकोण। समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा एल। प्रशिक्षण और विकास के बीच संबंध की समस्या का सार। | |||
प्रजनन जीवों का संतान उत्पन्न करने का गुण है या जीवों की स्वयं को पुन: उत्पन्न करने की क्षमता है। जीवित चीजों की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होने के नाते, प्रजनन जीवन की निरंतरता और प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
प्रजनन की प्रक्रिया बेहद जटिल है और यह न केवल माता-पिता से संतानों तक आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण से जुड़ी है, बल्कि जीवों के शारीरिक और शारीरिक गुणों, उनके व्यवहार और हार्मोनल नियंत्रण से भी जुड़ी है। जीवों का प्रजनन उनकी वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के साथ होता है।
जीवित प्राणियों की विशेषता उनके प्रजनन के तरीकों में अत्यधिक विविधता है। फिर भी, प्रजनन की दो मुख्य विधियाँ हैं - अलैंगिक और लैंगिक (चित्र 16)। अलैंगिक प्रजनन, या एपोमिक्सिस (ग्रीक से)। एआरओ -बिना, मिक्सिस -मिश्रण) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक (कोशिका या बहुकोशिकीय जीव) भाग लेता है। इसके विपरीत, यौन प्रजनन में दो माता-पिता शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्रजनन प्रणाली होती है और यौन कोशिकाएं (युग्मक) पैदा करती हैं, जो संलयन के बाद, एक युग्मनज (निषेचित अंडाणु) बनाती हैं, जो फिर एक भ्रूण में बदल जाती है। नतीजतन, यौन प्रजनन के दौरान वंशानुगत कारकों का मिश्रण होता है, यानी एक प्रक्रिया जिसे एम्फिमिक्सिस (ग्रीक से) कहा जाता है। उभयचर -दोनों तरफ, मिक्सिस -मिश्रण)।
असाहवासिक प्रजनन
अलैंगिक प्रजनन कई प्रजातियों के जीवों, पौधों और जानवरों दोनों की विशेषता है। यह वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, संवहनी पौधों, प्रोटोजोआ, स्पंज, कोइलेंटरेट्स, ब्रायोज़ोअन और ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है।
अलैंगिक प्रजनन का सबसे सरल रूप वायरस की विशेषता है। उनकी प्रजनन प्रक्रिया न्यूक्लिक एसिड अणुओं से जुड़ी होती है, इन अणुओं की स्वयं-दोहराने की क्षमता होती है
और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच अपेक्षाकृत कमजोर हाइड्रोजन बांड की विशिष्टता पर आधारित है।
चावल। 16.जीवों के प्रजनन के तरीके
अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अन्य जीवों के संबंध में, वानस्पतिक प्रजनन और स्पोरुलेशन द्वारा प्रजनन के बीच अंतर किया जाता है।
वनस्पति प्रसार वह प्रजनन है जिसमें मातृ जीव से अलग हुए भाग से एक नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार का प्रजनन एककोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों की विशेषता है, लेकिन उनमें अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ होती हैं।
एककोशिकीय जीवों में, वानस्पतिक प्रजनन को विभाजन, एकाधिक विखंडन और नवोदित जैसे रूपों द्वारा दर्शाया जाता है। एक मूल जीव से दो पुत्री जीवों के निर्माण के साथ साधारण संकुचन द्वारा विभाजन बैक्टीरिया और नीले-हरे शैवाल (सायनोबैक्टीरिया) की विशेषता है। इसके विपरीत, भूरे और हरे शैवाल के विभाजन के साथ-साथ एककोशिकीय जानवरों (सारकोड्स, फ्लैगेलेट्स और सिलिअट्स) का प्रजनन नाभिक के माइटोटिक विभाजन के माध्यम से होता है जिसके बाद साइटोप्लाज्म का संकुचन होता है।
एकाधिक विखंडन (स्किज़ोगोनी) द्वारा प्रजनन में नाभिक का विभाजन शामिल होता है जिसके बाद साइटोप्लाज्म को भागों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से अनेक पुत्री जीवों का निर्माण होता है। एकाधिक विभाजन का एक उदाहरण फाल्सीपेरम प्लास्मोडियम का प्रजनन है (पी. विवैक्स)मानव एरिथ्रोसाइट्स में. इस मामले में, प्लास्मोडिया में, बार-बार परमाणु विभाजन साइटोकाइनेसिस के बिना कई बार होता है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। परिणामस्वरूप, एक प्लाज्मोडियम 12-24 पुत्री जीवों को जन्म देता है।
बहुकोशिकीय पौधों के जीवों में, विभाजन द्वारा वानस्पतिक प्रसार कलमों, बल्बों, पत्तियों और प्रकंदों द्वारा किया जाता है। लेकिन यह अनिवार्य रूप से कृषि अभ्यास में उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम प्रसार है। कृत्रिम परिस्थितियों में उच्च पौधों का प्रजनन एक कोशिका से भी संभव है। जो जीव एक कोशिका (क्लोन) से विकसित होते हैं उनमें मूल बहुकोशिकीय जीव के सभी गुण होते हैं। इस प्रसार को क्लोनल माइक्रोप्रोपेगेशन कहा जाता है। वानस्पतिक प्रसार के रूपों में से एक कई खेती वाले पौधों का ग्राफ्टिंग या प्रत्यारोपण हो सकता है, जिसमें एक पौधे से दूसरे पौधे में एक कली या अंकुर का हिस्सा प्रत्यारोपित करना शामिल है। बेशक, यह भी प्रजनन की एक विधि है, जो प्रकृति में नहीं होती है, लेकिन कृषि में इसका बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
बहुकोशिकीय जानवरों में, कायिक प्रजनन उनके शरीर को भागों में विभाजित करके होता है, जिसके बाद प्रत्येक
एक भाग एक नये जानवर के रूप में विकसित होता है। इस तरह का प्रजनन स्पंज, कोएलेंटरेट्स (हाइड्रा), नेमेर्टियन, फ्लैटवर्म, इचिनोडर्म (स्टारफिश) और कुछ अन्य जीवों के लिए विशिष्ट है। जानवरों के वानस्पतिक प्रजनन के विखंडन का एक करीबी रूप पशु बहुभ्रूण है, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि विकास के एक निश्चित चरण में भ्रूण को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र जीव में विकसित होता है। बहुभ्रूणता आर्मडिलोस में होती है। हालाँकि, बाद वाला यौन रूप से प्रजनन करता है। इसलिए, बहुभ्रूणता यौन प्रजनन में एक अनोखा चरण है, और बहुभ्रूणता से उत्पन्न संतानों को मोनोज़ायगोटिक जुड़वाँ द्वारा दर्शाया जाता है।
बडिंग में मातृ कोशिका पर एक केंद्रक के साथ एक ट्यूबरकल (बहिर्वाह) का निर्माण होता है, जो फिर अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। मुकुलन एककोशिकीय पौधों में होता है, उदाहरण के लिए यीस्ट में, और एककोशिकीय जानवरों में, उदाहरण के लिए सिलिअट्स की कुछ प्रजातियों में।
स्पोरुलेशन द्वारा प्रजनन विशेष कोशिकाओं के निर्माण से जुड़ा होता है - बीजाणु, जिसमें एक नाभिक, साइटोप्लाज्म होता है, एक घने झिल्ली से ढके होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक अस्तित्व में रहने में सक्षम होते हैं, जो इसके अलावा, उनके फैलाव में योगदान देता है। अधिकतर, ऐसा प्रजनन बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, काई और फ़र्न में होता है। कुछ हरे शैवालों में, तथाकथित ज़ोस्पोर्स व्यक्तिगत कोशिकाओं से बन सकते हैं।
जानवरों में, स्पोरुलेशन द्वारा प्रजनन स्पोरोज़ोअन में देखा जाता है, विशेष रूप से फाल्सीपेरम प्लास्मोडियम में।
कई प्रजातियों के जीवों में, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन के साथ वैकल्पिक हो सकता है।
यौन प्रजनन
यौन प्रजनन एककोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों दोनों में होता है।
जैसा कि अध्याय V और XIII में बताया गया है, बैक्टीरिया में यौन प्रजनन संयुग्मन द्वारा किया जाता है, जो यौन प्रक्रिया के एक एनालॉग के रूप में कार्य करता है और इन जीवों के पुनर्संयोजन की एक प्रणाली है, जबकि प्रोटोजोआ में, यौन प्रजनन भी संयुग्मन या सिनगैमी के माध्यम से होता है। और ऑटोगैमी।
बहुकोशिकीय जीवों (पौधों और जानवरों) में, यौन प्रजनन रोगाणु या सेक्स कोशिकाओं (युग्मक), निषेचन और युग्मनज के निर्माण से जुड़ा होता है।
लैंगिक प्रजनन जीवों का एक महत्वपूर्ण विकासवादी अधिग्रहण है। दूसरी ओर, यह जीनों के पुनर्संयोजन, जीवों की विविधता के उद्भव और लगातार बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में योगदान देता है।
एककोशिकीय जीवों में लैंगिक प्रजनन कई रूपों में होता है। बैक्टीरिया में, यौन प्रजनन को उनमें होने वाले संयुग्मन के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें दाता कोशिकाओं (प्लास्मिड युक्त) से प्राप्तकर्ता कोशिकाओं (प्लास्मिड युक्त नहीं) में प्लास्मिड या क्रोमोसोमल डीएनए का स्थानांतरण होता है, साथ ही बैक्टीरिया का स्थानांतरण भी होता है। , जिसमें कुछ जीवाणु कोशिकाओं से आनुवंशिक सामग्री को अन्य चरणों में स्थानांतरित करना शामिल है। संयुग्मन सिलिअट्स में भी पाया जाता है, जिसमें इस प्रक्रिया के दौरान नाभिक का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, जिसके बाद उनका विभाजन होता है।
बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों में, कोशिकाओं का यौन प्रजनन मादा और नर जनन कोशिकाओं (अंडे और शुक्राणु) के निर्माण, उसके बाद शुक्राणु द्वारा अंडे के निषेचन और युग्मनज के निर्माण के माध्यम से होता है। पौधों में, सेक्स कोशिकाएं विशेष प्रजनन संरचनाओं में निर्मित होती हैं; जानवरों में, वे जननग्रंथियों में निर्मित होती हैं जिन्हें गोनाड (ग्रीक से) कहा जाता है। गया -बीज)।
जानवरों की दैहिक और प्रजनन कोशिकाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह इस तथ्य में निहित है कि दैहिक कोशिकाएं विभाजित होने में सक्षम हैं, अर्थात, वे स्वयं को पुन: उत्पन्न करती हैं, और, इसके अलावा, उनसे रोगाणु कोशिकाएं बनती हैं। इसके विपरीत, यौन कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि वे पूरे जीव का प्रजनन "शुरू" करती हैं।
द्विगुणित दैहिक कोशिकाएँ जिनमें नर जनन कोशिकाएँ बनती हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं, और जिनमें मादा जनन कोशिकाएँ बनती हैं - ओगोनिया कहलाती हैं। नर और मादा जनन कोशिकाओं के निर्माण (विकास और विभेदन) की प्रक्रिया को युग्मकजनन कहा जाता है।
युग्मकजनन अर्धसूत्रीविभाजन (ग्रीक से) पर आधारित है। अर्धसूत्रीविभाजन -कम करना), जो कोशिका नाभिक का एक कमी विभाजन है, जिसके साथ प्रति नाभिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है। अर्धसूत्रीविभाजन जीवित प्राणियों के प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है जो यौन रूप से प्रजनन करते हैं (चित्र 17)। उदाहरण के लिए, टेरिडोफाइट्स में, अर्धसूत्रीविभाजन इन पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर स्थित विशेष स्पोरैन्जियल कोशिकाओं में होता है और बीजाणुओं में और फिर गैमेटोफाइट्स में विकसित होता है। उत्तरार्द्ध अलग-अलग मौजूद होते हैं, अंततः नर और मादा युग्मक पैदा करते हैं। फूल वाले पौधों में, अर्धसूत्रीविभाजन बीजांड की विशेष कोशिकाओं में होता है, जो बीजाणुओं में विकसित होते हैं। उत्तरार्द्ध एक अंडे के साथ गैमेटोफाइट का उत्पादन करता है। इसके अलावा, इन पौधों में, अर्धसूत्रीविभाजन विशेष एथेर कोशिकाओं में भी होता है, जो बीजाणुओं में भी विकसित होते हैं जो अंततः दो नर युग्मकों के साथ पराग का उत्पादन करते हैं। केंचुओं में, जो उभयलिंगी होते हैं और शरीर के एक खंड में नर और दूसरे में मादा प्रजनन अंग होते हैं और जिनकी विशेषता होती है
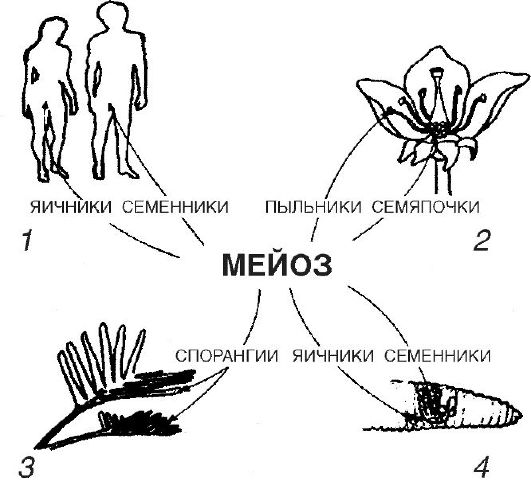
चावल। 17. विभिन्न जीवों में अर्धसूत्रीविभाजन: 1 - इंसान; 2 - फूल वाले पौधे; 3 - फर्न; 4 - केंचुआ
उनमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच परस्पर-निषेचन करने की क्षमता होती है; उनमें शुक्राणुजनन और अंडजनन एक साथ करने की क्षमता होती है।
अर्धसूत्रीविभाजन वृषण और अंडाशय की विशेष कोशिकाओं में होता है, जो क्रमशः नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। अर्धसूत्रीविभाजन के प्रेरक प्रोटीन की पहचान की गई है।
अर्धसूत्रीविभाजन की प्रक्रिया के दौरान, गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या (2एन), जो दैहिक कोशिकाओं (सेल नाभिक) और अपरिपक्व कोशिका रोगाणुओं की विशेषता है, अगुणित संख्या (एन) में बदल जाती है, जो परिपक्व रोगाणु कोशिकाओं की विशेषता है। इस प्रकार, युग्मकजनन के परिणामस्वरूप, रोगाणु कोशिकाओं को दैहिक कोशिकाओं के केवल आधे गुणसूत्र प्राप्त होते हैं (चित्र 18)।

चावल। 18.
जानवरों में युग्मकजनन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार नर और मादा दोनों में समान होता है। हालाँकि, अर्धसूत्रीविभाजन के विभिन्न चरणों की उत्पत्ति के समय में लिंग भिन्न-भिन्न होते हैं, जो विशेष रूप से है
मनुष्यों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य। पोस्टप्यूबर्टल पुरुषों में, अर्धसूत्रीविभाजन की पूरी प्रक्रिया लगभग दो महीने में पूरी हो जाती है, जबकि महिलाओं में, पहला अर्धसूत्रीविभाजन भ्रूण के अंडाशय में शुरू होता है और ओव्यूलेशन शुरू होने तक पूरा नहीं होता है, जो लगभग 15 वर्ष की आयु में होता है।
उच्चतर जानवरों में, पुरुषों के मामले में, अर्धसूत्रीविभाजन चार कार्यात्मक रूप से सक्रिय युग्मकों के गठन के साथ होता है।
इसके विपरीत, महिलाओं में, प्रत्येक दूसरे क्रम का अंडाणु केवल एक अंडा पैदा करता है। महिला अर्धसूत्रीविभाजन के अन्य परमाणु उत्पाद तीन कमी निकाय हैं जो प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं और पतित होते हैं।
अर्धसूत्रीविभाजन में दो परमाणु विभाजन होते हैं। पहला अर्धसूत्रीविभाजन समजातीय गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े के सदस्यों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने (सिनैप्सिस) और आनुवंशिक सामग्री (क्रॉसिंग ओवर) के आदान-प्रदान के बाद अलग करता है। इस विभाजन के परिणामस्वरूप दो अगुणित नाभिक बनते हैं। दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन इनमें से प्रत्येक नाभिक में गुणसूत्रों (क्रोमैटिड्स) के दो अनुदैर्ध्य हिस्सों को अलग करता है, जिससे चार अगुणित नाभिक बनते हैं।
युग्मकजनन की प्रक्रिया के दौरान, अंडों (ओवोजेनेसिस) और शुक्राणुजनन (शुक्राणुजनन) का विभेदन भी होता है, जो उनके कार्यों के लिए एक शर्त है। जानवरों के अंडे शुक्राणु की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, आमतौर पर गतिहीन होते हैं और इनमें पोषण सामग्री होती है जो निषेचन के बाद प्रारंभिक अवधि में भ्रूण के विकास को सुनिश्चित करती है। अधिकांश जानवरों के शुक्राणु में एक फ्लैगेलम होता है, जो उनकी गति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
अर्धसूत्रीविभाजन का उत्कृष्ट जैविक महत्व है। अर्धसूत्रीविभाजन के कारण, पीढ़ियों की संख्या की परवाह किए बिना, जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की एक निरंतर संख्या बनी रहती है। इसलिए, अर्धसूत्रीविभाजन प्रजातियों की स्थिरता को बनाए रखता है। अंत में, अर्धसूत्रीविभाजन में, क्रॉसिंग ओवर के परिणामस्वरूप, जीन पुनर्संयोजन होता है, जो विकास के कारकों में से एक है।
शुक्राणुजनन और ओवोजेनेसिस
शुक्राणुजनन परिपक्व पुरुष जनन कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्राणु विशेष दैहिक कोशिकाओं से नर गोनाड (वृषण, या वृषण) में विकसित होते हैं (चित्र 19)। ऐसी विशिष्ट कोशिकाएँ निम्नानुसार कार्य करती हैं:
प्राइमर्डियल जर्म कोशिकाएं कहलाती हैं, जो नर व्यक्ति के भ्रूणजनन की प्रारंभिक अवधि में वृषण में स्थानांतरित हो जाती हैं। नतीजतन, प्राइमर्डियल कोशिकाएं परिपक्व रोगाणु कोशिकाओं की पूर्वज (पूर्ववर्ती) होती हैं।
मानव वृषण कई नलिकाओं से बने होते हैं, जिनकी दीवारें कोशिकाओं की परतों से बनती हैं जो शुक्राणु विकास के विभिन्न चरणों में होती हैं। नलिकाओं की बाहरी परत शुक्राणुजन नामक बड़ी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का द्विगुणित समूह होता है और ये वृषण में प्राइमर्डियल जर्म कोशिकाओं के वंशज हैं। किसी व्यक्ति के यौवन की अवधि के दौरान, शुक्राणुजन का हिस्सा नलिकाओं की आंतरिक परत में चला जाता है, जहां, अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप, वे पहले क्रम के शुक्राणुकोशिका (स्पर्मेटोसाइट्स I) नामक कोशिकाओं में विकसित होते हैं, फिर दूसरे क्रम के शुक्राणुकोशिका में। (शुक्राणुकोशिका II) और, अंत में,

चावल। 19.शुक्राणुजनन और अंडजनन
शुक्राणुओं में, जो अगुणित रोगाणु कोशिकाएं हैं जो अंततः परिपक्व शुक्राणु में विभेदित होती हैं। इस प्रकार, सामान्य शब्दों में, हम कह सकते हैं कि शुक्राणुजनन द्विगुणित दैहिक कोशिकाओं (स्पर्मेटोगोनिया) में शुरू होता है, इसके बाद रोगाणु कोशिका परिपक्वता की अवधि होती है, जिसमें अर्धसूत्रीविभाजन के माध्यम से दो परमाणु विभाजन होते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये एक शख्स की तस्वीर है.
शुक्राणुजनन में अर्धसूत्रीविभाजन (चित्र 20) कई चरणों (चरणों) में होता है। विभाजनों के बीच दो अंतरावस्थाएँ होती हैं। इस प्रकार, अर्धसूत्रीविभाजन को एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है, अर्थात्: इंटरफ़ेज़ I - पहला अर्धसूत्रीविभाजन (प्रारंभिक प्रोफ़ेज़ I, देर से प्रोफ़ेज़ I, मेटाफ़ेज़ I, एनाफ़ेज़ I, टेलोफ़ेज़ I) - इंटरफ़ेज़ II (इंटरोकिनेसिस) - दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन (प्रोफ़ेज़ I, मेटाफ़ेज़ II, एनाफ़ेज़ II, टेलोफ़ेज़ II)। अर्धसूत्रीविभाजन की प्रक्रिया बहुत गतिशील है, इसलिए विभिन्न चरणों के बीच सूक्ष्म अंतर स्वयं चरणों की प्रकृति को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि विभिन्न चरणों में गुणसूत्रों के गुणों को दर्शाते हैं। इंटरफ़ेज़ I

चावल। 20.अर्धसूत्रीविभाजन चरण: 1 - प्रथम अर्धसूत्रीविभाजन; 2 - दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन
इसकी विशेषता यह है कि इसमें गुणसूत्र प्रतिकृति (डीएनए दोहरीकरण) होता है, जो प्रारंभिक प्रोफ़ेज़ I की शुरुआत तक लगभग पूरी तरह से पूरा हो जाता है।
पहला अर्धसूत्रीविभाजन प्राथमिक शुक्राणुकोशिका में शुरू होता है और एक लंबे प्रोफ़ेज़ की विशेषता होती है, जिसमें प्रोफ़ेज़ I और प्रोफ़ेज़ II एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। प्रोफ़ेज़ I में, पाँच मुख्य चरण होते हैं - लेप्टोनिमा, जाइगोनेमा, पचीनेमा, डिप्लोनेमा और डायकाइनेसिस।
लेप्टोनिमा चरण में, नाभिक में गुणसूत्र पतले सर्पिल धागों के रूप में प्रस्तुत होते हैं जिनमें कई गहरे रंग के कण (क्रोमोमेरेस) होते हैं। क्रोमोमेरेस और धागों का विभाजन नोट नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जाता है कि इस स्तर पर गुणसूत्र दोहरे यानी द्विगुणित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी के होमोलॉग क्लैस्प सिद्धांत के अनुसार उनकी लंबाई के साथ क्रोमोमेरेस द्वारा एकजुट होते हैं।
जाइगोनेमा चरण को समजात गुणसूत्रों के बीच सिनैप्स की स्थापना की विशेषता है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मित गुणसूत्र (द्विसंयोजक) का निर्माण होता है। क्रोमोसोम एक्स और वाई ऑटोसोम की तुलना में कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। वे संघनित होकर गहरे रंग के विषमवर्णीय पिंडों में बदल जाते हैं, जो उनके सिरों पर समजातीय क्षेत्रों के परिणामस्वरूप जुड़ जाते हैं।
पचीनेमा चरण में, जो अर्धसूत्रीविभाजन में सबसे लंबा चरण है, द्विसंयोजक का संघनन होता है और प्रत्येक क्रोमैटिड का विभाजन दो में होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक द्विसंयोजक एक जटिल पेचदार संरचना होती है जिसमें चार बहन क्रोमैटिड (टेट्राड) होते हैं। इस चरण के अंत में, युग्मित द्विसंयोजक गुणसूत्रों का पृथक्करण शुरू हो जाता है। अब समजात गुणसूत्रों को अगल-बगल देखा जा सकता है। इसलिए, कुछ तैयारियों में कोई चार गुणसूत्र देख सकता है, जो प्रत्येक होमोलॉग के दोहराव के परिणामस्वरूप बनते हैं, जिससे बहन क्रोमैटिड बनते हैं। इस स्तर पर, समजातियों के बीच आदान-प्रदान होता है और चियास्माटा का निर्माण होता है।
डिप्लोनेमा चरण में, बहन क्रोमैटिड्स का छोटा होना, मोटा होना और पारस्परिक प्रतिकर्षण होता है, जिसके परिणामस्वरूप द्विसंयोजक में क्रोमैटिड लगभग अलग हो जाते हैं। पृथक्करण को अधूरा माना जाता है क्योंकि गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में सेंट्रोमियर अभी तक विभाजित नहीं हुआ है। जहां तक द्विसंयोजकों का सवाल है, वे अपनी लंबाई के साथ विभिन्न स्थानों पर चियास्माटा द्वारा बंधे होते हैं, जो परिणामस्वरूप समजात क्रोमैटिड्स के बीच बनने वाली संरचनाएं हैं।
सिनैप्टिक रूप से जुड़े होमोलोग्स के बीच पिछला क्रॉसिंग। अच्छी तैयारियों में, द्विसंयोजक की लंबाई के आधार पर, एक से कई चियास्माटा देखे जा सकते हैं। इस चरण में देखा गया प्रत्येक चियास्मा पचीनेमा चरण के दौरान गैर-बहन क्रोमैटिड्स के बीच हुए आदान-प्रदान के परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-जैसे द्विसंयोजकों का संपीड़न और प्रतिकर्षण तीव्र होता है, चियास्माटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर बढ़ता है, यानी, गुणसूत्रों का टर्मिनलीकरण होता है। डिप्लोनेमा के अंत में, गुणसूत्रों का अवसादन होता है; समजात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं।
डायकिनेसिस के चरण में, जो डिप्लोनिमा के समान है, द्विसंयोजकों का छोटा होना जारी रहता है और चियास्माटा कमजोर (कमी) हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रोमैटिड्स (चार) के रूप में असतत इकाइयाँ बनती हैं। इस चरण के पूरा होने के तुरंत बाद, परमाणु झिल्ली का विघटन होता है।
मेटाफ़ेज़ I में, द्विसंयोजक अपनी उच्चतम सांद्रता तक पहुँचते हैं। अंडाकार बनकर, वे नाभिक के भूमध्यरेखीय भाग में स्थित होते हैं, जहाँ वे अर्धसूत्रीविभाजन I की भूमध्यरेखीय प्लेटों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक द्विसंयोजक का आकार चियास्माटा की संख्या और स्थान से निर्धारित होता है। पुरुषों में, मेटाफ़ेज़ I में प्रति द्विसंयोजक चियास्माटा की संख्या आमतौर पर 1-5 होती है। एकल टर्मिनली स्थित चियास्म के परिणामस्वरूप XY द्विसंयोजक छड़ के आकार का हो जाता है।
एनाफ़ेज़ I में, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर विपरीत सेंट्रोमियर की गति शुरू हो जाती है। परिणामस्वरूप, समजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में अब दो क्रोमैटिड होते हैं जो एक सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो विभाजित नहीं होते हैं और बरकरार रहते हैं। यह अर्धसूत्रीविभाजन के एनाफेज I को माइटोसिस के एनाफेज से अलग करता है, जिसमें सेंट्रोमियर विभाजन से गुजरता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रॉसिंग ओवर प्रत्येक क्रोमैटिड को आनुवंशिक रूप से भिन्न बनाता है।
टेलोफ़ेज़ I चरण में, गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुँचते हैं, जो पहले अर्धसूत्रीविभाजन को समाप्त करता है। टेलोफ़ेज़ I के बाद, एक छोटा इंटरफ़ेज़ (इंटरकाइनेसिस) होता है, जिसमें गुणसूत्र सर्पिल हो जाते हैं और फैल जाते हैं, या टेलोफ़ेज़ I सीधे दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन के प्रोफ़ेज़ II में चला जाता है। किसी भी मामले में डीएनए प्रतिकृति नहीं देखी गई है। पहले अर्धसूत्रीविभाजन के बाद, कोशिकाओं को दूसरे क्रम के शुक्राणुकोशिका कहा जाता है। ऐसी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घटती जाती है 2एन 1n तक, लेकिन डीएनए सामग्री अभी तक नहीं बदली है।
दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन कई चरणों (प्रोफ़ेज़ II, मेटाफ़ेज़ II, एनाफ़ेज़ II, टेलोफ़ेज़ II) में होता है और माइटोटिक विभाजन के समान होता है। प्रोफ़ेज़ II में, द्वितीयक शुक्राणुकोशिकाओं के गुणसूत्र ध्रुवों पर रहते हैं। मेटाफ़ेज़ II में, प्रत्येक दोहरे गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजित होता है, जिससे प्रत्येक नए गुणसूत्र को अपना स्वयं का सेंट्रोमियर मिलता है। एक धुरी का निर्माण शुरू होता है, जिसके ध्रुव की ओर नए गुणसूत्र गति करते हैं। टेलोफ़ेज़ II में, दूसरा अर्धसूत्रीविभाजन समाप्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दूसरे क्रम के शुक्राणुकोशिका में दो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जिनमें से शुक्राणु अलग हो जाते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की तरह, स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित (1n) होती है। हालाँकि, स्पर्मेटिड्स के गुणसूत्र एकल होते हैं, जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स II के क्रोमोसोम दोहरे होते हैं, जो दो क्रोमैटिड्स से निर्मित होते हैं। नतीजतन, प्रत्येक शुक्राणु के केंद्रक में गैर-समरूप गुणसूत्रों का एक सेट होता है। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री प्रकार (भूमध्यरेखीय विभाजन) का एक विभाजन है। यह डबल सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करता है और कमी विभाजन से अलग होता है, जिसमें समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। शास्त्रीय माइटोसिस से एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट होता है।
तो, पहले क्रम के शुक्राणुकोशिका के पहले अर्धसूत्रीविभाजन से दो माध्यमिक शुक्राणुकोशिका (दूसरे क्रम) का निर्माण होता है। कमी विभाजन के परिणामस्वरूप बनी संरचनाओं के दोनों क्रोमैटिड बहन क्रोमैटिड हैं। उत्तरार्द्ध पहले अर्धसूत्रीविभाजन से पहले की प्रतिकृति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणुकोशिका के दूसरे अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार, विशिष्ट अर्धसूत्रीविभाजन में, कोशिकाएं दो बार विभाजित होती हैं, जबकि गुणसूत्र केवल एक बार विभाजित होते हैं (चित्र 21)।
शुक्राणुजनन का अंतिम चरण विभेदन से जुड़ा होता है, जो प्रत्येक अपेक्षाकृत बड़े, गोलाकार रूप से स्थिर शुक्राणु के छोटे लम्बे गतिशील शुक्राणु में बदलने के साथ समाप्त होता है।
अधिकांश वयस्क (यौन रूप से परिपक्व) नर जानवरों में, शुक्राणुजनन लगातार या समय-समय पर (मौसमी तौर पर) वृषण में होता है। उदाहरण के लिए, कीड़ों में शुक्राणुजनन चक्र को पूरा करने में केवल कुछ दिन लगते हैं, जबकि स्तनधारियों में यह चक्र हफ्तों या यहां तक कि तक खिंच जाता है

चावल। 21.युग्मकजनन के दौरान गुणसूत्रों का वितरण
महीने. एक वयस्क में, शुक्राणुजनन पूरे वर्ष होता है। आदिम शुक्राणुजन का परिपक्व शुक्राणु में विकास का समय लगभग 74 दिन है।
विभिन्न प्रजातियों के जीवों द्वारा निर्मित नर प्रजनन कोशिकाएं, गतिशीलता और आकार और संरचना में अत्यधिक विविधता की विशेषता होती हैं (चित्र 22)। प्रत्येक मानव शुक्राणु में तीन खंड होते हैं - सिर, मध्य भाग और पूंछ (चित्र 23)। शुक्राणु के सिर में एक केन्द्रक होता है जिसमें गुणसूत्रों का एक अगुणित समूह होता है।
सिर एक एक्रोसोम से सुसज्जित होता है, जिसमें शुक्राणु सामग्री को अंडे में प्रवेश करने के लिए आवश्यक लिटिक एंजाइम होते हैं। दो सेंट्रीओल्स भी सिर में स्थानीयकृत होते हैं - proc-

चावल। 22. शुक्राणु का आकार

चावल। 23. शुक्राणु की संरचना: ए - विभिन्न विमानों में प्रकाश सूक्ष्म छवि: 1 - सिर, 2 - मध्य भाग, 3 - पूंछ; बी - एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म छवि का योजनाबद्ध पुनर्निर्माण: 1 - नाभिक, 2 - एक्रोसोम, 3 - सेंट्रोसोम (समीपस्थ सेंट्रीओल), 4 - केंद्रीय रिंग, 5 - माइटोकॉन्ड्रियल हेलिक्स,
6 - अक्षीय धागा
सिमल, जो शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे के विभाजन को उत्तेजित करता है, और डिस्टल, जो पूंछ के अक्षीय शाफ्ट को जन्म देता है। शुक्राणु के मध्य भाग में पूंछ और माइटोकॉन्ड्रिया का आधारीय भाग होता है। शुक्राणु की पूंछ (प्रक्रिया) एक आंतरिक अक्षीय छड़ और एक बाहरी आवरण से बनती है, जो साइटोप्लाज्मिक मूल की होती है। मानव शुक्राणु को महत्वपूर्ण गतिशीलता की विशेषता होती है।
ओवोजेनेसिस और ऑगल कोशिकाएं
अंडे बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। इसका कार्य अंडे के केंद्रक में गुणसूत्रों के अगुणित सेट और युग्मनज की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है। अपनी अभिव्यक्ति में अंडजनन मूलतः शुक्राणुजनन से तुलनीय है।
स्तनधारियों और मनुष्यों में, अंडजनन जन्मपूर्व अवधि (जन्म से पहले) में शुरू होता है। ओगोनिया, जो काफी बड़े केंद्रक वाली छोटी कोशिकाएं होती हैं और डिम्बग्रंथि के रोम में स्थानीयकृत होती हैं, प्राथमिक अंडाणु में अंतर करना शुरू कर देती हैं। उत्तरार्द्ध अंतर्गर्भाशयी विकास के तीसरे महीने में पहले से ही बनते हैं, जिसके बाद वे पहले अर्धसूत्रीविभाजन के प्रोफ़ेज़ में प्रवेश करते हैं। जब एक लड़की का जन्म होता है, तब तक सभी प्राथमिक अंडाणु पहले से ही पहले अर्धसूत्रीविभाजन के प्रोफ़ेज़ में होते हैं। प्राथमिक अंडाणु मादा व्यक्ति में यौवन की शुरुआत तक प्रोफ़ेज़ में रहते हैं। एक अंडाणु में 100,000 माइटोकॉन्ड्रिया तक होते हैं। जब यौवन की शुरुआत में डिम्बग्रंथि के रोम परिपक्व हो जाते हैं, तो प्राथमिक ओसाइट्स में अर्धसूत्रीविभाजन फिर से शुरू हो जाता है। प्रत्येक विकासशील अंडे का पहला अर्धसूत्रीविभाजन उस अंडे के ओव्यूलेशन के समय से कुछ समय पहले पूरा हो जाता है। पहले अर्धसूत्रीविभाजन और साइटोप्लाज्म के असमान वितरण के परिणामस्वरूप, एक परिणामी कोशिका एक द्वितीयक oocyte बन जाती है, दूसरी - एक ध्रुवीय (कमी) शरीर बन जाती है।
द्वितीयक अर्धसूत्रीविभाजन तब होता है जब द्वितीयक अंडाणु (विकासशील अंडाणु) अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। हालाँकि, यह विभाजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु में प्रवेश नहीं कर जाता, जो आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब शुक्राणु द्वितीयक अंडाणु में प्रवेश करता है, तो बाद वाला विभाजित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अंडाणु (परिपक्व अंडा) बनता है, जिसमें एक एकल सेट वाला प्रोन्यूक्लियस होता है।
23 मातृ गुणसूत्रों में से। इस विभाजन से उत्पन्न दूसरी कोशिका एक दूसरा ध्रुवीय पिंड है, जो आगे विकास करने में असमर्थ है। इस समय ध्रुवीय (कमी) पिंड का भी दो भागों में विभाजन हो जाता है। इस प्रकार, एक प्रथम-क्रम अंडाणु का विकास एक अंडाणु और तीन न्यूनीकरण निकायों के गठन के साथ होता है। अंडाशय में, 300-400 अंडाणु आमतौर पर जीवन भर इसी तरह परिपक्व होते हैं, लेकिन प्रति माह केवल एक अंडाणु परिपक्व होता है। अंडों के विभेदन के दौरान झिल्लियाँ बनती हैं और उनके केन्द्रक का आकार छोटा हो जाता है।
कुछ पशु प्रजातियों में, अंडजनन तेजी से और लगातार होता है और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अंडे का उत्पादन होता है।
शुक्राणुजनन के साथ समानता के बावजूद, अंडजनन की विशेषता कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। प्राथमिक अंडाणु की पोषण सामग्री (जर्दी) अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाली चार कोशिकाओं के बीच समान रूप से वितरित नहीं होती है। जर्दी की मुख्य मात्रा एक बड़ी कोशिका में संग्रहित होती है, जबकि ध्रुवीय पिंडों में यह पदार्थ बहुत कम होता है। विभाजनों के परिणामस्वरूप, पहले और दूसरे ध्रुवीय निकायों को द्वितीयक oocytes के समान गुणसूत्र सेट प्राप्त होते हैं, लेकिन वे रोगाणु कोशिकाएं नहीं बनते हैं। इसलिए, शुक्राणु की तुलना में अंडे पोषण सामग्री में अधिक समृद्ध होते हैं। यह अंतर विशेष रूप से अंडे देने वाले जानवरों के मामले में स्पष्ट होता है।
स्तनधारी अंडों का आकार अंडाकार या कुछ हद तक लम्बा होता है (चित्र 24) और ये कोशिकीय संरचना की विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होते हैं। उनमें दैहिक कोशिकाओं की विशेषता वाली सभी संरचनाएं शामिल हैं, हालांकि, अंडे का इंट्रासेल्युलर संगठन बहुत विशिष्ट है और इस तथ्य से निर्धारित होता है कि अंडा भी वह वातावरण है जो युग्मनज के विकास को सुनिश्चित करता है। अंडों की एक विशेषता उनकी झिल्लियों की संरचना की जटिलता है। कई जानवरों में, अंडों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक झिल्लियाँ प्रतिष्ठित होती हैं। प्राथमिक खोल (आंतरिक) अंडाणु चरण में बनता है। डिम्बाणुजनकोशिका की सतह परत का प्रतिनिधित्व करते हुए, इसकी एक जटिल संरचना होती है, क्योंकि यह इसके निकटवर्ती कूपिक कोशिकाओं के बहिर्गमन द्वारा प्रवेश करती है। द्वितीयक (मध्य) खोल पूरी तरह से कूपिक कोशिकाओं द्वारा बनता है, और तृतीयक (बाहरी) खोल उन पदार्थों द्वारा बनता है जो डिंबवाहिनी ग्रंथियों के स्रावी उत्पाद हैं जिनके माध्यम से अंडे गुजरते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षियों में,
अंडों की तृतीयक झिल्लियाँ एल्ब्यूमिन, उपकोश और शैल झिल्लियाँ हैं। स्तनधारी अंडों की विशेषता दो झिल्लियों की उपस्थिति होती है। अंडों के अंतःकोशिकीय घटकों की संरचना प्रजातियों के संदर्भ में विशिष्ट होती है, और कभी-कभी इसमें व्यक्तिगत विशेषताएं भी होती हैं।

चावल। 24. अंडे की संरचना: 1 - कूपिक कोशिकाएं; 2 - खोल; 3 - साइटोप्लाज्म; 4- मुख्य
निषेचन
निषेचन नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद एक नए जीव का विकास होता है। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, युग्मनज में गुणसूत्रों का एक द्विगुणित सेट स्थापित होता है, जो इस प्रक्रिया के उत्कृष्ट जैविक महत्व को निर्धारित करता है।
लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों की प्रजातियों के आधार पर, बाह्य और आंतरिक निषेचन को प्रतिष्ठित किया जाता है। बाहरी निषेचन उस वातावरण में होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन कोशिकाएं प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए, मछली में निषेचन बाह्य होता है। उनके द्वारा छोड़े गए नर (दूध) और मादा (कैवियार) प्रजनन कोशिकाएं पानी में प्रवेश करती हैं, जहां वे मिलते हैं और एकजुट होते हैं।
आंतरिक निषेचन पुरुष शरीर से महिला शरीर में शुक्राणु के स्थानांतरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा निषेचन स्तनधारियों में होता है, जिसका केंद्रीय बिंदु रोगाणु कोशिकाओं के नाभिक का संलयन होता है। ऐसा माना जाता है कि एक शुक्राणु की सामग्री अंडे में प्रवेश करती है। निषेचन के तंत्र में
पूरा होने के बाद भी बहुत कुछ अस्पष्ट है। समुद्री अर्चिन में निषेचन के आंकड़ों से पता चलता है कि शुक्राणु और अंडे के संपर्क के 2 सेकंड बाद ही, बाद के प्लाज्मा झिल्ली के विद्युत गुणों में परिवर्तन होते हैं। युग्मकों का संलयन 7 सेकंड के भीतर होता है। यह माना जाता है कि अंडे में कई शुक्राणुओं में से केवल एक की सामग्री का प्रवेश उसके प्लाज्मा झिल्ली के विद्युत गुणों में परिवर्तन से समझाया गया है। एक निषेचित अंडा युग्मनज को जन्म देता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु चयापचय के सक्रिय होने के कारणों पर दो राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शुक्राणु का कोशिकाओं की सतह पर बाहरी रिसेप्टर्स से जुड़ना एक संकेत है जो झिल्ली के माध्यम से अंडे में प्रवेश करता है और वहां इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम आयनों को सक्रिय करता है। दूसरों का मानना है कि शुक्राणु में एक विशेष आरंभक कारक होता है।
हाल के वर्षों में किए गए प्रायोगिक विकास से पता चला है कि मनुष्यों सहित स्तनधारियों के अंडों का निषेचन इन विट्रो में संभव है। इसके अलावा, इन विट्रो में विकसित भ्रूणों को एक महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जहां उनका आगे सामान्य विकास होता है। "टेस्ट ट्यूब" बच्चों के जन्म के कई मामले हैं।
जाइगोजेनेसिस द्वारा प्रजनन करने वाले जानवरों के विपरीत, कई जीव पार्थेनोजेनेसिस (ग्रीक से) द्वारा प्रजनन करने में सक्षम हैं। पार्थेनोस -कुंवारी और जीनोस -जन्म), जो एक अनिषेचित अंडे से जीवों के प्रजनन को संदर्भित करता है। बाध्यकारी और ऐच्छिक पार्थेनोजेनेसिस हैं। ओब्लिगेट पार्थेनोजेनेसिस कुछ प्रजातियों के जीवों के प्रजनन का मुख्य तरीका बन गया है, उदाहरण के लिए, कोकेशियान रॉक छिपकली। इस प्रजाति के जानवर केवल मादा होते हैं। इसके विपरीत, वैकल्पिक पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ है कि अंडे निषेचन के बिना और निषेचन के बाद दोनों विकसित करने में सक्षम हैं। वैकल्पिक पार्थेनोजेनेसिस, बदले में, महिला और पुरुष है। मादा पार्थेनोजेनेसिस अक्सर मधुमक्खियों, चींटियों और रोटिफ़र्स में देखा जाता है, जिसमें नर अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। नर अनिषेकजनन कुछ समविवाही शैवालों में होता है।
पार्थेनोजेनेसिस प्राकृतिक और कृत्रिम (प्रेरित) दोनों हो सकता है। कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस का तंत्र भौतिक या रासायनिक का उपयोग करके अंडों की जलन है
ऐसे कारक, जो अंडों की सक्रियता की ओर ले जाते हैं और परिणामस्वरूप, अनिषेचित अंडों का विकास होता है। कई व्यवस्थित समूहों के जानवरों में कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है - इचिनोडर्म, कीड़े, मोलस्क और यहां तक कि स्तनधारी भी।
पार्थेनोजेनेसिस के एक ज्ञात रूप को एंड्रोजेनेसिस (ग्रीक से) कहा जाता है। एंड्रोस -आदमी, उत्पत्ति -मूल)। यदि किसी अंडे में नाभिक निष्क्रिय हो और फिर कई शुक्राणु उसमें प्रवेश कर जाएं, तो ऐसे अंडे से पुरुष (शुक्राणु) नाभिक के संलयन के परिणामस्वरूप एक पुरुष जीव विकसित होता है।
ऐसे मामले हैं जहां पार्थेनोजेनेसिस मौसम के आधार पर चक्रीय रूप से होता है। उदाहरण के लिए, रोटिफ़र्स, डफ़निया और एफिड्स गर्मियों में पार्थेनोजेनेसिस द्वारा प्रजनन करते हैं, और पतझड़ में अंडों के निषेचन और युग्मनज के गठन, यानी जाइगोजेनेसिस द्वारा प्रजनन करते हैं।
प्रकृति में पार्थेनोजेनेसिस और इसके रूपों की भूमिका छोटी है, क्योंकि यह जीवों की व्यापक अनुकूली क्षमताएं प्रदान नहीं करता है।
जाइगोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस के विपरीत, गाइनोजेनेसिस होता है, जो स्यूडोगैमी है, जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है और इसे सक्रिय करता है, लेकिन शुक्राणु नाभिक अंडे के नाभिक के साथ विलय नहीं करता है। इस मामले में, परिणामी संतान में केवल महिलाएं होती हैं। गाइनोजेनेसिस प्राकृतिक रूप से नेमाटोड और मछली में होता है, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है। विशेष रूप से, रेशमकीट, मछली और उभयचरों में कृत्रिम गाइनोजेनेसिस के मामलों का वर्णन किया गया है।
वैकल्पिक अगुणता और द्विगुणितता।
पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन
जो जीव लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, उनके विकास में बारी-बारी से अगुणित और द्विगुणित चरण होते हैं। स्तनधारियों सहित कई जीवों में, यह विकल्प नियमित है, और जीवों की प्रजातियों की विशेषताओं का संरक्षण इस पर आधारित है।
कई जीवों में पीढ़ियों के परिवर्तन की भी विशेषता होती है, जब अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले व्यक्तियों की पीढ़ियों को युग्मकों के निर्माण के साथ यौन रूप से प्रजनन करने वाले व्यक्तियों की पीढ़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे पीढ़ियों का प्राथमिक परिवर्तन कहा जाता है। यह स्पोरोज़ोअन, फ़्लैजेलेट्स और कई पौधों में पाया जाता है। पीढ़ियों का प्राथमिक परिवर्तन नियमित है, और यह वर्तमान है
प्रकृति में जो पाया जाता है वह अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों के कई जीवों के फाइलोजेनी में संरक्षण का संकेत देता है। अन्य जीवों में, पार्थेनोजेनेसिस के साथ यौन प्रजनन का विकल्प होता है। इसे द्वितीयक पीढ़ीगत परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कंपकंपी में, यौन प्रजनन को नियमित रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पीढ़ियों के इस द्वितीयक प्रत्यावर्तन को हेटेरोगोनी कहा जाता है। सहसंयोजकों में, विकास के कुछ चरणों में, यौन प्रजनन से अलैंगिक (वानस्पतिक) में संक्रमण होता है। पीढ़ियों के द्वितीयक प्रत्यावर्तन के इस रूप को मेटाजेनेसिस कहा जाता है।
यौन द्विरूपता. उभयलिंगीपन
नर और मादा में विशिष्ट फेनोटाइपिक लक्षण होते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच उनके गुणों में अंतर को यौन द्विरूपता कहा जाता है। जानवरों में यह पहले से ही विकासवादी विकास के निचले चरणों में होता है, उदाहरण के लिए गोल हेल्मिंथ और आर्थ्रोपोड में, और कशेरुक में इसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तक पहुंचता है।
यदि नर और मादा प्रजनन कोशिकाएं एक ही व्यक्ति द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें नर और मादा दोनों गोनाड होते हैं, तो इस घटना को वास्तविक उभयलिंगीपन कहा जाता है। यह फ़्लैटवर्म, एनेलिड्स और मोलस्क में पाया जाता है। फ्लैटवर्म में, नर और मादा गोनाड व्यक्ति के पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। इसके विपरीत, मोलस्क में गोनाड बारी-बारी से अंडे और शुक्राणु का उत्पादन करते हैं।
सच्चा उभयलिंगीपन मनुष्यों में भी होता है, जो विकास संबंधी विकारों के परिणामस्वरूप होता है। उभयलिंगी जीवों के जीनोटाइप 46 XX या 46 XY हैं, जिनमें से अधिकांश मामले XX (लगभग 60%) हैं। जीनोटाइप XX अक्सर नीग्रोइड अफ्रीकी आबादी के उभयलिंगी लोगों में पाया जाता है, जबकि XY अक्सर जापानी लोगों में पाया जाता है। दोनों प्रकार के उभयलिंगियों में, द्विपक्षीय गोनाडल विषमता की ओर प्रवृत्ति देखी गई। सच्चे उभयलिंगियों में, क्रोमोसोमल मोज़ाइक भी होते हैं, जिनमें कुछ दैहिक कोशिकाओं में XX गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है, दूसरों में - XY की एक जोड़ी होती है।
गलत उभयलिंगीपन को भी जाना जाता है, जब व्यक्तियों में बाहरी जननांग और दोनों लिंगों की माध्यमिक यौन विशेषताएं होती हैं, लेकिन केवल एक प्रकार की रोगाणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं - पुरुष या महिला।
प्रजनन विधियों की उत्पत्ति
ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन अलैंगिक प्रजनन है, विशेष रूप से वानस्पतिक प्रजनन। उत्तरार्द्ध से, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन विकसित हुआ, जिसका निस्संदेह लाभ यह है कि यह प्रजातियों के संरक्षण और विशेष रूप से उनके फैलाव के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है।
लैंगिक प्रजनन जीवों के प्रजनन का सबसे प्रभावी तरीका है। ऐसा माना जाता है कि यह अलैंगिक से विकसित हुआ, लगभग 1 अरब साल पहले उभरा, और पहले चरण युग्मकों के विकास में जटिलता से जुड़े थे। आदिम युग्मकों को अपर्याप्त रूपात्मक विभेदन की विशेषता थी, जिसके परिणामस्वरूप आइसोगैमी (ग्रीक से। आइसोस-बराबर, गामोस -विवाह), जब सेक्स कोशिकाएं गतिशील आइसोगैमेट्स थीं, नर और मादा रूपों में विभेदित नहीं थीं।
इसके बाद, अनिसोगैमी विकसित हुई (ग्रीक से)। अनिसोस-असमान, गामोस -विवाह), विभेदित युग्मकों की उपस्थिति की विशेषता है जो केवल आकार में भिन्न होते हैं। विकास के बाद के चरणों में, युग्मकों की गतिशीलता, आकार और आकार में तीव्र अंतर उत्पन्न हुए। विकास की प्रक्रिया में, कशेरुकियों ने कई अतिरिक्त उपकरण भी विकसित किए जो पुरुष शुक्राणु को महिला प्रजनन पथ में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करते हैं और एक निषेचित अंडे के विकास के लिए स्थितियां बनाते हैं। विकास के दौरान, ये उपकरण उत्सर्जन तंत्र से विकसित हुए, जिससे जनन मूत्र तंत्र का निर्माण हुआ।
द्विगुणित अवस्था जीवों को अत्यधिक लाभ प्रदान करती है क्योंकि इस अवस्था में विभिन्न एलील्स का संचय होता है। इसलिए, लैंगिक प्रजनन का वह लाभ भी है जो यह जीवों को प्रदान करता हैहेअलैंगिक की तुलना में परिवर्तनशीलता की अधिक संभावना है, और यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पार्थेनोजेनेसिस के स्पष्ट प्रजनन लाभ हैं, क्योंकि यह केवल मादा संतान पैदा करता है। हालाँकि, यह दुर्लभ है। जीवों की प्राकृतिक आबादी में पार्थेनोजेनेसिस द्वारा यौन प्रजनन के प्रतिस्थापन की कम आवृत्ति को समझाने के लिए दो परिकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। उनमें से एक (उत्परिवर्तन-संचय) के अनुसार, सेक्स एक अनुकूली अनुकूलन है, क्योंकि यह समय के साथ दोहराए जाने वाले उत्परिवर्तन से जीनोम को "साफ" करता है, जबकि एक अन्य परिकल्पना (पारिस्थितिक) के अनुसार, सेक्स एक अनुकूली अनुकूलन है।
वृद्धि और विकास के बारे में पहला विचार प्राचीन विश्व का है। यहां तक कि हिप्पोक्रेट्स (460-377 ईसा पूर्व) ने भी माना कि अंडों में पहले से ही एक पूर्ण रूप से गठित जीव होता है, लेकिन बहुत कम रूप में। इस विचार को तब प्रीफॉर्मेशनिज्म (अक्षांश से) के सिद्धांत में विकसित किया गया था। प्रीफॉर्मेटियो -प्रीफ़ॉर्मेशन), जो 17वीं-18वीं शताब्दी में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। प्रीफॉर्मेशनवाद के समर्थक हार्वे, माल्पीघी और उस समय के कई अन्य प्रमुख जीवविज्ञानी और चिकित्सक थे। प्रीफॉर्मेशनवादियों के लिए, विवादास्पद मुद्दा केवल यह था कि जीव किस सेक्स कोशिकाओं में प्रीफॉर्म हुआ था - महिला या पुरुष। जो लोग अंडे को प्राथमिकता देते थे उन्हें ओविस्ट कहा जाता था, और जो पुरुष प्रजनन कोशिकाओं को अधिक महत्व देते थे उन्हें एनिमलकुलिस्ट कहा जाता था। प्रीफॉर्मेशनिज़्म शुरू से अंत तक एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, क्योंकि इसने विकास को नकार दिया है। प्रीफॉर्मेशनिज्म को निर्णायक झटका सी. बोनट (1720-1793) ने दिया, जिन्होंने 1745 में अनिषेचित अंडों से एफिड्स के विकास के उदाहरण का उपयोग करके पार्थेनोजेनेसिस की खोज की। इसके बाद, प्रीफॉर्मेशनिज़्म अब ठीक नहीं हो सका और अपना महत्व खोना शुरू कर दिया।
प्राचीन विश्व में, एक और सिद्धांत उत्पन्न हुआ जो प्रीफॉर्मेशनिज़्म के विपरीत था और बाद में इसे एपिजेनेसिस (ग्रीक से) नाम मिला। महामारीबाद में, उत्पत्ति -विकास)। प्रीफॉर्मेशनिज्म की तरह, एपिजेनेसिस भी 17वीं-18वीं शताब्दी में व्यापक हो गया। एपिजेनेसिस के प्रसार में के.एफ. के विचारों का बहुत महत्व था। वुल्फ (1733-1794) ने अपनी पुस्तक "द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट" (1759) में इसका सारांश दिया है। के.एफ. वुल्फ का मानना था कि अंडे में न तो कोई पूर्वनिर्मित जीव होता है और न ही उसके हिस्से होते हैं और इसमें प्रारंभिक रूप से सजातीय द्रव्यमान होता है। प्रीफॉर्मिस्टों के विपरीत, के.एफ. के विचार। वुल्फ और एपिजेनेसिस के अन्य समर्थक अपने समय के लिए प्रगतिशील थे, क्योंकि उनमें विकास का विचार निहित था। हालाँकि, बाद में नए क्षण सामने आए। विशेष रूप से, 1828 में, के. बेयर ने अपना काम "द हिस्ट्री ऑफ एनिमल डेवलपमेंट" प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि अंडे की सामग्री विषम है, यानी संरचित है, और भ्रूण के विकसित होने के साथ संरचना की डिग्री बढ़ जाती है। इस प्रकार, के. बेयर ने प्रीफ़ॉर्मेशनिज़्म और एपिजेनेसिस दोनों की असंगतता दिखाई।
वृद्धि और विकास जीवित चीजों के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। विकास कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूरे जीव के द्रव्यमान में वृद्धि है, जबकि विकास शरीर में गुणात्मक परिवर्तन है जो कोशिका विभेदन और मोर्फोजेनेसिस द्वारा निर्धारित होते हैं, जो अंडों से शुरू होकर व्यक्तियों में प्रगतिशील परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। और उनकी वयस्क अवस्था पर समाप्त होता है।
ओटोजेनेसिस (ग्रीक से। ओन्टोस -प्राणी, उत्पत्ति -विकास) किसी व्यक्ति के विकास का इतिहास (चक्र) है, जो उसे जन्म देने वाली रोगाणु कोशिकाओं के निर्माण से शुरू होता है और उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है। ओटोजनी के बारे में विचार वृद्धि, विकास और विभेदीकरण के आंकड़ों पर आधारित हैं। मानव जीव विज्ञान को समझने के लिए ओटोजेनेसिस के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन महत्वपूर्ण है।
जीवों के विकास पर आधुनिक आंकड़े प्रीफॉर्मेशनिज्म और एपिजेनेसिस दोनों को खारिज करते हैं। आधुनिक अवधारणाओं के ढांचे के भीतर, किसी जीव के विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जिसमें पहले बनी संरचनाएं बाद की संरचनाओं के विकास को उत्तेजित करती हैं। विकास प्रक्रिया आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है और इसका पर्यावरण से गहरा संबंध होता है। परिणामस्वरूप, विकास आंतरिक और बाह्य कारकों की एकता से निर्धारित होता है।
वृद्धि और विकास की एकता
किसी जीव की वृद्धि उसके द्रव्यमान में क्रमिक वृद्धि और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और उनके विभेदन, ऊतकों और अंगों के निर्माण और कोशिकाओं और ऊतकों में जैव रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आकार में परिवर्तन है। इस प्रकार, वृद्धि कोशिकाओं की संख्या (शरीर के वजन) में वृद्धि के रूप में मात्रात्मक परिवर्तन और कोशिका विभेदन और मोर्फोजेनेसिस के रूप में गुणात्मक परिवर्तन का परिणाम है। कोशिका विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ कोशिकाएँ रूपात्मक, जैव रासायनिक और कार्यात्मक रूप से अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। कुछ कोशिकाओं का प्रजनन और विभेदन हमेशा दूसरों की वृद्धि और विभेदन के साथ समन्वित होता है। ये दोनों प्रक्रियाएँ जीव के पूरे जीवन चक्र में होती रहती हैं। चूँकि विभेदित कोशिकाएँ अपना आकार बदलती हैं, और कोशिकाओं के समूह आकार में परिवर्तन में शामिल होते हैं, यह मोर्फोजेनेसिस के साथ होता है, जो प्रक्रियाओं का एक सेट है जो कोशिकाओं और ऊतकों के संरचनात्मक संगठन के साथ-साथ जीवों की सामान्य आकृति विज्ञान को निर्धारित करता है।
माप परिणामों के आधार पर शरीर के आकार, वजन, शुष्क द्रव्यमान, कोशिका संख्या, नाइट्रोजन सामग्री और अन्य संकेतकों के वक्र बनाकर विकास को मापा जा सकता है।
ओटोजेनेसिस और इसके प्रकार। ओटोजेनेसिस की अवधि
जीवों के विकास की प्रकृति के आधार पर ओटोजेनेसिस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में वर्गीकृत किया जाता है, और इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास के बीच अंतर किया जाता है। प्रकृति में जीवों का प्रत्यक्ष विकास गैर-लार्वा और अंतर्गर्भाशयी विकास के रूप में होता है, जबकि अप्रत्यक्ष विकास लार्वा विकास के रूप में देखा जाता है। ओटोजनी के विपरीत, प्रजाति श्रेणी फाइलोजेनी है।
बड़े पैमाने पर विकास. इस विकास को अप्रत्यक्ष विकास के रूप में समझा जाता है, क्योंकि जीवों के विकास में एक या अधिक लार्वा चरण होते हैं। लार्वा का विकास कीड़ों, उभयचरों और इचिनोडर्म्स के लिए विशिष्ट है। इन जानवरों के लार्वा एक स्वतंत्र जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं, फिर परिवर्तनों से गुजरते हैं। इसलिए, इस विकास को कायापलट वाला विकास भी कहा जाता है (नीचे देखें)।
गैर-लार्वा विकास. विकास का यह रूप उन जीवों की विशेषता है जो सीधे विकसित होते हैं, उदाहरण के लिए, मछली, सरीसृप और पक्षी, जिनके अंडे जर्दी (पोषक तत्व) से भरपूर होते हैं। इसके कारण, ओटोजनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाहरी वातावरण में रखे गए अंडों में होता है। भ्रूण का चयापचय अनंतिम अंगों के विकास से सुनिश्चित होता है, जो भ्रूण की झिल्ली (जर्दी थैली, एमनियन, एलेंटोइस) होते हैं।
अंतर्गर्भाशयी विकास. यह विकास उन जीवों की भी विशेषता है जो सीधे विकसित होते हैं, जैसे मनुष्य सहित स्तनधारी। चूँकि इन जीवों के अंडों में पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है, इसलिए भ्रूण के सभी महत्वपूर्ण कार्य मातृ शरीर द्वारा माँ और भ्रूण के ऊतकों से अनंतिम अंगों के निर्माण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य है नाल। विकासात्मक रूप से, अंतर्गर्भाशयी विकास नवीनतम रूप है, लेकिन यह भ्रूणों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।
ओटोजेनेसिस को प्रीएम्ब्रायोनिक, भ्रूणीय और पोस्टएम्ब्रायोनिक अवधियों में विभाजित किया गया है। मनुष्यों के मामले में, जन्म से पहले के विकास की अवधि को जन्मपूर्व या प्रसवपूर्व कहा जाता है, जन्म के बाद - प्रसवोत्तर। अंग के मूल तत्वों के निर्माण से पहले विकासशील भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है, अंग के निर्माण के बाद - एक भ्रूण।
प्राक्गर्भाशय विकास
जीवों के व्यक्तिगत विकास में यह अवधि युग्मकजनन की प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण से जुड़ी होती है। पुरुष प्रजनन कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं से महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है, जबकि अंडे इस मायने में भिन्न होते हैं कि उनमें बहुत अधिक मात्रा में जर्दी होती है। अंडों में जर्दी की मात्रा और उसके वितरण को ध्यान में रखते हुए, बाद वाले को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
1) आइसोलेसीथल अंडे, इसमें थोड़ी सी जर्दी होती है, जो पूरी कोशिका में समान रूप से स्थानीयकृत होती है। ये अंडे इचिनोडर्म्स (समुद्री अर्चिन), लोअर कॉर्डेट्स (लैंसलेट्स) और स्तनधारियों द्वारा निर्मित होते हैं;
2) टेलोलेसिथल अंडे इसमें बड़ी मात्रा में जर्दी होती है, जो ध्रुवों में से एक - वानस्पतिक - पर केंद्रित होती है। ऐसे अंडे मोलस्क, उभयचर, सरीसृप और पक्षियों द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, मेंढक के अंडे में 50% जर्दी होती है, मुर्गी के अंडे (आमतौर पर मुर्गी के अंडे) - 95% होते हैं। टेलोलेसिथल अंडों के दूसरे ध्रुव (जानवर) पर, साइटोप्लाज्म और नाभिक केंद्रित होते हैं;
3) सेंट्रोलेसीथल ओसाइट्स, जिसमें जर्दी बहुत कम होती है और वह केन्द्रीय स्थान रखती है। साइटोप्लाज्म ऐसे अंडों की परिधि पर स्थित होता है। सेंट्रोलेसीथल अंडे आर्थ्रोपोड द्वारा निर्मित होते हैं।
प्राक्भ्रूण काल की विशेषता इस तथ्य से भी है कि इस अवधि के दौरान युग्मकों में डीएनए अणुओं के संचय से जुड़ी चयापचय प्रक्रियाएं होती हैं।
भ्रूणीय विकास
भ्रूणजनन (ग्रीक से। एटब्रायोप -रोगाणु), या भ्रूण काल, नर और मादा जनन कोशिकाओं के संलयन से शुरू होता है, जो अंडों के निषेचन की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।
अंतर्गर्भाशयी विकास की विशेषता वाले जीवों में, भ्रूण की अवधि जन्म के साथ समाप्त होती है, और लार्वा और गैर-लार्वा प्रकार के विकास की विशेषता वाले जीवों में, भ्रूण की अवधि क्रमशः अंडे या भ्रूण झिल्ली से जीव की रिहाई के साथ समाप्त होती है। भ्रूण काल के भीतर, युग्मनज, दरार, ब्लास्टुला, रोगाणु परतों का निर्माण, हिस्टोजेनेसिस और ऑर्गोजेनेसिस के चरणों को प्रतिष्ठित किया जाता है।
युग्मनज.निषेचन में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसमें पुरुष प्रजनन कोशिका एक अंडे के विकास की शुरुआत करती है। नर युग्मक द्वारा सक्रिय अंडे में, प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि सहित कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। प्रोटोप्लाज्म की गति से अंडे की द्विपक्षीय समरूपता स्थापित होती है। नाभिक फ्यूज हो जाता है, और गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट बहाल हो जाता है। इससे एककोशिकीय जीव का निर्माण होता है।
बंटवारे अप।यह युग्मनज (निषेचित अंडाणु) के विकास की प्रारंभिक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें समसूत्रण के माध्यम से युग्मनज को विभाजित करना शामिल है। विभाजन की शुरुआत अंडे की सतह पर एक खांचे की उपस्थिति से होती है। पहली नाली से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है - दो ब्लास्टोमेरेस, दूसरा - चार ब्लास्टोमेरेस, तीसरा - आठ ब्लास्टोमेरेस (चित्र 25)। क्रमिक विखंडन के परिणामस्वरूप बनने वाले कोशिकाओं के समूह को मोरुला (लैटिन से) कहा जाता है। मोरम- शहतूत)।
इस चरण का जैविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि एक बड़ी कोशिका, जो कि एक अंडाणु है, से छोटी कोशिकाएँ बनती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म और नाभिक का अनुपात कम हो जाता है।
युग्मनज का विखंडन एक बहुकोशिकीय संरचना के निर्माण के साथ समाप्त होता है जिसे ब्लास्टुला (ग्रीक से) कहा जाता है। ब्लास्टोस -अंकुर)। यह संरचना ब्लास्टोडर्म नामक पुटिका के आकार की होती है, जिसमें कोशिकाओं की एक परत होती है। अब इन कोशिकाओं को भ्रूणीय कहा जाता है। ब्लास्टुला का आकार अंडे के समान होता है। विखंडन की अवधि के दौरान, नाभिकों की संख्या और डीएनए की कुल संख्या बढ़ जाती है। थोड़ी मात्रा में एमआरएनए और टीआरएनए भी संश्लेषित होते हैं, जबकि राइबोसोमल आरएनए अभी तक पता लगाने योग्य नहीं है।
सभी जानवर ब्लास्टुला चरण से गुजरते हैं, लेकिन प्रत्येक मामले की अपनी विशेषताएं होती हैं। स्तनधारियों में, विभाजन असमान होता है, इसलिए मोरूला में विभिन्न संख्या में कोशिकाएँ होती हैं। इसके अलावा, कोशिकाओं का एक भाग ट्रोफोब्लास्ट नामक संरचना बनाता है,

ब्लास्टोकोल लार्वामेढक का डिंभकीट
रूप
चावल। 25.विभिन्न जीवों में युग्मनज का विखंडन और ब्लास्टुला का निर्माण: 1 - मूल अंडा; 2 - दो ब्लास्टोमेर; 3 - चार ब्लास्टोमेरेस; 4 - आठ ब्लास्टोमेर; 5 - ब्लास्टुला; 6 - वयस्क रूप
जिनकी कोशिकाएं भ्रूण को पोषण देती हैं और, एंजाइमों के लिए धन्यवाद, गर्भाशय की दीवार में भ्रूण के प्रवेश को सुनिश्चित करती हैं। बाद में, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं भ्रूण से अलग हो जाती हैं और एक पुटिका बनाती हैं, जो गर्भाशय के ऊतकों से तरल पदार्थ से भर जाती है।
इस चरण का जैविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि अंडे जैसी बड़ी कोशिका से छोटी कोशिकाएँ बनती हैं जिनमें साइटोप्लाज्म और नाभिक का अनुपात कम हो जाता है और नाभिक में एक नया साइटोप्लाज्मिक वातावरण होता है।
जठराग्नि(ग्रीक से गैस्ट्रे -वाहिका गुहा)। यह ब्लास्टुला के निर्माण के बाद भ्रूण कोशिकाओं की गति की प्रक्रिया है, जो भ्रूण की दो या तीन (जानवर के प्रकार के आधार पर) परतों या तथाकथित रोगाणु परतों के गठन के साथ होती है (चित्र 26)। ).
आइसोलेसीथल अंडों का विकास (गैस्ट्रुलेशन) ब्लास्टुला के अंदर वनस्पति ध्रुव के अंतःक्षेपण (इनवेजिनेशन) से होता है, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत ध्रुव लगभग विलीन हो जाते हैं, और ब्लास्टोकोल (ब्लास्टुला गुहा) लगभग या पूरी तरह से गायब हो जाता है। बाहरी
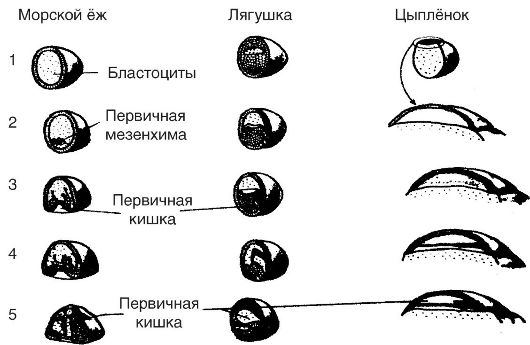
चावल। 26.विभिन्न जीवों में गैस्ट्रुलेशन: 1 - ब्लास्टोकोल; 2 - प्राथमिक मेसेनचाइम; 3, 4, 5 - प्राथमिक आंत
भ्रूण कोशिकाओं की परत को एक्टोडर्म (ग्रीक से) कहा जाता है। एक्टोस -बाहर, डर्मा -त्वचा), या बाहरी रोगाणु परत, जबकि आंतरिक एंडोडर्म (ग्रीक से) है। एंटोस -अंदर), या आंतरिक रोगाणु परत। इस मामले में बनी गुहा को गैस्ट्रोसील या प्राथमिक आंत कहा जाता है, जिसके प्रवेश द्वार को ब्लास्टोपोर (प्राथमिक मुंह) कहा जाता है।
दो रोगाणु परतों का विकास स्पंज और सहसंयोजक की विशेषता है। हालाँकि, गैस्ट्रुलेशन अवधि के दौरान कॉर्डेट्स को तीसरी रोगाणु परत - मेसोडर्म (ग्रीक से) के विकास की विशेषता होती है। मेसोस -मध्य), एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बनता है।
गैस्ट्रुलेशन विकास के बाद के चरणों के लिए एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि यह कोशिकाओं को ऐसी स्थिति में लाता है जिससे अंगों का निर्माण संभव हो जाता है। तीन भ्रूणीय उपांगों में विभेदित भ्रूणीय सामग्री विकासशील भ्रूण के सभी ऊतकों और अंगों को जन्म देती है।
रोगाणु परतों का विकास (विभेदन) उनके साथ विभिन्न ऊतकों और अंगों के निर्माण के साथ होता है। विशेष रूप से, त्वचा की बाह्य त्वचा, नाखून और बाल, वसामय और पसीने की ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, गैन्ग्लिया, तंत्रिकाएं), संवेदी अंगों की रिसेप्टर कोशिकाएं, आंख के लेंस, मुंह के उपकला , नाक गुहा और गुदा, दांत -
नया तामचीनी. एंडोडर्म से अन्नप्रणाली, पेट, आंत, पित्ताशय, श्वासनली, ब्रांकाई, फेफड़े, मूत्रमार्ग के उपकला, साथ ही यकृत, अग्न्याशय, थायरॉयड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथियां विकसित होती हैं। मेसोडर्म से चिकनी मांसपेशियां, कंकाल और हृदय की मांसपेशियां, डर्मिस, संयोजी ऊतक, हड्डियां और उपास्थि, दंत डेंटिन, रक्त और रक्त वाहिकाएं, मेसेंटरी, गुर्दे, वृषण और अंडाशय विकसित होते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सबसे पहले अलग होती है। 2 महीने के बाद, शरीर की लगभग सभी संरचनाएँ दिखाई देने लगती हैं। पर्यावरण के साथ भ्रूण का संबंध अनंतिम अंगों के माध्यम से होता है। भ्रूण काल के अंत में ऑर्गोजेनेसिस समाप्त हो जाता है। यदि प्राथमिक मुख (ब्लास्टोपोर) के स्थान पर निश्चित मौखिक उद्घाटन बनता है, तो इन जानवरों को प्रोटोस्टोम (कीड़े, मोलस्क, आर्थ्रोपोड) कहा जाता है।
यदि निश्चित मुख विपरीत स्थान पर बनता है तो इन जंतुओं को ड्यूटेरोस्टोम्स (इचिनोडर्म्स, कॉर्डेट्स) कहा जाता है।
पर्यावरण के साथ भ्रूण का संबंध सुनिश्चित करने के लिए, तथाकथित अनंतिम अंगों का उपयोग किया जाता है, जो अस्थायी रूप से मौजूद होते हैं। अंडों के प्रकार के आधार पर, अनंतिम अंग अलग-अलग संरचना वाले होते हैं। मछली, सरीसृप और पक्षियों में, अस्थायी अंगों में जर्दी थैली शामिल होती है। स्तनधारियों में, जर्दी थैली भ्रूणजनन की शुरुआत में बनती है, लेकिन विकसित नहीं होती है। बाद में इसे कम कर दिया जाता है. भ्रूण की बाहरी झिल्ली को कोरियोन कहा जाता है। यह गर्भाशय में बढ़ता है। गर्भाशय में सबसे अधिक वृद्धि के स्थान को प्लेसेंटा कहा जाता है। भ्रूण गर्भनाल, या गर्भनाल के माध्यम से नाल से जुड़ा होता है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो नाल को रक्त परिसंचरण प्रदान करती हैं। भ्रूण का चयापचय नाल के माध्यम से सुनिश्चित होता है।
भ्रूण के हिस्सों की रचनात्मक अंतःक्रिया कुछ समन्वित चयापचय प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। विकास का पैटर्न हेट्रोक्रोनी है, जिसे समय के साथ अंग संरचनाओं के अलग-अलग गठन और उनके विकास की अलग-अलग तीव्रता के रूप में समझा जाता है। जिन अंगों और प्रणालियों को पहले काम करना शुरू कर देना चाहिए उनका विकास तेजी से होता है। उदाहरण के लिए, मनुष्यों में, ऊपरी अंगों की शुरुआत निचले अंगों की तुलना में तेजी से विकसित होती है।
भ्रूण विभिन्न प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इसलिए, महत्वपूर्ण अवधियों को प्रतिष्ठित किया जाता है, अर्थात, वह अवधि जब भ्रूण हानिकारक कारकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। मनुष्यों के मामले में, भ्रूणीय ओटोजेनेसिस की महत्वपूर्ण अवधि
ये निषेचन के बाद के पहले दिन, नाल के गठन और बच्चे के जन्म का समय हैं।
दैहिक कोशिकाओं के नाभिक अंडों के सामान्य विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं, जो कि नाभिक की कमी वाले अंडों में दैहिक कोशिका नाभिक के प्रत्यारोपण पर प्रयोगों में स्पष्ट किया गया था।
प्रयोगों से यह भी पता चला कि एक नस्ल की भेड़ के 8- और 16-कोशिका वाले भ्रूण से एक एकल ब्लास्टोमेयर का दूसरी नस्ल के अंडे के एन्युक्लिएट आधे हिस्से में परिवर्तन (बाद वाले को आधे में काटने के बाद) व्यवहार्य भ्रूण के विकास के साथ हुआ था। और मेमनों का जन्म।
हिप्पोक्रेट्स (5वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के समय से, भ्रूण के जन्म की शुरुआत करने वाले कारणों के सवाल पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से, हिप्पोक्रेट्स ने स्वयं सुझाव दिया कि भ्रूण का विकास स्वयं उसके जन्म की शुरुआत करता है। अंग्रेजी शोधकर्ताओं द्वारा भेड़ों पर किए गए नवीनतम प्रायोगिक कार्य से पता चला है कि भेड़ों में मेमने की शुरुआत एक जटिल प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस + पिट्यूटरी ग्रंथि + भ्रूण की अधिवृक्क ग्रंथियां।हाइपोथैलेमिक नाभिक को नुकसान, पिट्यूटरी ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथियों के पूर्वकाल लोब को हटाने से भेड़ की गर्भावस्था बढ़ जाती है। इसके विपरीत, भेड़ों को एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन (पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि से एक स्राव) या कोर्टिसोल (अधिवृक्क ग्रंथियों से एक स्राव) देने से उनकी गर्भधारण की अवधि कम हो जाती है।
तो, उच्च यूकेरियोट्स के विकास की प्रक्रिया में, एक एकल निषेचित युग्मनज कोशिका, माइटोसिस के परिणामस्वरूप आगे के विकास के दौरान, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है - उपकला, तंत्रिका, हड्डी, रक्त कोशिकाएं और अन्य, जिनकी विशेषता होती है आकृति विज्ञान और मैक्रोमोलेक्यूलर संरचना की विविधता। हालाँकि, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की यह भी विशेषता है कि उनमें जीन के समान सेट होते हैं, लेकिन अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, केवल एक या कई विशिष्ट कार्य करते हैं, अर्थात, कुछ जीन कोशिकाओं में "कार्य" करते हैं, जबकि अन्य निष्क्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए,

चावल। 27. मोनोज़ायगोटिक जुड़वाँ का विकास
केवल लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के संश्लेषण और भंडारण में विशिष्ट होती हैं। उसी तरह, केवल एपिडर्मल कोशिकाएं ही केराटिन का संश्लेषण करती हैं। इसलिए, दैहिक कोशिकाओं के नाभिक की आनुवंशिक पहचान और कोशिका विभेदन के अंतर्निहित तंत्र को समझने के लिए एक शर्त के रूप में निषेचित अंडों के विकास के नियंत्रण तंत्र के बारे में सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं। कोशिका विभेदन में स्टेम कोशिकाओं का बहुत महत्व है (नीचे देखें)। चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि एक प्रकार की कोशिकाएँ दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होने में सक्षम हैं। विशेष रूप से, विभेदित या विभेदित यकृत कोशिकाओं को अग्न्याशय कोशिकाओं में परिवर्तित होते दिखाया गया है।
50 के दशक से। XX सदी कई प्रयोगशालाओं में, कृत्रिम रूप से अपने स्वयं के नाभिक से वंचित अंडों में दैहिक कोशिका नाभिक के सफल प्रत्यारोपण पर प्रयोग किए गए। विभिन्न विभेदित कोशिकाओं के नाभिक से डीएनए के एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग सभी मामलों में जीनोम में न्यूक्लियोटाइड जोड़े के अनुक्रमों के समान सेट होते हैं। ऐसे ज्ञात अपवाद हैं जहां स्तनधारी लाल रक्त कोशिकाएं विभेदन के अंतिम चरण के दौरान अपने नाभिक खो देती हैं। लेकिन इस समय तक पूल
कुछ हीमोग्लोबिन एमआरएनए पहले ही संश्लेषित किए जा चुके हैं, इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को अब नाभिक की आवश्यकता नहीं है। अन्य उदाहरणों में इम्युनोग्लोबुलिन और टी-सेल जीन शामिल हैं जो विकास के दौरान संशोधित होते हैं।
भ्रूणीय ओटोजेनेसिस के नियंत्रण तंत्र को समझने की दिशा में प्रमुख चरणों में से एक 1960-1970 के दशक में किए गए प्रयोगों के परिणाम थे। अंग्रेजी शोधकर्ता डी. गुर्डन ने यह पता लगाने के लिए कि क्या दैहिक कोशिकाओं के नाभिक में अंडों के आगे के विकास को सुनिश्चित करने की क्षमता है यदि इन नाभिकों को उन अंडों में पेश किया जाता है जिनमें से उनके स्वयं के नाभिक पहले हटा दिए गए हैं। चित्र में. चित्र 28 इन प्रयोगों में से एक का आरेख दिखाता है, जिसमें टैडपोल दैहिक कोशिकाओं के नाभिक को पहले हटाए गए नाभिक के साथ मेंढक के अंडों में प्रत्यारोपित किया गया था। इन प्रयोगों से पता चला कि दैहिक कोशिकाओं के नाभिक वास्तव में अंडों के आगे के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि वे अंडों को निषेचित करने और उन्हें आगे विकसित होने के लिए "मजबूर" करने में सक्षम थे। इससे जानवरों की क्लोनिंग की संभावना सिद्ध हो गई।

चावल। 28.दैहिक कोशिका नाभिक के नाभिकीय अंडों में प्रत्यारोपण पर एक प्रयोग की योजना (डी. गुर्डन, 1968)
बाद में, अन्य शोधकर्ताओं ने प्रयोग किए जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक नस्ल की भेड़ के 8 और 16-दिवसीय भ्रूणों से अलग-अलग ब्लास्टोमेरेस को दूसरी नस्ल के अंडे के नाभिकीय आधे भाग (बाद वाले को आधे में काटने के बाद) में स्थानांतरित किया गया था। मेमनों के बाद के जन्म के साथ व्यवहार्य भ्रूण का निर्माण।
1997 की शुरुआत में, अंग्रेजी लेखकों ने स्थापित किया कि कृत्रिम रूप से विकेंद्रीकृत भेड़ के अंडों में दैहिक कोशिका नाभिक (भ्रूण, भ्रूण या वयस्क भेड़ के थन की कोशिकाएं) का परिचय, और फिर इस प्रकार निषेचित अंडे को भेड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। मेमनों के जन्म के बाद गर्भावस्था की घटना (चित्र 29)। मेमनों में से एक का नाम डॉली था। 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। इस दौरान चूहों, गायों, खरगोशों, घोड़ों, चूहों और अन्य जानवरों के भ्रूण प्राप्त किए गए।

माँ के शरीर में संस्कृति का परिचय
चावल। 29.दैहिक कोशिका नाभिकों का एकल अंडों में प्रत्यारोपण
इन परिणामों के मूल्यांकन से पता चलता है कि स्तनधारियों को अलैंगिक रूप से पुन: उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे ऐसे जानवरों की संतान पैदा होती है जिनकी कोशिकाओं में दाता भेड़ के लिंग के आधार पर पैतृक या मातृ मूल की परमाणु सामग्री होती है। ऐसी कोशिकाओं में
केवल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया मातृ मूल के हैं। इस निष्कर्ष का सामान्य जैविक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह जानवरों की प्रजनन क्षमता पर हमारे विचारों का विस्तार करता है। लेकिन यह भी जोड़ना ज़रूरी है कि हम आनुवंशिक हेरफेर के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं। दूसरी ओर, व्यावहारिक रूप से, ये आनुवंशिक जोड़-तोड़ वांछित गुणों वाले उच्च संगठित जानवरों की क्लोनिंग का एक सीधा तरीका दर्शाते हैं, जिसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है। चिकित्सीय भाषा में कहें तो इस मार्ग का उपयोग भविष्य में पुरुष बांझपन को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
इसलिए, भ्रूण के सामान्य विकास के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी तथाकथित स्टेम कोशिकाओं के कारण कोशिका विभेदन के दौरान नष्ट नहीं होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की शरीर कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। जब स्टेम कोशिकाएँ विभाजित होती हैं, तो प्रत्येक नई कोशिका में या तो स्टेम कोशिका बने रहने या अधिक विशिष्ट कार्य वाली कोशिका (मांसपेशियाँ कोशिकाएँ, रक्त कोशिकाएँ, या मस्तिष्क कोशिकाएँ) बनने की क्षमता होती है। एक निषेचित अंडा पूर्णशक्तिशाली होता है क्योंकि यह शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देता है। टोटिपोटेंट स्टेम कोशिकाएँ भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक कोशिकाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोशिका को जन्म दे सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकती हैं, सामान्यतः कहलाती हैं मल्टीटोटिपोटेंटकोशिकाएं. यह स्थापित किया गया है कि वयस्क स्टेम कोशिकाएँ भ्रूण के असंबद्ध ऊतकों से विभेदित कोशिकाएँ उत्पन्न कर सकती हैं। दैहिक कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी नामक एक गुण भी होता है, अर्थात उनके जीनोम में वह सारी जानकारी होती है जो उन्हें निषेचित अंडे से प्राप्त हुई थी जिससे भेदभाव के परिणामस्वरूप उनका विकास हुआ। इन आंकड़ों की उपस्थिति का निस्संदेह मतलब है कि कोशिका विभेदन आनुवंशिक नियंत्रण के अधीन है। स्टेम कोशिकाओं के अध्ययन का चिकित्सा पर प्रभाव पड़ता है।
यह स्थापित किया गया है कि अधिकांश यूकेरियोट्स में निषेचन के बाद तीव्र प्रोटीन संश्लेषण एमआरएनए संश्लेषण के साथ नहीं होता है। कशेरुकियों में, विशेष रूप से उभयचरों में अंडजनन के अध्ययन से पता चला है कि गहन प्रतिलेखन अर्धसूत्रीविभाजन के प्रोफ़ेज़ I (विशेष रूप से डिप्लोमा) के दौरान भी होता है। इसलिए, एमआरएनए या प्रो-एमआरएनए अणुओं के रूप में जीन प्रतिलेख अंडों में सुप्त अवस्था में संग्रहीत होते हैं। यह स्थापित किया गया है कि भ्रूण कोशिकाओं में एक तथाकथित असममितता होती है
टर्नरी डिवीजन, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि एक भ्रूण कोशिका का विभाजन दो कोशिकाओं को जन्म देता है, जिनमें से केवल एक को प्रतिलेखन में शामिल प्रोटीन विरासत में मिलता है। इस प्रकार, पुत्री कोशिकाओं के बीच प्रतिलेखन कारकों का असमान वितरण विभाजन के बाद उनमें जीन के विभिन्न सेटों की अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, यानी कोशिका विभेदन।
उभयचरों और शायद अधिकांश कशेरुकियों में, आनुवंशिक कार्यक्रम जो प्रारंभिक विकास (ब्लास्टुला चरण से पहले) को नियंत्रित करते हैं, अंडजनन के दौरान स्थापित होते हैं। विकास के बाद के चरणों में, जब सेलुलर भेदभाव शुरू होता है (लगभग गैस्ट्रुला चरण से), जीन अभिव्यक्ति के लिए नए कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, कोशिका विभेदन किसी न किसी दिशा में आनुवंशिक जानकारी के पुन:प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है।
कोशिका विभेदन की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह अपरिवर्तनीय रूप से एक या दूसरे कोशिका प्रकार की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दृढ़ निश्चयऔर आनुवंशिक नियंत्रण में भी है, और जैसा कि अब माना जाता है, कोशिका विभेदन और निर्धारण को टायरोसिन कीनेज रिसेप्टर्स के माध्यम से पेप्टाइड वृद्धि कारकों द्वारा किए गए संकेतों के आधार पर कोशिकाओं की बातचीत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संभवतः ऐसी कई प्रणालियाँ हैं। उनमें से एक यह है कि मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं का विभेदन न्यूरोरेगुलिन्स द्वारा नियंत्रित होता है, जो झिल्ली प्रोटीन होते हैं जो एक या अधिक टायरोसिन कीनेस रिसेप्टर्स के माध्यम से कार्य करते हैं।
निर्धारण का आनुवंशिक नियंत्रण तथाकथित होमियोट्रोपिक या होमियोटिक उत्परिवर्तन के अस्तित्व से भी प्रदर्शित होता है, जो कि कीड़ों में विशिष्ट काल्पनिक डिस्क में निर्धारण में परिवर्तन का कारण बनता है। परिणामस्वरूप, शरीर के कुछ अंग अपनी जगह से हटकर विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोसोफिला में, उत्परिवर्तन एंटेना डिस्क के निर्धारण को एक डिस्क में बदल देता है जो सिर से विस्तारित अंग के परिशिष्ट में विकसित होता है। जाति के कीड़ों में ओफ्थाल्मोप्टेरानेत्र डिस्क से पंख संरचनाएं विकसित हो सकती हैं। चूहों में, एक जीन क्लस्टर (कॉम्प्लेक्स) हॉक्स का अस्तित्व दिखाया गया है, जिसमें 38 जीन होते हैं और अंगों के विकास को नियंत्रित करते हैं।
भ्रूण के विकास के दौरान जीन गतिविधि के नियमन का मुद्दा स्वतंत्र महत्व का है। ऐसा माना जाता है कि विभेदन के दौरान जीन अलग-अलग समय पर कार्य करते हैं, जो व्यक्त होता है
विभिन्न एमआरएनए की अलग-अलग विभेदित कोशिकाओं में प्रतिलेखन में, यानी जीन का दमन और डीरेप्रेशन होता है। उदाहरण के लिए, समुद्री अर्चिन ब्लास्टोसाइट्स में आरएनए में स्थानांतरित जीन की संख्या 10% है, चूहे के जिगर की कोशिकाओं में भी यह 10% है, और मवेशी थाइमस कोशिकाओं में यह 15% है। यह माना जाता है कि गैर-हिस्टोन प्रोटीन जीन की ट्रांसक्रिप्शनल स्थिति के नियंत्रण में शामिल होते हैं। निम्नलिखित डेटा इस धारणा का समर्थन करते हैं। जब कोशिका क्रोमैटिन चरण में होती है एससिस्टम में प्रतिलेखित कृत्रिम परिवेशीय,तब केवल हिस्टोन एमआरएनए संश्लेषित होता है, उसके बाद हिस्टोन होता है। इसके विपरीत, जब β-चरण से कोशिकाओं के क्रोमैटिन का उपयोग किया जाता है, तो कोई हिस्टोन एमआरएनए संश्लेषित नहीं होता है। जब गैर-पिस्टोन प्रोटीन को β-चरण के क्रोमैटिन से हटा दिया जाता है और गैर-हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है चरण एस,फिर ऐसे क्रोमैटिन के प्रतिलेखन के बाद कृत्रिम परिवेशीयहिस्टोन एमआरएनए संश्लेषित होता है। इसके अलावा, जब गैर-हिस्टोन प्रोटीन 1-चरण कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं, और डीएनए और हिस्टोन एस-चरण कोशिकाओं से आते हैं, तो कोई हिस्टोन एमआरएनए संश्लेषित नहीं होता है। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि क्रोमेटिन में निहित गैर-हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन एन्कोडिंग जीन को स्थानांतरित करने की क्षमता निर्धारित करते हैं .इसलिए विश्वास है कि गैर-हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यूकेरियोट्स में जीन के विनियमन और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि प्रोटीन और स्टेरॉयड हार्मोन जानवरों में प्रतिलेखन के नियमन में शामिल होते हैं। प्रोटीन (इंसुलिन) और स्टेरॉयड (एस्ट्रोगोन और टेस्टोस्टेरोन) हार्मोन दो सिग्नलिंग सिस्टम हैं जिनका उपयोग अंतरकोशिकीय संचार में किया जाता है। उच्चतर जानवरों में, हार्मोन विशेष स्रावी कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। रक्तप्रवाह में छोड़े जाने पर, वे ऊतकों में प्रवेश करते हैं। चूंकि प्रोटीन हार्मोन के अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, वे कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव लक्ष्य कोशिकाओं की झिल्लियों और चक्रीय एएमपी (सीएमपी) के इंट्रासेल्युलर स्तरों में स्थानीयकृत रिसेप्टर प्रोटीन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत, स्टेरॉयड हार्मोन छोटे अणु होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। एक बार कोशिकाओं के अंदर, वे विशिष्ट रिसेप्टर प्रोटीन से बंध जाते हैं जो केवल लक्ष्य कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स पर विचार किया जाता है हार्मोन - प्रोटीन रिसेप्टर,लक्ष्य कोशिकाओं के नाभिक में ध्यान केंद्रित करते हुए, वे निश्चित के साथ बातचीत के माध्यम से विशिष्ट जीन के प्रतिलेखन को सक्रिय करते हैं
मील गैर-हिस्टोन प्रोटीन जो विशिष्ट जीन के प्रवर्तक क्षेत्रों से जुड़ते हैं। नतीजतन, परिसर का बंधन हार्मोन + प्रोटीन (प्रोटीन रिसेप्टर)गैर-हिस्टोन प्रोटीन आरएनए पोलीमरेज़ की गति के लिए प्रमोटर क्षेत्रों को मुक्त करता है। जीवों के ओण्टोजेनेसिस में भ्रूण काल के आनुवंशिक नियंत्रण पर डेटा को सारांशित करते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विभिन्न कोशिकाओं (ऊतकों) में जीन की क्रिया को उनके अवसादन और दमन के माध्यम से चालू और बंद करने के अंतर से नियंत्रित होता है।
पोस्टमब्रायोनल विकास
किसी जीव के जन्म के बाद उसका भ्रूणोत्तर विकास शुरू होता है (मनुष्यों में प्रसवोत्तर), जो विभिन्न जीवों में उनकी प्रजाति के आधार पर कई दिनों से लेकर सैकड़ों वर्षों तक चलता है। नतीजतन, जीवन प्रत्याशा जीवों की एक प्रजाति की विशेषता है जो उनके संगठन के स्तर पर निर्भर नहीं करती है (नीचे देखें)।
पोस्टएम्ब्रायोनिक ओटोजेनेसिस में, किशोर और यौवन अवधि के साथ-साथ बुढ़ापे की अवधि, जो मृत्यु के साथ समाप्त होती है, के बीच अंतर किया जाता है।
किशोर काल. यह अवधि (अक्षांश से) किशोर- युवा) जीव के जन्म से लेकर यौवन तक के समय से निर्धारित होता है। यह अलग-अलग तरीकों से होता है और जीवों के ओटोजेनेसिस के प्रकार पर निर्भर करता है। यह अवधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास की विशेषता है।
उन जीवों के मामले में जिनका प्रत्यक्ष विकास होता है (कई अकशेरुकी, मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य), जो अंडे के छिलके या नवजात शिशुओं से उत्पन्न होते हैं, वे वयस्क रूपों के समान होते हैं, केवल छोटे आकार में ही बाद वाले से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत अंगों के अविकसित होने और शरीर के अपूर्ण अनुपात के रूप में (चित्र 30)।
प्रत्यक्ष विकास के अधीन जीवों की किशोर अवधि में वृद्धि की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि होती है, और शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है। उसके ओटोजेनेसिस की विभिन्न अवधियों के दौरान मानव विकास को चित्र में दिखाया गया है। 31. विभिन्न मानव अंगों की वृद्धि असमान होती है। उदाहरण के लिए, सिर का विकास बचपन में समाप्त हो जाता है, पैर लगभग 10 वर्षों तक आनुपातिक आकार तक पहुँच जाते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच बाह्य जननांग बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। निश्चित और अनिश्चित विकास के बीच अंतर किया जाता है। एक निश्चित वृद्धि उन जीवों की विशेषता है जो एक निश्चित उम्र में बढ़ना बंद कर देते हैं,
उदाहरण के लिए कीड़े, स्तनधारी, मनुष्य। अनिश्चित वृद्धि उन जीवों की विशेषता है जो जीवन भर बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए, मोलस्क, मछली, उभयचर, सरीसृप और कई पौधों की प्रजातियाँ।

चावल। तीस।विभिन्न प्रजातियों के जीवों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास
अप्रत्यक्ष विकास के मामले में, जीव ऐसे परिवर्तनों से गुजरते हैं जिन्हें कायापलट कहा जाता है (अक्षांश से)। कायापलट -परिवर्तन)।

चावल। 31.मानव ओण्टोजेनेसिस की विभिन्न अवधियों में वृद्धि और विकास
वे विकास के दौरान जीवों के संशोधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कायापलट व्यापक रूप से कोएलेंटरेट्स (हाइड्रा, जेलीफ़िश, कोरल पॉलीप्स), फ्लैटवर्म (फ़ासिओला), राउंडवॉर्म (राउंडवॉर्म), मोलस्क (सीप, मसल्स, ऑक्टोपस), आर्थ्रोपोड (क्रेफ़िश, नदी केकड़े, झींगा मछली, झींगा, बिच्छू, मकड़ियों, कण) में पाए जाते हैं। , कीड़े) और यहां तक कि कुछ कॉर्डेट्स (ट्यूनिकेट्स और उभयचर) में भी। इस मामले में, पूर्ण और अपूर्ण कायापलट को प्रतिष्ठित किया जाता है। कायापलट के सबसे अभिव्यंजक रूप कीड़ों में देखे जाते हैं जो अपूर्ण और पूर्ण दोनों तरह के कायापलट से गुजरते हैं।
अपूर्ण परिवर्तन एक ऐसा विकास है जिसमें अंडे के छिलके से एक जीव निकलता है, जिसकी संरचना एक वयस्क जीव की संरचना के समान होती है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। ऐसे जीव को लार्वा कहा जाता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान, लार्वा का आकार बढ़ जाता है, लेकिन मौजूदा चिटिनाइज्ड आवरण शरीर के आकार में और वृद्धि को रोकता है, जिससे गलन होती है, यानी, चिटिनाइज्ड आवरण का बहाव होता है, जिसके नीचे एक नरम छल्ली होती है। उत्तरार्द्ध सीधा हो जाता है, और इसके साथ जानवर के आकार में वृद्धि होती है। कई बार निर्मोचन के बाद, जानवर परिपक्वता तक पहुँच जाता है। अधूरा परिवर्तन विशिष्ट है, उदाहरण के लिए, खटमल के विकास के मामले में।
पूर्ण कायापलट एक ऐसा विकास है जिसमें अंडे के छिलके से एक लार्वा निकलता है, जो काफी भिन्न होता है
वयस्क व्यक्तियों से संरचना में. उदाहरण के लिए, तितलियों और कई कीड़ों में लार्वा कैटरपिलर होते हैं। कैटरपिलर पिघलने के अधीन हैं, और कई बार पिघल सकते हैं, फिर प्यूपा में बदल सकते हैं। उत्तरार्द्ध से, वयस्क रूप (इमागो) विकसित होते हैं, जो मूल से भिन्न नहीं होते हैं।
कशेरुकियों में, उभयचरों और हड्डी वाली मछलियों में कायापलट होता है। लार्वा चरण की विशेषता अनंतिम अंगों की उपस्थिति से होती है, जो या तो पूर्वजों की विशेषताओं को दोहराते हैं या स्पष्ट रूप से अनुकूली महत्व रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक टैडपोल, जो मेंढक का लार्वा रूप है और मूल रूप की विशेषताओं को दोहराता है, मछली जैसी आकृति, गिल श्वास की उपस्थिति और रक्त परिसंचरण के एक चक्र की विशेषता है। टैडपोल की अनुकूली विशेषताएं उनके चूसने वाले और लंबी आंतें हैं। लार्वा रूपों की यह भी विशेषता है कि, वयस्क रूपों की तुलना में, वे पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, एक अलग पारिस्थितिक स्थान और खाद्य श्रृंखला में एक अलग स्थान पर कब्जा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, मेंढक के लार्वा में गिल श्वसन होता है, जबकि वयस्क रूपों में फुफ्फुसीय श्वसन होता है। वयस्क रूपों के विपरीत, जो मांसाहारी होते हैं, मेंढक के लार्वा पौधों के खाद्य पदार्थों पर फ़ीड करते हैं।
जीवों के विकास में होने वाली घटनाओं के क्रम को अक्सर जीवन चक्र कहा जाता है, जो सरल या जटिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, सबसे सरल विकास चक्र स्तनधारियों की विशेषता है, जब एक जीव एक निषेचित अंडे से विकसित होता है, जो फिर से अंडे पैदा करता है, आदि। जटिल जैविक चक्र जानवरों में चक्र होते हैं, जो कायापलट के साथ विकास की विशेषता रखते हैं। जैविक चक्रों के बारे में ज्ञान व्यावहारिक महत्व का है, खासकर उन मामलों में जहां जीव जानवरों और पौधों में रोगज़नक़ या रोगज़नक़ों के वाहक होते हैं।
कायापलट से जुड़ा विकास और भेदभाव प्राकृतिक चयन का परिणाम है, जिसके कारण कई लार्वा रूप, जैसे कि कीट कैटरपिलर और मेंढक टैडपोल, वयस्क यौन रूप से परिपक्व रूपों की तुलना में पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं।
तरुणाई। इस अवधि को परिपक्व भी कहा जाता है और यह जीवों की यौन परिपक्वता से जुड़ा होता है। इस अवधि के दौरान जीवों का विकास अपने चरम पर पहुँच जाता है।
भ्रूण के बाद की अवधि में वृद्धि और विकास पर्यावरणीय कारकों से काफी प्रभावित होते हैं। पौधों के लिए, निर्णायक कारक प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता हैं। जानवरों के लिए, उचित आहार सर्वोपरि है (चारा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज लवण, विटामिन, सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति)। ऑक्सीजन, तापमान, प्रकाश (विटामिन डी संश्लेषण) भी महत्वपूर्ण हैं।
पशु जीवों की वृद्धि और व्यक्तिगत विकास हास्य और तंत्रिका नियामक तंत्र द्वारा न्यूरोह्यूमोरल विनियमन के अधीन है। पौधों में फाइटोहोर्मोन नामक हार्मोन जैसे सक्रिय पदार्थ पाए गए हैं। उत्तरार्द्ध पौधों के जीवों के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करते हैं।
पशु कोशिकाओं में, उनकी जीवन प्रक्रियाओं के दौरान, रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ संश्लेषित होते हैं जो जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोसेक्रेट्स नामक पदार्थ का उत्पादन करती हैं। अंतःस्रावी, या आंतरिक, स्राव ग्रंथियां भी हार्मोन नामक पदार्थों का स्राव करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, विशेष रूप से वृद्धि और विकास से संबंधित, तंत्रिका स्राव द्वारा नियंत्रित होती हैं। आर्थ्रोपोड्स में, वृद्धि और विकास का विनियमन मोल्टिंग पर हार्मोन के प्रभाव से बहुत अच्छी तरह से चित्रित होता है। कोशिकाओं द्वारा लार्वा स्राव का संश्लेषण मस्तिष्क में जमा होने वाले हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। क्रस्टेशियंस में एक विशेष ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो पिघलने को रोकती है। इन हार्मोनों का स्तर मोल्टिंग की आवृत्ति निर्धारित करता है। कीड़ों में, अंडे की परिपक्वता और डायपॉज का हार्मोनल विनियमन स्थापित किया गया है।
कशेरुकियों में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायरॉयड, पैराथायराइड, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथियां और गोनाड हैं, जो एक दूसरे से निकटता से जुड़े हुए हैं। कशेरुकियों में पिट्यूटरी ग्रंथि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का उत्पादन करती है, जो गोनाड की गतिविधि को उत्तेजित करती है। मनुष्यों में, पिट्यूटरी हार्मोन विकास को प्रभावित करता है। कमी से बौनापन विकसित होता है; अधिकता से विशालता विकसित होती है। पीनियल ग्रंथि एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो जानवरों की यौन गतिविधियों में मौसमी उतार-चढ़ाव को प्रभावित करती है। थायराइड हार्मोन कीड़ों और उभयचरों के कायापलट को प्रभावित करता है। स्तनधारियों में, थायरॉयड ग्रंथि के अविकसित होने से विकास मंदता और जननांग अंगों का अविकसित होना होता है। मनुष्यों में, थायरॉइड ग्रंथि में दोष के कारण हड्डी बनने और विकास में देरी होती है।
(बौनापन), यौवन नहीं आता, मानसिक विकास रुक जाता है (क्रेटिनिज़्म)। अधिवृक्क ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो चयापचय, विकास और कोशिकाओं के विभेदन को प्रभावित करती हैं। गोनाड सेक्स हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो माध्यमिक यौन विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। गोनाडों को हटाने से कई विशेषताओं में अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, बधिया किए गए मुर्गों में कंघी की वृद्धि रुक जाती है और यौन प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। बधिया किया गया पुरुष एक महिला के साथ बाहरी समानता प्राप्त करता है (त्वचा पर दाढ़ी और बाल नहीं उगते हैं, छाती और श्रोणि क्षेत्र पर वसा जमा होती है, आवाज का समय संरक्षित रहता है, आदि)।
पादप फाइटोहोर्मोन ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरेलिन हैं। वे कोशिका वृद्धि और विभाजन, नई जड़ों के निर्माण, फूलों के विकास और अन्य पौधों के गुणों को नियंत्रित करते हैं।
ओण्टोजेनेसिस की सभी अवधियों में, जीव खोए हुए या क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को बहाल करने में सक्षम होते हैं। जीवों के इस गुण को कहा जाता है पुनर्जनन,जो शारीरिक और पुनरावर्ती हो सकता है।
शारीरिक पुनर्जनन - यह शरीर के जीवन के दौरान खोए हुए शरीर के अंगों का प्रतिस्थापन है। इस प्रकार का पुनर्जनन पशु जगत में बहुत आम है। उदाहरण के लिए, आर्थ्रोपोड्स में इसे मोल्टिंग द्वारा दर्शाया जाता है, जो विकास से जुड़ा होता है। सरीसृपों में, पुनर्जनन पूंछ और तराजू के प्रतिस्थापन में व्यक्त किया जाता है, पक्षियों में - पंख, पंजे और स्पर्स में। स्तनधारियों में, शारीरिक पुनर्जनन का एक उदाहरण हिरणों द्वारा सींगों का वार्षिक रूप से झड़ना है।
पुनरावर्ती पुनर्जनन - यह किसी जीव के शरीर के उस हिस्से की बहाली है जिसे हिंसक रूप से तोड़ दिया गया था। इस प्रकार का पुनर्जनन कई जानवरों में संभव है, लेकिन इसकी अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, यह हाइड्रा में आम है और बाद वाले के प्रजनन से जुड़ा है, क्योंकि पूरा जीव एक भाग से पुनर्जीवित होता है। अन्य जीवों में, पुनर्जनन किसी भी अंग के नुकसान के बाद व्यक्तिगत अंगों की पुनर्प्राप्ति की क्षमता के रूप में प्रकट होता है। मनुष्यों में, उपकला, संयोजी, मांसपेशी और हड्डी के ऊतकों में काफी उच्च पुनर्योजी क्षमता होती है।
कई प्रजातियों के पौधे पुनर्जनन में भी सक्षम हैं।
पुनर्जनन पर डेटा न केवल जीव विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। इनका व्यापक रूप से कृषि, चिकित्सा, विशेषकर शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है।
वृद्धावस्था ओन्टोजेनेसिस के एक चरण के रूप में। वृद्धावस्था पशु ओन्टोजेनेसिस का अंतिम चरण है, और इसकी अवधि निर्धारित होती है
कुल जीवनकाल, जो एक प्रजाति की विशेषता के रूप में कार्य करता है और विभिन्न जानवरों के बीच भिन्न होता है। मनुष्यों में वृद्धावस्था का सबसे सटीक अध्ययन किया गया है।
मानव वृद्धावस्था की अनेक प्रकार की परिभाषाएँ हैं। विशेष रूप से, सबसे लोकप्रिय परिभाषाओं में से एक यह है कि बुढ़ापा क्रमिक परिवर्तनों का संचय है जो किसी जीव की उम्र में वृद्धि के साथ होता है और उसकी बीमारी या मृत्यु की संभावना को बढ़ाता है। मानव उम्र बढ़ने के विज्ञान को जेरोन्टोलॉजी (ग्रीक से) कहा जाता है। गेरोन -बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, लोगो -विज्ञान)। इसका कार्य परिपक्वता और मृत्यु के बीच आयु परिवर्तन के पैटर्न का अध्ययन करना है।
जेरोन्टोलॉजी में वैज्ञानिक अनुसंधान सेलुलर एंजाइमों की गतिविधि में परिवर्तन के अध्ययन से लेकर वृद्ध लोगों के व्यवहार पर पर्यावरणीय तनाव में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय शमन के प्रभाव को स्पष्ट करने तक, विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
मनुष्यों के मामले में, शारीरिक वृद्धावस्था को प्रतिष्ठित किया जाता है; कैलेंडर आयु से जुड़ी वृद्धावस्था; और सामाजिक कारकों और बीमारियों के कारण समय से पहले बुढ़ापा आना। डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों के अनुसार, एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगभग 60-75 वर्ष का माना जाना चाहिए, और वृद्ध को - 75 वर्ष या उससे अधिक का माना जाना चाहिए।
मानव वृद्धावस्था की पहचान कई बाहरी और आंतरिक लक्षणों से होती है।
बुढ़ापे के बाहरी लक्षणों में, सबसे अधिक ध्यान देने योग्य हैं आंदोलनों की सहजता में कमी, मुद्रा में बदलाव, त्वचा की लोच में कमी, शरीर का वजन, मांसपेशियों की दृढ़ता और लोच, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर झुर्रियों की उपस्थिति। शरीर, और दाँत का नुकसान। इसलिए, उदाहरण के लिए, सामान्यीकृत आंकड़ों के अनुसार, 30 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति 2 दांत खो देता है (नुकसान के परिणामस्वरूप), 40 वर्ष की आयु में - 4 दांत, 50 वर्ष की आयु में - 8 दांत, और 60 वर्ष की आयु में - पहले से ही 11 दांत. पहली सिग्नलिंग प्रणाली में ध्यान देने योग्य परिवर्तन होते हैं (संवेदी अंगों की तीक्ष्णता कम हो जाती है)। उदाहरण के लिए, अधिकतम दूरी जिस पर स्वस्थ लोग कुछ समान ध्वनियों को अलग कर सकते हैं, 20-30 वर्ष की आयु में 12 मीटर, 50 वर्ष की आयु में 10 मीटर, 60 वर्ष की आयु में 7 मीटर और 70 वर्ष की आयु में केवल 4 मीटर होती है। परिवर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं एक दूसरी सिग्नलिंग प्रणाली (भाषण का स्वर बदल जाता है, आवाज सुस्त हो जाती है)।
आंतरिक संकेतों में सबसे पहले हमें अंगों के विपरीत विकास (इनवॉल्यूशन) जैसे संकेतों का उल्लेख करना चाहिए। लीवर और किडनी के आकार के साथ-साथ संख्या में भी कमी आती है
गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या (80 वर्ष की आयु तक, लगभग आधी), जो गुर्दे की कार्यक्षमता को कम कर देती है और जल-इलेक्ट्रोलाइट चयापचय को प्रभावित करती है। रक्त वाहिकाओं की लोच कम हो जाती है, ऊतकों और अंगों का रक्त छिड़काव कम हो जाता है, और परिधीय संवहनी प्रतिरोध बढ़ जाता है। हड्डियों में अकार्बनिक लवण जमा हो जाते हैं, उपास्थि बदल जाती है (कैल्सीफाई हो जाती है), और अंगों की पुनर्जीवित होने की क्षमता कम हो जाती है। कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, विभाजन और उनके कार्यात्मक स्वर की बहाली धीमी हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, सेलुलर एंजाइमों की गतिविधि कम हो जाती है, आत्मसात और प्रसार के बीच समन्वय बाधित हो जाता है। मस्तिष्क में, प्रोटीन संश्लेषण बाधित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली की चिपचिपाहट बढ़ जाती है, सेक्स हार्मोन का संश्लेषण और उपयोग बाधित हो जाता है, और न्यूरॉन्स की संरचना में परिवर्तन होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रोटीन और इस ऊतक की लोच में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं कमजोर हो जाती हैं और ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं की संभावना बढ़ जाती है। अंतःस्रावी तंत्र, विशेष रूप से गोनाड, के कार्य कम हो जाते हैं। वृद्धावस्था में अन्य लक्षणों का व्यवहार चित्र में दिखाया गया है। 32.

चावल। 32.उम्र के साथ कुछ मानवीय विशेषताओं में परिवर्तन: 1 - तंत्रिका आवेगों की गति; 2 - बेसल चयापचय का स्तर; 3 - कार्डियक इंडेक्स; 4 - इंसुलिन के लिए वृक्क निस्पंदन का स्तर; 5 - फेफड़ों की ज्वारीय मात्रा; 6 - गुर्दे में प्लाज्मा प्रवाह का स्तर
शरीर की उम्र बढ़ने की प्रकृति को समझने की इच्छा लंबे समय से रही है। प्राचीन ग्रीस में, हिप्पोक्रेट्स का मानना था कि उम्र बढ़ने का संबंध भोजन की अधिकता और ताजी हवा के अपर्याप्त संपर्क से है। अरस्तू के अनुसार, उम्र बढ़ना शरीर द्वारा तापीय ऊर्जा के उपभोग के कारण होता है। उम्र बढ़ने के एक कारक के रूप में भोजन के महत्व को गैलेन ने भी नोट किया था। लेकिन लंबे समय तक इस समस्या को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा नहीं था। केवल 19वीं सदी में. उम्र बढ़ने के अध्ययन में कुछ प्रगति हुई है और उम्र बढ़ने के सिद्धांत सामने आने लगे हैं।
मानव शरीर की उम्र बढ़ने के पहले सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक जर्मन डॉक्टर एच. हफ़लैंड (1762-1836) का सिद्धांत है, जिन्होंने दीर्घायु में श्रम गतिविधि को महत्व दिया। हमने उनका यह कथन सुना है कि एक भी आलसी व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहता। और भी प्रसिद्ध उम्र बढ़ने का अंतःस्रावी सिद्धांत,जो पिछली सदी के मध्य में बर्थोल्ड (1849) द्वारा किए गए प्रयोगों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने दिखाया कि एक जानवर से दूसरे जानवर में वृषण का प्रत्यारोपण माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के साथ होता है। बाद में, फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट सी. ब्राउन-सेक्वार्ड (1818-1894) ने वृषण से अर्क के साथ खुद को इंजेक्शन लगाने के परिणामों के आधार पर तर्क दिया कि ये इंजेक्शन एक लाभकारी और कायाकल्प प्रभाव पैदा करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में. पहले से ही एक धारणा है कि बुढ़ापे की शुरुआत अंतःस्रावी ग्रंथियों, विशेष रूप से गोनाडों की गतिविधि के विलुप्त होने से जुड़ी है। 20-30 के दशक में. XX सदी इसी मान्यता के आधार पर अलग-अलग देशों में बुजुर्गों या बूढ़ों को तरोताजा करने के लिए कई सर्जरी की गई हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रिया में जी. स्टीनैच ने पुरुषों के शुक्राणु रज्जुओं को बांध दिया, जिससे गोनाडों का बाहरी स्राव बंद हो गया और कथित तौर पर कुछ हद तक कायाकल्प हो गया। एस.ए. फ्रांस में वोरोनोव ने युवा जानवरों से बूढ़ों में और बंदरों से पुरुषों में वृषण प्रत्यारोपित किए, और यूएसएसआर में तुश्नोव ने मुर्गों को गोनाड के हिस्टोलिसेट्स का इंजेक्शन देकर उन्हें फिर से जीवंत किया। इन सभी ऑपरेशनों से कुछ प्रभाव तो पड़े, लेकिन केवल अस्थायी। इन प्रभावों के बाद, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जारी रही, और भी अधिक तीव्रता से।
20वीं सदी की शुरुआत में. पड़ी उम्र बढ़ने का सूक्ष्मजीवविज्ञानी सिद्धांत,जिसके निर्माता आई.आई. थे। मेचनिकोव, जिन्होंने शारीरिक और रोग संबंधी बुढ़ापे के बीच अंतर किया। उनका मानना था कि मानव बुढ़ापा रोगात्मक है, अर्थात्। समय से पहले. आई.आई. के विचारों का आधार मेचनिकोव का ऑर्थोबायोसिस का सिद्धांत (ऑर्थोस -
सही, बायोस -जीवन), जिसके अनुसार उम्र बढ़ने का मुख्य कारण बड़ी आंत में सड़न के परिणामस्वरूप बनने वाले नशा उत्पादों द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं को होने वाली क्षति है। सामान्य जीवन शैली (स्वच्छता नियमों का पालन, नियमित काम, बुरी आदतों से परहेज) के सिद्धांत का विकास करना, आई.आई. मेचनिकोव ने किण्वित दूध उत्पादों के सेवन से आंतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दबाने का एक तरीका भी प्रस्तावित किया।
30 के दशक में XX सदी व्यापक हो गया उम्र बढ़ने में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) की भूमिका के बारे में सिद्धांत।इस सिद्धांत के रचयिता आई.पी. पावलोव, जिन्होंने जीवों के सामान्य कामकाज में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एकीकृत भूमिका की स्थापना की। आई.पी. के अनुयायी जानवरों पर पावलोव के प्रयोगों से पता चला कि समय से पहले बुढ़ापा तंत्रिका संबंधी झटके और लंबे समय तक तंत्रिका तनाव के कारण होता है।
उल्लेख के लायक संयोजी ऊतक में उम्र से संबंधित परिवर्तनों का सिद्धांत, 30 के दशक में तैयार किया गया। XX सदी ए.ए. बोगोमोलेट्स (1881-1946)। उनका मानना था कि शरीर की शारीरिक गतिविधि संयोजी ऊतक (हड्डी ऊतक, उपास्थि, कंडरा, स्नायुबंधन और रेशेदार संयोजी ऊतक) द्वारा सुनिश्चित की जाती है और कोशिकाओं की कोलाइडल अवस्था में परिवर्तन, उनके स्फीति का नुकसान, आदि उम्र से संबंधित परिवर्तनों को निर्धारित करते हैं। जीवों में. आधुनिक आंकड़े संयोजी ऊतकों में कैल्शियम संचय के महत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि यह इसकी लोच के नुकसान के साथ-साथ रक्त वाहिकाओं को सख्त करने में योगदान देता है।
उम्र बढ़ने के सार और तंत्र को समझने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान के डेटा का व्यापक उपयोग और विशेष रूप से आणविक आनुवंशिकी की उपलब्धियां हैं। उम्र बढ़ने के तंत्र के बारे में सबसे आम आधुनिक विचार इस तथ्य पर आते हैं कि जीवन के दौरान, शरीर की कोशिकाओं में दैहिक उत्परिवर्तन जमा हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण प्रोटीन या प्रोटीन के साथ अप्रयुक्त डीएनए क्रॉस-लिंक का संश्लेषण होता है। चूंकि दोषपूर्ण प्रोटीन सेलुलर चयापचय में विघटनकारी भूमिका निभाते हैं, इससे उम्र बढ़ने लगती है। सुसंस्कृत फ़ाइब्रोब्लास्ट के मामले में, पुरानी कोशिकाओं से जुड़े प्रोटीन और एमआरएनए को युवा फ़ाइब्रोब्लास्ट में डीएनए संश्लेषण को दबाने के लिए दिखाया गया है।
एक ज्ञात परिकल्पना भी है जिसके अनुसार उम्र बढ़ने को माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबोलाइट्स में परिवर्तन के साथ-साथ एंजाइमों की शिथिलता का परिणाम माना जाता है।
मनुष्यों में, जीन का अस्तित्व दिखाया गया है जो उम्र बढ़ने से जुड़ी वंशानुगत अपक्षयी प्रक्रियाओं के विकास का समय निर्धारित करता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि उम्र बढ़ने का कारण शरीर की प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली में परिवर्तन है, विशेष रूप से शरीर संरचनाओं के लिए ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं जो महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं। अंत में, उम्र बढ़ने के तंत्र की व्याख्या करते समय, विशेषज्ञ मुक्त कणों के निर्माण से जुड़ी प्रोटीन क्षति पर बहुत ध्यान देते हैं। अंत में, कभी-कभी लाइसोसोम के टूटने के बाद निकलने वाले हाइड्रोलेज़ को महत्व दिया जाता है, जो कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं।
हालाँकि, उम्र बढ़ने का एक व्यापक सिद्धांत अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी सिद्धांत स्वतंत्र रूप से उम्र बढ़ने के तंत्र की व्याख्या नहीं कर सकता है।
मौत।मृत्यु ओटोजेनेसिस का अंतिम चरण है। जीव विज्ञान में मृत्यु का प्रश्न एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि मृत्यु की भावना "... मानव स्वभाव में पूरी तरह से सहज है और हमेशा मनुष्य की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रही है" (आई.आई. मेचनिकोव, 1913)। इसके अलावा, मृत्यु का प्रश्न सभी दार्शनिक और धार्मिक शिक्षाओं के ध्यान के केंद्र में था और है, हालाँकि मृत्यु का दर्शन अलग-अलग ऐतिहासिक समय में अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था। प्राचीन विश्व में, सुकरात और प्लेटो ने आत्मा की अमरता के लिए तर्क दिया, जबकि अरस्तू ने प्लेटो की आत्मा की अमरता के विचार को नकार दिया और मानव आत्मा की अमरता में विश्वास किया, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। सिसरो और सेनेका ने भी भावी जीवन को मान्यता दी, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने मृत्यु को एक प्राकृतिक घटना माना जिसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया जाना चाहिए। 18वीं सदी में आई. कांट और आई. फिचटे (1762-1814) भी भविष्य के जीवन में विश्वास करते थे, और जी. हेगेल इस विश्वास का पालन करते थे कि आत्मा एक "पूर्ण अस्तित्व" द्वारा अवशोषित होती है, हालांकि इस "अस्तित्व" की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया था। .
सभी ज्ञात धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार, किसी व्यक्ति का सांसारिक जीवन उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, और व्यक्ति को इस भावी मृत्यु के लिए अथक तैयारी करनी चाहिए। हालाँकि, प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक जो अमरता को नहीं पहचानते हैं, वे मानते थे और अब भी मानते हैं कि मृत्यु है, जैसा कि आई.आई. ने बार-बार जोर दिया है। मेचनिकोव, एक जीव के जीवन का प्राकृतिक परिणाम। मृत्यु की एक अधिक आलंकारिक परिभाषा यह है कि यह "...अर्थ पर अर्थहीनता की, अंतरिक्ष पर अराजकता की स्पष्ट जीत है" (वी. सोलोविओव, 1894)।
वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि एकल-कोशिका वाले जीवों (पौधों और जानवरों) में मृत्यु को समाप्ति से अलग किया जाना चाहिए।
उनके अस्तित्व का ज्ञान. मृत्यु उनका विनाश है, जबकि अस्तित्व की समाप्ति उनके विभाजन से जुड़ी है। नतीजतन, एकल-कोशिका वाले जीवों की नाजुकता की भरपाई उनके प्रजनन से होती है। बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों में मृत्यु शब्द के पूर्ण अर्थ में जीव के जीवन का अंत है।
मनुष्यों में यौवन के दौरान मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से विकसित देशों में, 28 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु की संभावना लगभग तेजी से बढ़ जाती है।
किसी व्यक्ति की नैदानिक और जैविक मृत्यु होती है। नैदानिक मौत चेतना की हानि, दिल की धड़कन और सांस की समाप्ति में व्यक्त की जाती है, लेकिन अधिकांश कोशिकाएं और अंग अभी भी जीवित रहते हैं। कोशिकाओं का स्व-नवीनीकरण होता है और आंतों की गतिशीलता जारी रहती है। नैदानिक मृत्यु जैविक मृत्यु तक "पहुँचती" नहीं है, क्योंकि यह प्रतिवर्ती है, क्योंकि नैदानिक मृत्यु की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जीवन में "वापस" आ सकता है। उदाहरण के लिए, कुत्ते 5-6 मिनट के बाद जीवन में "लौट" आते हैं, मनुष्य - नैदानिक मृत्यु की शुरुआत से 6-7 मिनट के बाद। जैविक मृत्यु की विशेषता यह है कि यह अपरिवर्तनीय है। दिल की धड़कन और सांस रुकने के साथ-साथ स्व-नवीकरण प्रक्रिया, मृत्यु और कोशिकाओं का विघटन भी बंद हो जाता है। हालाँकि, कोशिका मृत्यु सभी अंगों में एक ही समय में शुरू नहीं होती है। सबसे पहले, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मर जाता है, फिर आंतों, फेफड़े, यकृत, मांसपेशियों की कोशिकाएं और हृदय की उपकला कोशिकाएं मर जाती हैं।
जीवों के पुनर्जीवन (पुनरुद्धार) के उपाय नैदानिक मृत्यु के विचार पर आधारित हैं, जिसका आधुनिक चिकित्सा में असाधारण महत्व है।
जीवनकाल
वनस्पतियों और जीवों के प्रतिनिधियों की जीवन प्रत्याशा पर आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि पौधों और जानवरों के बीच, अलग-अलग जीव अलग-अलग समय तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए, शाकाहारी पौधे (जंगली और खेती वाले) एक मौसम तक जीवित रहते हैं। इसके विपरीत, उनके लकड़ी वाले पौधों की विशेषता लंबी उम्र होती है। उदाहरण के लिए, चेरी 100 वर्ष जीवित रहती है, स्प्रूस - 1000 वर्ष, ओक -
2000 वर्ष, पाइन - 2000-4000 वर्ष तक।
कई प्रजातियों की मछलियाँ 55-80 वर्ष, मेंढक - 16 वर्ष, मगरमच्छ - 50-60 वर्ष, कुछ प्रजातियों के पक्षी - 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। स्तनधारियों का जीवनकाल छोटा होता है।
उदाहरण के लिए, छोटे पशुधन 20-25 वर्ष, मवेशी - 30 वर्ष या अधिक, घोड़े - 30 वर्ष तक, कुत्ते - 20 वर्ष या अधिक, भेड़िये - 15 वर्ष, भालू - 50 वर्ष, हाथी - 100 वर्ष जीवित रहते हैं। स्तनधारियों में मनुष्य सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है। बहुत से लोग 115-120 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे।
मौजूदा विचारों के अनुसार, जीवन प्रत्याशा एक प्रजाति-विशिष्ट मात्रात्मक विशेषता है जो जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसा माना जाता है कि आनुवंशिक रूप से निर्धारित जीवन प्रत्याशा ओटोजेनेसिस की अवधि (तालिका 5) से संबंधित है।
तालिका 5.दाता की उम्र पर खेती के दौरान फ़ाइब्रोब्लास्ट के स्तर की निर्भरता
यह माना जाता है कि प्रजातियों का जीवनकाल प्रजातियों का विकासवादी अधिग्रहण है। जहां तक व्यक्तियों की लंबी उम्र की बात है, तो इसे उनके जीनोटाइप में कुछ जीनों के संयोजन की उपस्थिति, या उनकी कोशिकाओं में कम संख्या या उत्परिवर्तन की पूर्ण अनुपस्थिति की धारणा से समझाया जा सकता है।
ए.ए. बोगोमोलेट्स और आई.आई. श्मालहाउज़ेन ने गणना की कि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक जीवन प्रत्याशा 120-150 वर्ष होनी चाहिए। हालाँकि, इस उम्र तक केवल कुछ ही जीवित बचे हैं। इसलिए, वास्तविक जीवन प्रत्याशा प्राकृतिक जीवन प्रत्याशा से मेल नहीं खाती है।
औसत जीवन प्रत्याशा कई कारकों (शिशु मृत्यु दर में कमी, संक्रमण नियंत्रण की प्रभावशीलता, सर्जरी में प्रगति, पोषण में सुधार और सामान्य जीवन स्थितियों) से प्रभावित होती है। जीवन प्रत्याशा में गिरावट का मुख्य कारण भूख, बीमारी और अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल से मृत्यु दर है। रूस में, हाल के वर्षों में, जन्म दर में कमी और उच्च मृत्यु दर के कारण सभी रूसी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नकारात्मक जनसंख्या देखी गई है।
चिकित्सा की दृष्टि से, जीवन प्रत्याशा किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य का संकेतक है। वृद्ध लोगों की संख्या के मामले में यूएसएसआर दुनिया में पहले स्थान पर है। उदाहरण के लिए, प्रति 1 मिलियन निवासियों पर 90 वर्ष से अधिक आयु के 104 लोग हैं, जबकि इंग्लैंड में - 6, फ्रांस में - 7
और यूएसए - 15 लोग। वर्तमान में, उदाहरण के लिए, 30 के दशक की तुलना में कामकाजी आबादी की सीमाओं में बदलाव आ रहा है। XX सदी सेवानिवृत्ति की आयु और लोगों की गतिविधि के स्तर के बीच का अंतर भी भिन्न होता है। 1982 में, विश्व जनसंख्या की उम्र बढ़ने की समस्याओं पर विश्व सभा वियना में आयोजित की गई थी, जिसमें 2025 तक इस मुद्दे पर पूर्वानुमान तैयार किए गए थे। यह माना जाता है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या तुलना में 5 गुना बढ़ जाएगी 1950 तक, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग - 7 बार। इस अंतरराष्ट्रीय मंच के अनुसार, विभिन्न लोगों, देशों और क्षेत्रों के बीच जनसंख्या की उम्र बढ़ने की दर में अंतर है।
जराचिकित्सा एक विज्ञान है जिसका कार्य उम्र बढ़ने वाले शरीर के बदलते कार्यों को सामान्य करने के तरीके विकसित करना है। हालाँकि, आधुनिक चिकित्सा के पास अभी तक सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के तरीके और साधन नहीं हैं। इसलिए, वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के उपचार और समय से पहले बुढ़ापा पैदा करने वाले जोखिम कारकों को खत्म करने (यदि संभव हो) तक जराचिकित्सा की भूमिका सीमित है।
चर्चा के लिए मुद्दे
1. जीवों के लैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं और इसकी जैविक भूमिका क्या है?
2. अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए तथा इसके रूपों के नाम बताइए।
3. एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में यौन प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन करें।
4. युग्मकजनन क्या है?
5. प्रत्येक प्रकार के युग्मक का क्या कार्य है?
6. आप युग्मकों के विकास के किन चरणों को जानते हैं?
7. शुक्राणुजनन और अंडजनन के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं?
8. अर्धसूत्रीविभाजन क्या है और इसका जैविक महत्व क्या है?
9. अर्धसूत्रीविभाजन के चरणों का वर्णन करें।
10. क्या क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्रीविभाजन के परिणामों को प्रभावित करता है और कैसे?
11. निषेचन के सार का वर्णन करें।
12. जाइगोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस के बीच क्या अंतर है?
13. वैकल्पिक अगुणित और द्विगुणित की जैविक भूमिका क्या है?
14. लैंगिक द्विरूपता क्या है? उभयलिंगीपन से आप क्या समझते हैं? क्या मनुष्यों में उभयलिंगीपन के मामले देखे गए हैं और कितनी बार?
15. आप प्रजनन के तरीकों के विकास की कल्पना कैसे करते हैं?
16. जीवों की वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं? कोशिका वृद्धि और विभेदन के बीच क्या संबंध है?
17. कोशिका विभेदन के आणविक आधार क्या हैं? आप स्टेम सेल के बारे में क्या जानते हैं?
18. ओन्टोजेनेसिस की अवधारणा तैयार करें और ओण्टोजेनेसिस की अवधियों का नाम बताएं।
19. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास में क्या अंतर हैं?
20. निषेचन का अंडों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
21. आनुवंशिक जानकारी के कार्यान्वयन के किस चरण में जीन की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है?
22. एक निषेचित अंडा एक बहुकोशिकीय संरचना में कैसे विकसित होता है?
23. विकास के दौरान विकासशील कोशिकाएँ और ऊतक एक दूसरे से कैसे भिन्न हो जाते हैं?
24. क्या खोए हुए या क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को वापस लाया जा सकता है?
25. ओन्टोजेनेसिस में वृद्धावस्था और जीवन प्रत्याशा के बीच क्या संबंध है?
26. प्राकृतिक (संभावित) और वास्तविक जीवन प्रत्याशा के बीच अंतर तैयार करें और निर्धारित करें।
27. आप जीवों की उम्र बढ़ने के कौन से सिद्धांत जानते हैं?
29. कौन से कारक जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करते हैं?
30. जीवों की क्लोनिंग किस पर आधारित है? जीवों की क्लोनिंग के उदाहरण दीजिए।
31. क्या शुक्राणु या उसकी सामग्री कोशिका में प्रवेश करती है?
32. क्लोनिंग डेटा क्या दर्शाता है?
33. जीव विज्ञान के इतिहास में प्रीफॉर्मेशनिज्म और एपिजेनेसिस। क्या इनका कोई वैज्ञानिक महत्व है?
34. नैदानिक और जैविक मृत्यु के बीच क्या अंतर हैं?
प्रजनन जीवों की अपनी प्रजाति बनाने की क्षमता है। प्रजनन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है और यह जीवों की संतान पैदा करने की सामान्य क्षमता के कारण संभव है। हालाँकि, तत्काल वंशज हमेशा अपने माता-पिता के समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, फर्न बीजाणुओं से अनेक संतानें विकसित होती हैं, जो ऐसे अंकुरों द्वारा प्रदर्शित होती हैं जो मातृ बीजाणु धारण करने वाले पौधे के समान नहीं होते हैं। वृद्धि पर, बदले में, स्वयं के विपरीत एक पौधा दिखाई देता है - एक स्पोरोफाइट। इस घटना को पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन कहा जाता है।
लैंगिक प्रजनन का एक विशेष रूप पार्थेनोजेनेसिस या वर्जिन प्रजनन है, जो एक अनिषेचित अंडे से एक जीव का विकास है। प्रजनन का यह रूप मुख्य रूप से स्पष्ट मौसमी परिवर्तनों के साथ छोटे जीवन चक्र वाली प्रजातियों की विशेषता है। पार्थेनोजेनेसिस अगुणित या द्विगुणित हो सकता है। अगुणित (जनरेटिव) पार्थेनोजेनेसिस में, एक अगुणित अंडे से एक नया जीव विकसित होता है। परिणामी व्यक्ति केवल पुरुष, केवल महिला, या दोनों हो सकते हैं। यह गुणसूत्र लिंग निर्धारण पर निर्भर करता है।
किसी जीव का व्यक्तिगत विकास, या ओण्टोजेनेसिस, जीव द्वारा अपनी स्थापना के क्षण से लेकर मृत्यु तक होने वाले क्रमिक रूपात्मक, शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तनों का एक समूह है। ओटोजेनेसिस के दौरान, शरीर को उसके माता-पिता से प्राप्त वंशानुगत जानकारी का कार्यान्वयन होता है। ओटोजेनेसिस में दो मुख्य अवधियाँ होती हैं - भ्रूणीय और पश्च-भ्रूण। भ्रूणीय अवस्था में पशुओं में भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य अंग तंत्र का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद की अवधि में, विकासात्मक प्रक्रियाएँ पूरी हो जाती हैं, यौवन, प्रजनन, बुढ़ापा और मृत्यु होती है।














